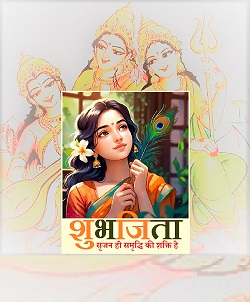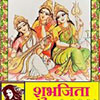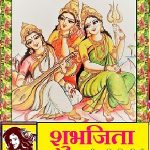अपराजिता फीचर डेस्क
पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 100 घंटे में जैश के आतंकियों को मार गिराया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीओसी चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल के जेएस ढिल्लन, सीआरपीएफ के आईजी जुल्फिकार हसन और श्रीनगर के आईजी एसपी पाणि ने कहा कि जैश के बड़ें आतंकियों की तलाश में अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि जो बंदूक उठाएंगे उनको मार गिराएंगे। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों की मांओं की सेना से अपील है कि बेटे को समझाएं कि घर वापास आ जाए।
सेना ने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान की सेना का हाथ और जैश को आईएसआई कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो घुसपैठ करेगा जिंदा नहीं बचेगा। कल की मुठभेड़ में जैश की तीन टॉप कमांडर ढेर किया गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कितने गाजी आए और चले गए।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए हैं। इनमें 12 यूपी से, 5 राजस्थान से और 4 पंजाब से हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल से दो-दो जवान हैं। इनके अलावा मध्यप्रदेश, झारखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक और असम से एक-एक जवान हैं। पुलवामा की शहादत को लेकर हर भारतीय सदमे में है। यह सच है कि समूचे राष्ट्र के लिए बेहद कठिन घड़ी है..मुश्किल घड़ी है..ये हम सब जानते हैं मगर ये नहीं जानते कि यह समय हर भारतीय के लिए एक चुनौती भी है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं…पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं..लगने भी चाहिए..मगर हमें रुककर यह भी सोचना होगा कि यह हमारे लिए इम्तहान की घड़ी है।

आज देखा जाए तो माहौल बहुत कुछ 1984 के बाद इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद वाला है मगर तब हमने जो गलती की थी और हमारी जिस नासमझी का फायदा अलगाववादी ताकतों को मिला था…हमें यह देखना होगा कि वह फायदा इस बार कश्मीरी अलगाववादी ताकतों को न मिले। यह यही है कि कश्मीर में दोहरी नागरिकता है मगर यह भी सच है कि अगर एक वर्ग नाराज है तो वहीं कुछ आम कश्मीरी ऐसे भी हैं जो हमसे, हमारे देश से प्यार करते हैं..वह खुद को भारतीय मानते हैं..। साल भर ही हुआ है सुजवां में सेना कैंप में हुए आतंकी हमले में हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे।

इन 6 में से एक शहीद मोहम्मद अशरफ मीर की अंतिम यात्रा उनके घर कुपवाड़ा में निकाली गई तो आस पड़ोस के गांवों के हजारों लोगों का सैलाब सड़कों पर उतर आया था। कुपवाड़ा के लोगों ने अपने जवान की शहादत के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। इस बार भी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों में जम्मू-कश्मीर के राजौरी के रहने वाले नसीर अहमद भी शामिल हैं। 47 साल के हेड कॉन्स्टेबल नसीर अहमद अपने पीछे पत्नी शाजिया कौसर और आठ साल और छह साल के बच्चे छोड़ गए हैं।

उनके पड़ोसी ने बताया कि नसीर रिटायरमेंट के बाद गांव डोदासन बाला में ही बसने की योजना बना रहे थे। नसीर अहमद ने 2014 में कश्मीर में आई भीषण बाढ़ से दर्जनों लोगों की जान बचाई थी। नसीर के बड़े भाई सिराज दीन जम्मू-कश्मीर पुलिस में है और फिलहाल जम्मू में तैनात हैं और उन्होंने ही पिता की मौत के बाद नसीर अहमद को पाल-पोस कर बड़ा किया था। जरूरी है कि कश्मीरी साथ रहे मगर आतंकियों से समझौता न हो, अलगाववादियों से समझौता न हो।

हमें पूरी कोशिश करके कश्मीरी जनता को अपने देश की मुख्यधारा में वापस लाना होगा…उनके अन्दर भारतीयता को पुख्ता करने की जिम्मेदारी हम सबको उठानी होगी और इसके लिए जरूरी है कि अलगाववादी ताकतों पर कार्रवाई हो..उनकी सुरक्षा छीन ली गयी है…उनकी सम्पत्तियाँ जब्त कर ली जाएं मगर आम कश्मीरी को कोई तकलीफ न हो..क्योंकि कश्मीर अगर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारा हिस्सा हैं। हमें उनकी मानसिकता को इस कदर बदलना होगा कि वे खुद आतंकियों को सहारा देना बंद कर दें और सेना के प्रयासों से स्थिति में सुधार आया है। पुलवामा में जो हुआ, वह आतंकियों की बौखलाहट है तो अब इनको जड़ से खत्म करने की जरूरत है।

इस हमले के खिलाफ पूरे देश में जो गुस्सा है, उसने हमें एक किया है और देश के विरोध में बोलने वाले बाकायदा बहिष्कृत हो रहे हैं। दो निजी कंपनियों ने अपने कश्मीर के उन कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है जिन्होंने पुलवामा में हुए आतंकी हमलों की तारीफ की थी। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुम्बई की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने श्रीनगर के अपने कर्मचारी को स्पीड पोस्ट के जरिए उसके निलंबन की जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि यदि उसने कारण बताओ नोटिस का दो हफ्ते के अंदर जवाब नहीं दिया तो उसे सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा।

इस कर्मचारी का नाम रियाज अहमद वानी है। उसने फेसबुक पर 14 फरवरी को पोस्ट पर लिखा था, ‘अथ वनान सर्जिकल स्ट्राइक।’ इसका मतलब होता है इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। कंपनी ने अपने नोटिस में लिखा है, ‘आपके राष्ट्र-विरोधी संदेश के कारण कंपनी को उग्र टिप्पणियां मिलनी शुरू हो गई। आखिर हमारे संगठन में एक राष्ट्र-विरोधी तत्व क्यों मौजूद है।’

कंपनी ने आगे कहा, ‘आपके कृत्य के कारण जो भयानक और गंभीर प्रकृति का है, उसके लिए आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। मामले में आगे की कार्रवाई लंबित है।’ दूसरा मामला अहमदाबाद बेस्ड हेल्थकेयर कंपनी का है। जिसने अपने श्रीनगर के रहने वाले कर्मचारी इकबाल हुसैन को तत्काल प्रभाव से उसकी टिप्पणी के कारण निलंबित कर दिया है। कर्मचारी ने रियाज अहमद वानी के पोस्ट पर लिखा था, ‘इसे कहते हैं असली सर्जिकल स्ट्राइक।’

इकबाल हुसैन हेल्थकेयर कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर हैं। उसे कंपनी ने 15 फरवरी को जारी किए कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब देने के लिए दो दिनों का समय दिया है। उसे बताया गया है कि यदि उसने अपनी सफाई नहीं दी तो उसे तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र पर ट्विटर पर हमले की प्रशंसा करने की वजह से एफआईआर दर्ज की गयी।

अब जरूरत है कि कश्मीर को इस देश का हिस्सा बनाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाएं, सेना पर भरोसा रखा जाए और हर भारतवासी निजी स्तर पर कोशिश जारी रखे। सबसे पहले तो धारा 370 खत्म करने की जरूरत है। कश्मीर के देश में मिलने -जुलने और एक होने में सबसे बड़ी बाधक यही धारा है। इस समय दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते मगर दूसरे राज्यों के लोग बसेंगे तो स्थानीय लोगों की असुरक्षा दूर करने में मदद मिलेगी। यह कश्मीर के लिए अच्छा है क्योंकि तब वहाँ उद्योग – धँधे विकसित होंगे और इस समय जो लोग रोटी के लिए हाथ में पत्थर उठा रहे हैं, वह मशीनें हाथ में लेंगे।

देश के विकास में हाथ बँटाएंगे। यह जरूरी है कि महबूबा और फारुक जैसे नेताओं को अल्टीमेटम दिया जाए…उनको केन्द्र से हटाया जाए और उनकी सत्ता हटाकर किसी आम कश्मीरी को नेतृत्व सौंपा जाए। रिश्ते तोड़ने हैं तो पाकिस्तान से तोड़िए..जितनी सख्ती कर सकते हैं, कीजिए। जो अलगाव की बात करे, अलगाववादियों के साथ खड़ा हो, उसका बहिष्कार करे। जो नेता ऐसी बात करे, हर पार्टी उसे निकाले। ऐसा हुआ भी है..कार्रवाई हुई है..इसे और तेज करने की जरूरत है। याद रहे कि हमारी लड़ाई कश्मीर या कश्मीरी से नहीं बल्कि अलगाववादी ताकतों और उनको पनाह देने वाले पाकिस्तान के सरपरस्तों से है। हमें खुद को मजबूत करना होगा…एक साथ आना होगा। आपसी मतभेद भुलाकर साथ खड़ा होना होगा। जनता जब जागेगी तो नेताओं को तो यूँ ही जागना होगा। इस हमले को किसी विशेष धर्म से मत जोड़िए क्योंकि ऐसा ही हमला ईरान में भी हुआ है, वहाँ भी 27 सैनिकों ने जान गँवाई है। हमें वह जड़ काटनी है जो अलगाववाद का जहर युवाओं के दिमाग में पहुँचा रही है और इसे काटना ही नहीं बल्कि समूल नष्ट करना है और इसके लिए कश्मीरी महिलाओं और पुरुषों को अपने बच्चों पर सख्त होना पड़े तो होना चाहिए।

इस समय सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर कश्मीरियों पर प्रहार हो रहे है। मीडिया शहादत में भी मसाला लगा रहा है..यहाँ संवेदनशील होने की जरूरत है। जिस सीआरपीएफ ने अपने 40 जवान खोए, वह जब अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रही, आम कश्मीरियों की सुरक्षा का प्रण ले रही है और अटल है तो हमें भी तो उसका साथ देना चाहिए। कश्मीर हमारा है तो उसे सँवारना भी हमारा काम है। अगर युवाओं का ब्रेनवॉश किसी आतंकी के द्वारा होता है और वह आतंक की राह पर चलता है तो हममें भी इतनी ताकत तो हो कि हम दोबारा उसे सही रास्ते पर लाएं और इसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है और कश्मीरी लोगों की बड़ी भूमिका है। देश में जहाँ कश्मीर के लोग हैं..उनके साथ खड़े होने का वक्त है मगर उससे ज्यादा उनको सही रास्ते पर लाने का वक्त भी है प्रण कीजिए कि हम 1984 की गलती फिर नहीं दोहराएंगे. मगर कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत तो दहशतगर्दों के हाथ से जरूर छुड़ान है.यही हमारी सच्चा सलाम होगा…शहीदों के नाम।
(इनपुट – इन्टरनेट से, शहीदों की तस्वीरें दैनिक भास्कर से)