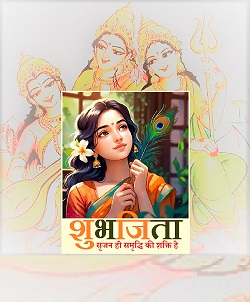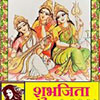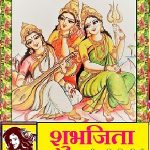कोलकाता । श्री शिक्षायतन कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) समिति और रेड रिबन क्लब ने पश्चिम बंगाल राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण सोसायटी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सघन अभियान का आयोजन एच.आई.वी / एड्स से मुक्त दुनिया बनाने के लिए गत शनिवार 29 नवंबर को किया गया। कॉलेज की प्राचार्या डॉ. तानिया चक्रवर्ती ने स्वागत भाषण में एच. आई. वी./ एड्स की रोकथाम और जागरूकता फैलाने की बात पर जोर दिया और संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में अनुदान की राशि बढ़ाने की ओर भी संकेत किया जिससे कि इस तरह के अभियान को तेज और सक्रिय करने में सहायता प्राप्त हो ।
एम. आर. बांगुर ,जिला अस्पताल की काउन्सिलर अरुंधति दत्ता, जिन्हें पश्चिम बंगाल स्टेट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटी के तहत नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स का अनुभव है, ने एच. आई. वी./ एड्स से होने वाले मानसिक तनाव को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने और ज़्यादा असरदार तरीके से भेदभाव को दूर करने के लिए इन गतिविधियों में युवाओं को शामिल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। अतिथियों और उपस्थित दर्शकों का स्वागत कॉलेज की छात्राओं द्वारा समूह नृत्य प्रस्तुत कर किया गया। कॉलेज की छात्रा ऋषिता, इशिका और शिवांगी ने क्रमशः बंगला, हिन्दी और अंग्रेजी में अपने वक्तव्य से एड्स के प्रति दर्शकों को जागरूक करने का प्रयास किया। एड्स की रोकथाम पर छात्राओं द्वारा नाट्य और गीत की प्रस्तुति के अलावा फ्लैश मॉब द्वारा भी जागरूकता फैलाने का सफल प्रयास किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कॉलेज के सचिव प्रदीप कुमार शर्मा के सहयोग एवं एन. एस. एस. समिति की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. बर्नाली लाहा, समिति के अन्य सदस्यों एवं छात्राओं का योगदान रहा।