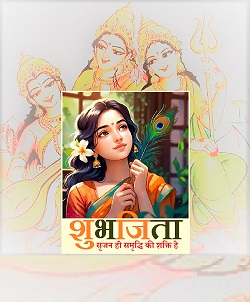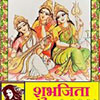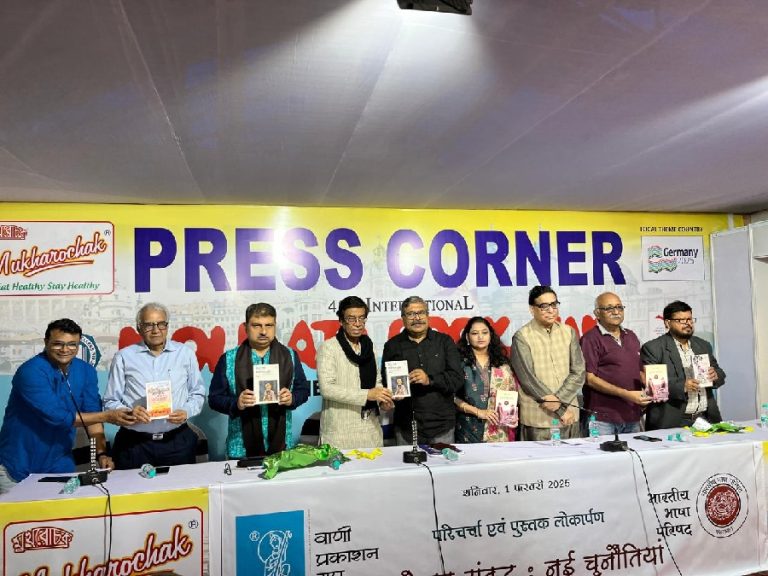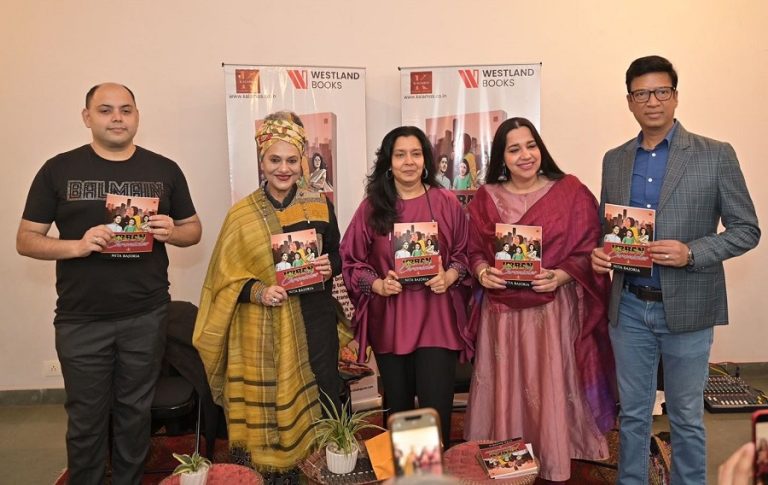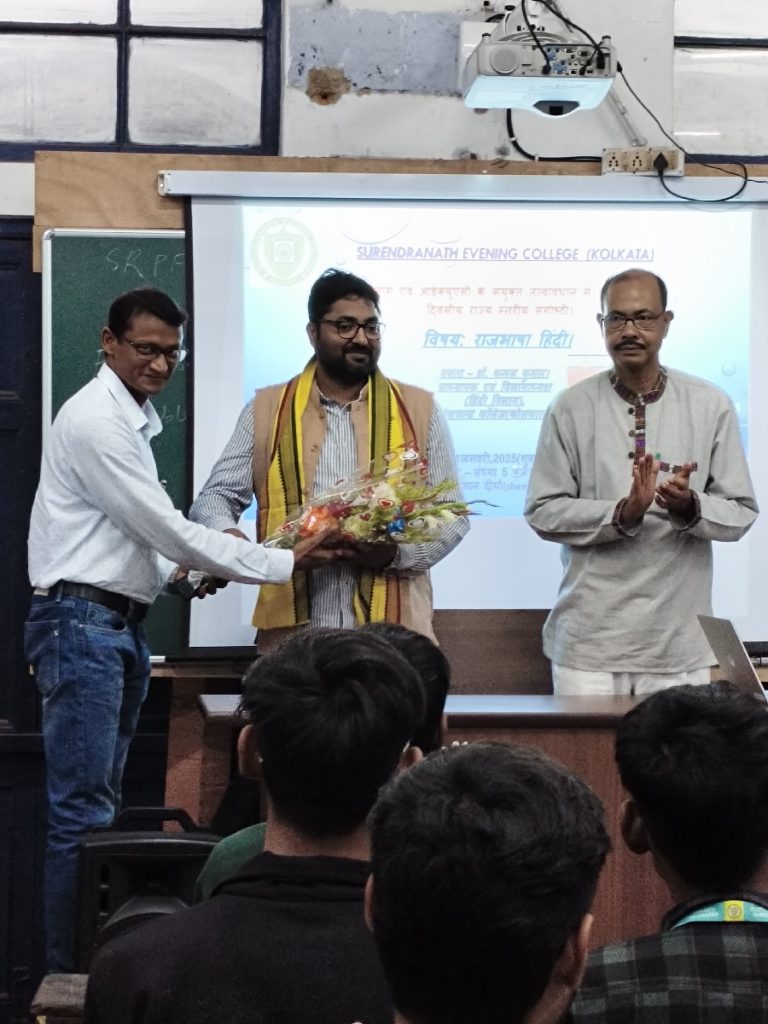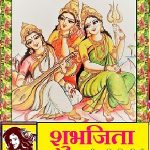नयी दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया। सर्वेक्षण में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की जीडीपी 6.3-6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। सर्वेक्षण में बताया गया कि युद्ध और तनाव के कारण भू-राजनीतिक जोखिम बने हुए हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को खतरा बना हुआ है।”
वैश्विक सर्विस निर्यात में देश सातवें स्थान पर –सर्वेक्षण में आगे कहा गया, “भारत का सर्विस ट्रेड सरप्लस में होने के – कारण समग्र व्यापार खाते संतुलन में बना हुआ है। मजबूत सर्विसेज के निर्यात के कारण वैश्विक सर्विस निर्यात में देश सातवें स्थान पर पहुंच गया है, जो इस सेक्टर में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दिखाता है।” आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक महंगाई नियंत्रण में है। वित्त वर्ष 25 के अप्रैल- दिसंबर की अवधि में औसत महंगाई कम होकर 4.9 हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 24 में 5.4 प्रतिशत थी।
चुनौतियों के बावजूद भारत में महंगाई प्रबंधन के सकारात्मक संकेत –सर्वेक्षण में कहा गया कि महंगाई को स्थिर करने में सरकार के सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण रहे हैं। इन उपायों में आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए बफर स्टॉक को मजबूत करना, समय-समय पर खुले बाजार में सामान जारी करना और आपूर्ति की कमी के दौरान आयात को आसान बनाने के प्रयास शामिल हैं। चुनौतियों के बावजूद भारत में महंगाई प्रबंधन के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि भारत की खुदरा महंगाई धीरे-धीरे वित्त वर्ष 2026 में लगभग 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगी।
देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत –सर्वेक्षण के मुताबिक, कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है। 2024 में खरीफ सीजन का खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 एलएमटी की वृद्धि दर्शाता है।उच्च मूल्य वाले सेक्टर जैसे बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन कृषि विकास के प्रमुख चालक बने हुए हैं। पीएम किसान के तहत 1 अक्टूबर तक, 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है, जबकि 23.61 लाख पीएम किसान मानधन के तहत नामांकित हैं।