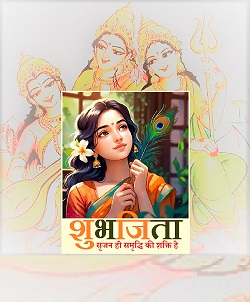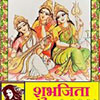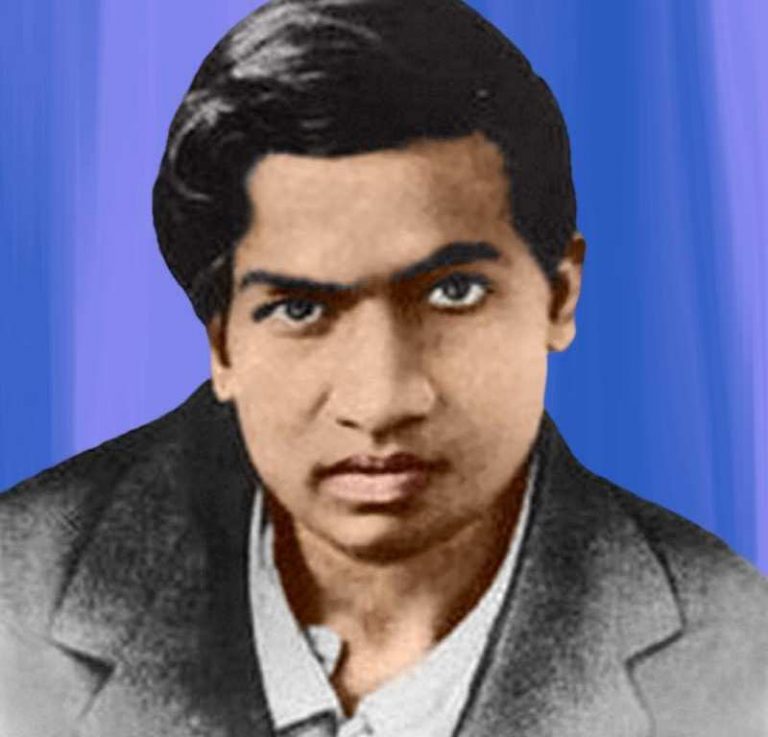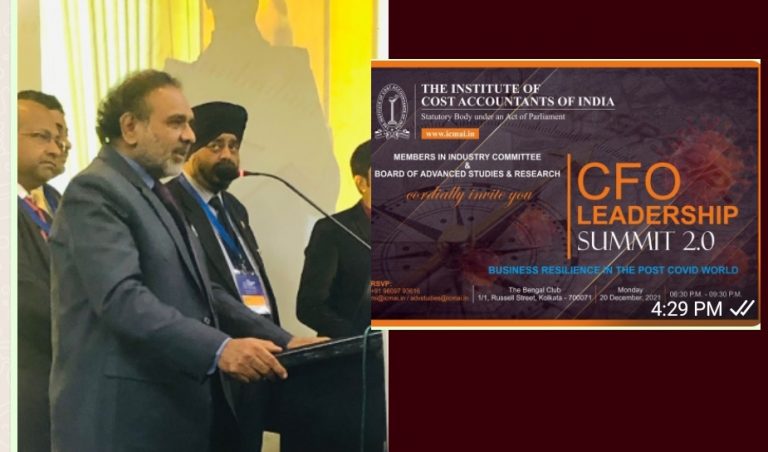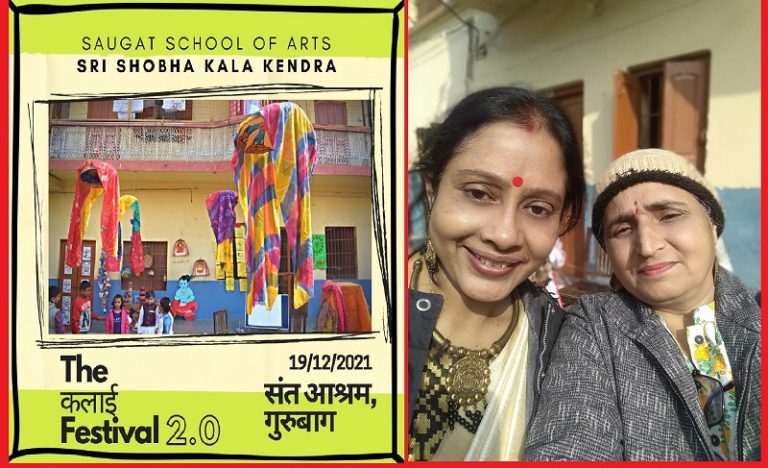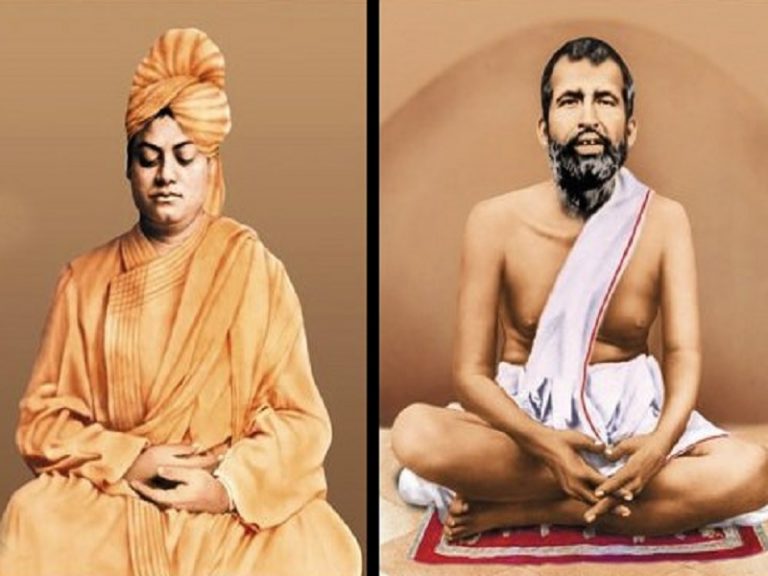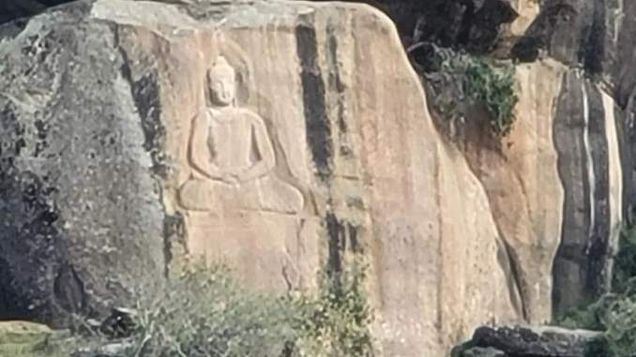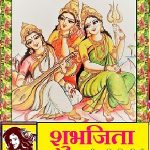कोलकाता । देश में सांस्कृतिक विविधता और अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में कोलकाता का हिंदी मेला आगामी 26 दिसंबर को लघु नाटक मेला के साथ मानिकतला के राममोहन हाल में शुरू हो रहा है। 1 जनवरी तक बाकी 6 दिनों का आयोजन भारतीय भाषा परिषद में होगा। आजादी के 75 वर्ष पर एक विशेष अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 31 दिसंबर को होगी जिसमें देश और बाहर के विद्वान भाग लेंगे।
सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन द्वारा भारतीय भाषा परिषद के साथ आयोजित इस मेले का मुख्य आकर्षण इस बार विभिन्न भाषाओं के गान पर काव्य नृत्य की प्रस्तुति है। सभागार के समानांतर ऑनलाइन हिंदी मेला में देश के दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों के भी विद्यार्थी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। हिंदी मेला विद्यार्थियों और नौजवानों के बीच खासतौर पर लोकप्रिय है और कोलकाता का गौरव है। यह मेले का 27वां साल है। इस बार भी यूको बैंक ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है।
हिंदी मेला भारत में अपनी तरह का अनोखा है। यह बच्चों, विद्यार्थियों और नौजवानों के बीच साहित्य को लोकप्रियकरण बनाने का एक साझा अभियान है। इसमें पश्चिम बंगाल के विभिन्न कोनों से हर साल 3000 से अधिक बच्चे, विद्यार्थी और नौजवान भाग लेते हैं। हिंदी मेले का उद्देश्य उनके मन में हिंदी भाषा, साहित्य और उदार भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग पैदा करना और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा को प्रकाश में लाना है।
27वें हिंदी मेले में कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है – लघु नाटक, काव्य आवृत्ति, काव्य संगीत, काव्य नृत्य, आशु भाषण, हिंदी प्रश्न मंच, लोक गीत, कविता पोस्टर, मल्टीमीडिया, रचनात्मक लेखन, और चित्रांकन। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चे और नौजवान निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, सर्वेश्वर, केदारनाथ सिंह, दुष्यंत कुमार आदि की कविताओं की आवृत्ति करते हैं, उन्हें वाद्ययंत्र पर गाते हैं, उन कविताओं के भाव पर आधारित नृत्य करते हैं और पोस्टर या चित्र बनाते हैं। लोक धुनों के बाजारीकरण के समानांतर लोकगीत स्वस्थ-सांस्कृतिक उमंग के साथ गाए जाते हैं। हिंदी मेला साहित्य और कला का अंत:संबंध मजबूत करने का अभियान भी है।
यह चिंताजनक है कि उच्चत्तर उद्देश्यों को समर्पित शिक्षण-संस्थान भी पॉप कल्चर की चपेट में आ गए हैं। हिंदी मेला की सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं पॉप कल्चर के प्रतिवाद और असहमति में खड़ी हैं। 27वें हिंदी मेले का उद्घाटन 26 दिसंबर, 2021 को होगा। 31 दिसंबर को स्वतंत्रता के 75 वर्ष की पूर्ति के अवसर पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है –स्वतंत्रता के 75 साल : साहित्य, संस्कृति और मीडिया। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता होंगे –विजय बहादुर सिंह (भोपाल), शंभुनाथ (कोलकाता), रविभूषण (रांची), अवधेश प्रधान (वाराणसी), अजय तिवारी (दिल्ली), दामोदर मिश्र (हावड़ा), हितेंद्र पटेल (कोलकाता), सोमा बंद्योपाध्याय (कोलकाता), संतोष भदौरिया (इलाहाबाद), अंजुमन आरा (कटक), वेदरमण (मॉरीशस)। इस मेले में ‘आज का विमर्श और मेरा लेखन’ साक्षात्कार श्रृंखला के अंतर्गत अशोक वाजपेयी (दिल्ली), राजेश जोशी (भोपाल), मोहनदास नैमिशराय (मेरठ), ए. अरविंदाक्षन (कोच्चि), भगवानदास मोरवाल (दिल्ली), रणेंद्र (रांची), अनिल प्रभा कुमार (अमेरिका), अग्निशेखर (जम्मू) का साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष युवा पत्रकार अनवर हुसैन को ‘युगल किशोर सुकुल पत्रकारिता सम्मान’, रंगकर्मी ओम पारीक को ‘माधव शुक्ल नाट्य सम्मान’ और प्रसिद्ध लेखिका प्रो. सोमा बंद्योपाध्याय को कल्याणमल लोढ़ा शिक्षक सम्मान दिया जाएगा।
हम हिंदी मेले में हिंदी की अखंडता और भारतीय भाषाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि हिंदी मेला शिक्षकों, लेखकों और साहित्य प्रेमियों के आर्थिक सहयोग के साथ यूको बैंक की प्रेरणाशक्ति से आयोजित हो रहा है। इस बार भारतीय भाषा परिषद का सह-योगदान भी हमें मिला है। इस तरह का हिंदी मेला हिंदी राज्यों में भी आयोजित होना चाहिए।