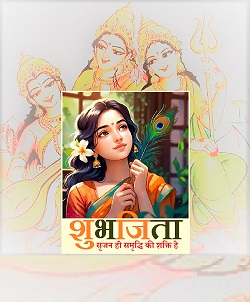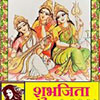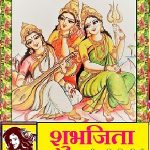रोंगटे खड़े कर देने वाले सिलहट युद्ध की कहानी
ढाका: तीन दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के एयरबेसेज को निशाना बनाना शुरू किया तो दोनों देशों के बीच जंग का आगाज हो गया। चार दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही भारत ने बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाया जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था। यहां से शुरू हुई बांग्लादेश की आजादी की कहानी जो 16 दिसंबर 1971 को भारत की जीत पर आकर खत्म हुई। इस युद्ध में यूं तो कई एतिहासिक मौके आए थे और सिलहट की लड़ाई इनमें से ही एक मौका थी। सात दिसंबर को सिलहट की लड़ाई शुरू हुई। भारतीय सेना इस लड़ाई में अजेय साबित हुई। सिलहट की लड़ाई में पहली बार था जब भारत ने दुश्मन की धरती पर कोई हेलीबॉर्न ऑपरेशन चलाया था। सिलहट की जंग नौ दिनों तक चली थी।
पाकिस्तान पर हुआ हमला
हवाई सर्वे के बाद सात दिसंबर को 4/5 गोरखा रेजीमेंट जिसके साथ माउंटेन गन और इंजीनियरों की एक टीम थी उसने हमले की शुरुआत कर दी थी। इसके साथ ही सेना की माउंटेन ब्रिगेड भी साथ थी। एमआई 4 हेलीकॉप्टर्स से एयरलिफ्ट किया गया था। ये हेलीकॉप्टर्स पहले से तय एक जगह पर उतरे थे। यह जगह थी मीरापुरा से बहने वाली सुरमा नदी की पूर्वी किनारा। पुल से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाकर सैनिकों को एयरलिफ्ट किया था। दोपहर में हेलीकॉप्टर्स ने जब लैंडिंग शुरू की तो दुश्मन हैरान रह गया था। सुरमा नदी बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली मेघना नदी का ही हिस्सा है। अगर भारतीय सेना को सिलहट पहुंचना था तो उन्हें सुरमा नदी को पार करना था।
शुरू हुई फायरिंग
दुश्मन को जैसे ही इसकी भनक लगी उसने फायरिंग शुरू दी। सिलहट में पाकिस्तान सेना के जवानों की संख्या भारतीय सेना की तुलना में आठ गुना तक ज्यादा थी। आज भी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह जंग ताकत नहीं सूझ-बूझ, बेहतर रणनीति और हौसले से लड़ी गई थी। समय-समय पर भारतीय सेना ने युद्ध का अपना तरीका और तब जाकर जीत मिली। सिलहट में पाकिस्तान के 6000 सैनिक मौजूद थे। भारतीय सेना को जो इंटेलीजेंस मिली थी उसके मुताबिक यह संख्या काफी कम थी। जब भारतीय सेना यहां पर पहुंची तो गलती का अहसास हुआ। सुरमा नदी पर बने पुल को पाकिस्तान की सेना ने नष्ट कर दिया था। सिलहट पाकिस्तान की सेना का वह ठिकाना था जिसकी वजह से ढाका के साथ सप्लाई रूट काफी मजबूत था। ऐसे में ढाका तक पहुंचने का रास्ता सिलहट से होकर जाता था। बिना सिलहट को जीते ढाका तक पहुंचना नामुमकिन था। सिलहट के उत्तर में मेघालय और पूरब में असम की सीमा से लगा हुआ है। पाकिस्तान की फौज ने यहां पर काफी तगड़ी घेराबंदी कर रखी थी। 31 पंजाब ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ था। सुरमा नदी से ठीक पहले पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे।
मुस्तैद गोरखा जवान
मुक्तिवाहिनी इस नदी को क्लीयर करने का काम दिया गया था और वह इसे पूरा नहीं कर सकी। फिर 750 सैनिक वाली गोरखा राइफल्स को इसका जिम्मा सौंपा गया। भारत को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान की 202 इंफेंट्री ब्रिगेड को सिलहट की सुरक्षा में तैनात है। लेकिन यह सूचना गलत साबित हो गई और दुश्मन ने हमला कर दिया। युद्ध के ऐलान से पहले ही गोरखा जवान मुस्तैद थे। गोरखा जवानों ने खुखरी से पाकिस्तानी जवानों को पस्त कर दिया और पाक सैनिकों को पीछे हटना पड़ा।
टॉर्च की रोशनी में लैंडिंग
अटग्राम और गाजीपुर पर जब पाकिस्तानी सेना ने कब्जा छोड़ा तो गोरखा सैनिकों के 10 हेलीकॉप्टर्स से सिलहट में लैंडिंग की योजना बनाई गई। गोरखा सैनिकों को हेलीबॉर्न ऑपरेशन के आदेश दिए। इससे पहले गोरखा जवान कभी भी हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़े थे और न ही उन्हें इसकी कोई ट्रेनिंग दी गई थी। रात करीब 9:30 बजे गोरखा सैनिकों ने इसका पूर्वाभ्यास किया और रात ढाई बजे ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। प्लान के तहत सात एमआई हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखा जवानों को हेलीकॉप्टर से लैंड कराया जाना था। मगर मुश्किल यह थी कि रात के वक्त न तो लैंडिंग हो सकती थी और न ही टेक ऑफ मुमकिन था। इसके बाद 80 टॉर्च की मदद से जमीन पर हैलीपैड का आकार बनाया गया। यह बिल्कुल हैलीपैड वाली जगह सा बना था। लैंडिंग का सिग्नल साफ नजर आया और लैंडिंग संभव हो सकी।
बीबीसी की गलती का फायदा
गोरखा जवानों के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने अल्लाह-हू-अकबर बोलते हुए हमला कर दिया। इसके बाद खुखरी के साथ पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया गया। जिस जगह पर लड़ाई हो रही थी वहां से ढाका करीब 300 किलोमीटर दूर था। इसी दूरी का फायदा उठाया गया। जब तक पाकिस्तानी सैनिक सिलहट पहुंचते तब तक गोरखा सैनिक अपना मिशन पूरा कर देते। गोरखा सैनिकों की संख्या कितनी है इस बात की जानकारी पाकिस्तान को नहीं थी। इस पर बीबीसी की गलती ने भी भारतीय सेना का फायदा पहुंचाया। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में गोरखा बटालियन को ब्रिगेड बता दिया यानी 3000 जवानों की संख्या। यह सुनकर पाकिस्तान भी घबरा गया था। हेलीबॉर्न ऑपरेशन को भारतीय वायुसेना की 110 हेलीकॉप्टर यूनिट ने अंजाम दिया था।
पाकिस्तान ने डाले हथियार
भारतीय जवानों ने एक बड़ा सा घेरा बना लिया था। इससे दुश्मन को लगा कि भारतीय सैनिक भारी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान के सैनिक डर के मारे बाहर ही नहीं आए। 800 गोरखा सैनिकों ने पाकिस्तान के 6000 सैनिकों को बंद करके रख दिया था। दिन में भारतीय वायुसेना के मिग और हंटर विमान हमले करते तो रात में गोरखा जवान कहर बनकर टूटते। पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला टूट गया और नौ दिनों के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डालने शुरू कर दिए थे।