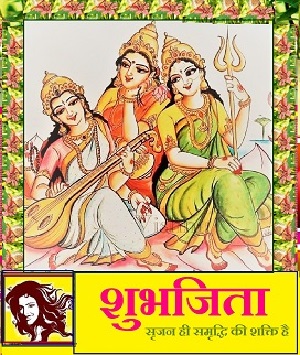इस देश में कृषि और कृषक हमेशा से ही महत्वपूर्ण मगर उतने ही उपेक्षित और शोषित रहे हैं। हम उन बड़े किसानों की बात नहीं कर रहे जो सम्पन्न हैं मगर उनकी तादाद भी कम है। देश के हर कोने में किसान परेशान है, वह मर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। सोशल मीडिया पर कृषक विमर्श की बाढ़ आ गयी है मगर यह सारा विमर्श आरोप – प्रत्यारोप में सिमट कर रह गया है। हर किसी ने अन्नदाता को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। मुमकिन है कि दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन को लेकर आप सवाल उठाएं मगर आप उन कठिनाइयों और कटु सत्य से मुँह नहीं मोड़ सकते और न ही शहर में रहकर परिस्थिति को समझा जा सकता है। माँग ऋणमाफ करने की हो रही थी मगर न तो यह कृषकों की समस्याओं का स्थायी समाधान है और न ही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत ही है। बावजूद इसके हर चुनाव के पहले ऋणमाफ करने को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मानने के बावजूद राज्य की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। प्रदर्शन और ऋणमाफी से आगे बढ़कर ठोस नीतियों की जरूरत है कि निचले स्तर तक इन नीतियों का लाभ पहुँचे और इसमें सरकार की ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट जगत, शिक्षाक्षेत्र से लेकर हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कृषि को महत्वपूर्ण मानने के बावजूद उद्योग की तुलना में उसे दोयम दर्जे का बनाया जा रहा है? हम किसानों के लिए रोते हैं और जब गाँवों के विकास को सरकार प्रमुखता देती है तो उस पर हाय – तौबा मचाने वाले भी हम ही होते हैं। जी हाँ, शहरों की शिक्षित और परिष्कृत जनता जो बहुरराष्ट्रीय कम्पनियों के मॉल से सब्जियाँ खरीदती है मगर पास जमीन पर बैठे दूर – दराज के गाँवों से आए एक कृषक से सब्जी या अनाज खरीदना उसकी शान के खिलाफ है। मनमानी कीमतों पर ब्रांडेड दाल, सब्जियाँ और फल खरीदने वाले लोग मोलभाव करते हैं और सोशल मीडिया पर आँसू बहाते हैं। खेती विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए महज एक प्रोजेक्ट वर्क है जिससे जरिए वे कुछ दिनों के लिए शहरों से ऊब कर गाँवों में जाते हैं मगर गाँवों में बसकर कृषि क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। आखिर ऐसे शोध क्यों नहीं हो रहे हैं जो कृषकों की मेहनत कम कर उसका उत्पादन बढ़ा सके और इसे एक बाजार उपलब्ध करवाए? कृषि से संबंधित इंजीनियरिंग, पशुओं को स्वस्थ रखने और दुधारू मवेशियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं या अभिभावक कहाँ तक बच्चों को गाँवों में जाने या बसने की अनुमति दे रहे हैं? खुद युवा पीढ़ी क्या गाँवों में जाना चाहती है या गाँवों को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहती है? क्यों सरकार जब पोस्टिंग किसी गाँव में करती है तो आन्दोलन और घेराव शुरू हो जाता है? कटु सत्य यह है कि सरकारी नौकरी प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि वहाँ तय मोटा वेतन है और यह धारणा है कि आरामदायक जीवनशैली भी मिलेगी। अगर ऐसा है तो हर बात के लिए सरकार को दोष देना कहाँ तक सही है? आज किसान मर रहे हैं तो भागीदारी हमारी भी है। कॉरपोरेट क्षेत्र चाहें तो कृषि से सम्बन्धित उद्योगों से इस देश के कृषि और प्राकृतिक संसाधनों को नया जीवन दे सकते हैं। आप पतंजलि का मजाक उड़ा सकते हैं मगर सत्य तो यही है कि पतंजलि ने कृषि को बड़ी सहायता दी है। सवा सौ करोड़ की आबादी वाला देश हर काम के लिए सरकार पर क्यों निर्भर है? क्या हम हर बात के लिए राजनेताओं और सरकारों पर निर्भर नहीं होते जा रहे? दोहरापन कहीं और नहीं हमारे भीतर है।
Uncategorized
किसान को बचाना, खुद को बचाना है, जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं हम सबकी है
-
सुषमा त्रिपाठी
इस देश में कृषि और कृषक हमेशा से ही महत्वपूर्ण मगर उतने ही उपेक्षित और शोषित रहे हैं। हम उन बड़े किसानों की बात नहीं कर रहे जो सम्पन्न हैं मगर उनकी तादाद भी कम है। देश के हर कोने में किसान परेशान है, वह मर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। सोशल मीडिया पर कृषक विमर्श की बाढ़ आ गयी है मगर यह सारा विमर्श आरोप – प्रत्यारोप में सिमट कर रह गया है। हर किसी ने अन्नदाता को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। मुमकिन है कि दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन को लेकर आप सवाल उठाएं मगर आप उन कठिनाइयों और कटु सत्य से मुँह नहीं मोड़ सकते और न ही शहर में रहकर परिस्थिति को समझा जा सकता है। माँग ऋणमाफ करने की हो रही थी मगर न तो यह कृषकों की समस्याओं का स्थायी समाधान है और न ही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत ही है। बावजूद इसके हर चुनाव के पहले ऋणमाफ करने को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मानने के बावजूद राज्य की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। प्रदर्शन और ऋणमाफी से आगे बढ़कर ठोस नीतियों की जरूरत है कि निचले स्तर तक इन नीतियों का लाभ पहुँचे और इसमें सरकार की ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट जगत, शिक्षाक्षेत्र से लेकर हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कृषि को महत्वपूर्ण मानने के बावजूद उद्योग की तुलना में उसे दोयम दर्जे का बनाया जा रहा है? हम किसानों के लिए रोते हैं और जब गाँवों के विकास को सरकार प्रमुखता देती है तो उस पर हाय – तौबा मचाने वाले भी हम ही होते हैं। जी हाँ, शहरों की शिक्षित और परिष्कृत जनता जो बहुरराष्ट्रीय कम्पनियों के मॉल से सब्जियाँ खरीदती है मगर पास जमीन पर बैठे दूर – दराज के गाँवों से आए एक कृषक से सब्जी या अनाज खरीदना उसकी शान के खिलाफ है। मनमानी कीमतों पर ब्रांडेड दाल, सब्जियाँ और फल खरीदने वाले लोग मोलभाव करते हैं और सोशल मीडिया पर आँसू बहाते हैं। खेती विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए महज एक प्रोजेक्ट वर्क है जिससे जरिए वे कुछ दिनों के लिए शहरों से ऊब कर गाँवों में जाते हैं मगर गाँवों में बसकर कृषि क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। आखिर ऐसे शोध क्यों नहीं हो रहे हैं जो कृषकों की मेहनत कम कर उसका उत्पादन बढ़ा सके और इसे एक बाजार उपलब्ध करवाए? कृषि से संबंधित इंजीनियरिंग, पशुओं को स्वस्थ रखने और दुधारू मवेशियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं या अभिभावक कहाँ तक बच्चों को गाँवों में जाने या बसने की अनुमति दे रहे हैं? खुद युवा पीढ़ी क्या गाँवों में जाना चाहती है या गाँवों को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहती है? क्यों सरकार जब पोस्टिंग किसी गाँव में करती है तो आन्दोलन और घेराव शुरू हो जाता है? कटु सत्य यह है कि सरकारी नौकरी प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि वहाँ तय मोटा वेतन है और यह धारणा है कि आरामदायक जीवनशैली भी मिलेगी। अगर ऐसा है तो हर बात के लिए सरकार को दोष देना कहाँ तक सही है? आज किसान मर रहे हैं तो भागीदारी हमारी भी है। कॉरपोरेट क्षेत्र चाहें तो कृषि से सम्बन्धित उद्योगों से इस देश के कृषि और प्राकृतिक संसाधनों को नया जीवन दे सकते हैं। आप पतंजलि का मजाक उड़ा सकते हैं मगर सत्य तो यही है कि पतंजलि ने कृषि को बड़ी सहायता दी है। सवा सौ करोड़ की आबादी वाला देश हर काम के लिए सरकार पर क्यों निर्भर है? क्या हम हर बात के लिए राजनेताओं और सरकारों पर निर्भर नहीं होते जा रहे? दोहरापन कहीं और नहीं हमारे भीतर है।
कृषि और कृषि क्षेत्र से संबंधित गहन अनुभव नहीं हैं मगर स्थिति को देखने और समझने के लिए अपराजिता ने थोड़ी सामग्री और आँकड़ों का संकलन किया है जिसमें बीबीसी हिन्दी से लेकर कई ब्लॉग और समाचार पत्रों के खबरों की कतरने शामिल हैं। हम जो कह रहे हैं, इनके आधार पर ही कह रहे हैं। यह स्थिति कृषि के साथ ही नहीं है बल्कि हमारी तमाम परम्परागत कलाओं और उद्योगों के साथ है। सच तो यह है कि आज गाँव, किसान और कृषि के लिए आँसू हर कोई बहा रहा है मगर कोई भी वहाँ जाकर काम करके स्थिति को सुधारने के लिए आगे नहीं आ रहा है। मीडिया भी नहीं, जिसने प्रदर्शन दिखाए मगर वह स्थिति नहीं जिस वजह से इन किसानों को दिल्ली आना पड़ा। खबरों के नाम पर हमें तमाशा करने और देखने की आदत हो गयी है। किसानों ने चूहे खाए और आपने उनको रोका नहीं, गजेन्द्र सिंह चौहान एक राजनीतिक सभा में सबके बीच में पेड़ से फाँसी लगाकर मर जाता है और हम उसे लाइव देखते हैं, ये संवेदनहीनता हमें मनुष्य होने का अधिकार भी रखने नहीं देती। स्थानीय स्तर पर जो आम नागरिक हैं, वे बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। केन्द्र के किसी मंत्री ने किसानों से मिलने की जरूरत नहीं समझी, कोई सितारा वहाँ नहीं गया और खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी लगभग महीने भर बाद आए।
हाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं और भारत में गरीबी और आर्थिक तंगी के चलते बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या करते हैं। सरकार कह रही है कि उसने किसानों की आत्महत्या के मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। महेन्द्र सिंह टिकैत के बाद कोई बड़ा किसान नेता नजर नहीं आया। 1990 के दशक से भारत में किसानों की आत्महत्या के मामले सुर्खियां बटोरते रहे हैं। पहले-पहल महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आईं और उसके बाद देश के दूसरे राज्यों में भी किसानों की आत्महत्या देखने को मिलीं।
कर्ज़ की वजह
किसानों का समर्थन कर रहे समूहों का कहना है कि अनाज की वास्तविक कीमतें किसानों को नहीं मिलती और उन्हें जीएम कंपनियों से कपास के काफी महंगे बीज और खाद खरीदने होते हैं। इन समूहों के मुताबिक जीएम बीज को खरीदने में कई किसान गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। जब फसल की सही कीमत नहीं मिलती है तो उन्हें आत्महत्या कर लेना एकमात्र विकल्प नजर आता है। यह स्थिति पंजाब जैसे राज्य में भी है। एक आँकड़े के अनुसार “भारत में वर्ष 2010 में करीब 1,90,000 आत्महत्याएं हुई हैं। इसमें किसान महज 10 फ़ीसदी ही हैं।” बावजूद इसके सरकारी आंकड़े भी कम भयावह नहीं हैं. इनके मुताबिक भी हर साल भारत में हजारों किसान आत्महत्या करते हैं. सरकार के ताजा आकंड़ों के मुताबिक 2011 में करीब 14 हजार किसानों ने आत्महत्या की। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट में भारत में आत्महत्याओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट छपी है जो बताती है कि कई आत्महत्याओं की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। लैंसेट के मुताबिक, वर्ष 2010 में 19 हजार किसानों ने आत्महत्या की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि किसानों की समस्या की जड़ें बेहद गहरी हैं और इनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है।
हर 30 मिनट में एक आत्महत्या
भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यहां की 80 फीसदी आबादी खेती पर ही निर्भर है. बावजूद इसके देश में यह क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की फुर्सत न तो किसी सरकार को है और न ही किसी राजनीतिक पार्टी को। हां, उनकी आत्महत्या के मामले अक्सर विपक्षी दलों के लिए सरकार पर हमले का हथियार जरूर बन जाते हैं। आंकड़ों के आईने में यह समस्या काफी गंभीर नजर आती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, वर्ष 1995 से 2013 के बीच तीन लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वर्ष 2012 में 13,754 किसानों ने विभिन्न वजहों से आत्महत्या की थी और 2013 में 11,744 ने। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। आँकड़े कुछ साल पुराने हैं तो जाहिर है कि यह स्थिति और भी विकट हो सकती है। वर्ष 2014 में भी आत्महत्या की दर में तेजी आई। इस दौरान 3,144 मामलों के साथ महाराष्ट्र लगातार 12वें वर्ष भी पहले स्थान पर बना हुआ है।
बस आंकड़ों की बाजीगरी
केंद्रीय खुफिया विभाग ने भी हाल में किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उसमें कहा गया था कि किसानों की आत्महत्या की वजह प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी। इनमें असमान बारिश, ओलावृष्टि, सिंचाई की दिक्कतों, सूखा और बाढ़ को प्राकृतिक वजह की श्रेणी में रखा गया था तो कीमतें तय करने की नीतियों और विपणन सुविधाओं की कमी को मानवनिर्मित वजह बताया गया था इस रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि आखिर इस समस्या पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। जाहिर है सरकारी एजेंसी की यह रिपोर्ट आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है। देश के जिन राज्यों में यह समस्या सबसे गंभीर है उनमें महाराष्ट्र तो पहले नंबर पर है ही, उसके बाद पंजाब, गुजारत, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। इन राज्यों में साल-दर-साल आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। किसानों की समस्याएं और उनके आत्महत्या के मामले कुछ दिनों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। सरकारें छोटा-मोटा मुआवजा देकर या राहत पैकेज का एलान कर अपने दायित्व से मुक्त हो जाती हैं। नतीजतन समस्या जस की तस रहती है और आत्महत्या का यह चक्र जारी रहता है. बस चेहरे बदलते रहते हैं।
एक ही उपाय, मौत
आखिर किसानों की बढ़ती आत्महत्या की वजहें क्या है? मोटे तौर पर इसकी जो वजहें हैं उनमें मानसून का बदलता मिजाज प्रमुख है। तमाम आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता के बावजूद तथ्य यह है कि ज्यादातर किसान अब भी फसलों की बुवाई और सिंचाई के मामले में बारिश पर ही निर्भर हैं। बीते कोई डेढ़ दशक से मौसम के लगातार बदलते मिजाज और बेमौसमी बरसात ने उनकी तबाही के रास्ते खोल दिए हैं। कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश उनकी तबाही की वजह बन जाती है तो कहीं बेमौसम बारिश फसलों की काल बन जाती है। सूखा और बाढ़ की समस्या तो लगभग हर साल सामने आती है। इसके अलावा कर्ज का लगातार बढ़ता चक्र भी एक अहम वजह है। बैकों से कर्ज की खास सुविधा नहीं होने की वजह से किसानों को बीज, खाद और सिंचाई के लिए पैसों की खातिर महाजनों और सूदखोरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह लोग 24 से 50 फीसदी ब्याज दर पर उनको कर्ज देते हैं लेकिन फसलों की उपज के बाद उसकी उचित कीमत नहीं मिलने की वजह किसान पहले का कर्ज नहीं चुका पाता। वह दोबारा नया कर्ज लेता है और इस तरह पीढ़ी-दर-पीढ़ी कर्ज के भंवरजाल में फंसती रहती है। आखिर में उसे इस समस्या से निजात पाने का एक ही उपाय सूझता है और वह है मौत को गले लगाना।
कीमतें तय करना जरूरी
विडंबना यह है कि बंपर फसल भी किसानों के लिए जानलेवा होती है और फसलों की बर्बादी भी। कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलों के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन उपज से लागत भी नहीं वसूल हो पाती। यही वजह है कि आत्महत्या की सबसे ज्यादा घटनाएं इन नकदी फसलों वाले राज्यों में ही होती हैं। फसल पैदा होने के बाद उनकी खरीद, कीमतें तय करने की कोई ठोस नीति और विपणन सुविधाओं का अभाव किसानों के ताबूत की आखिरी कील साबित होते हैं। तो आखिर इस समसया पर अंकुश लगाने का कारगर तरीका क्या है? विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक विपदाओं पर काबू पाना तो किसी के वश में नहीं है लेकिन फसल पैदा होने के बाद उनकी कीमतें तय करने की एक ठोस और पारदर्शी नीति जरूरी है ताकि किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिल सके। इसके अलावा विपणन सुविधाओं की बेहतरी और खेती के मौजूदा तौर-तरीकों में आमूल-चूल बदलाव जरूरी हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न सहकारी कृषक समितियों के साथ मिल कर इस दिशा में ठोस कदम उठाना होगा। उसी हालत में किसानों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
रोजाना ढाई हजार किसान छोड़ रहे हैं खेती
एनसीआरबी के पिछले पांच सालों के आंकड़ों के मुताबिक 2009 में 17 हजार, 2010 में 15 हजार, 2011 में 14 हजार, 2012 में 13 हजार और 2013 में 11 हजार से ज्यादा किसानों ने खेती से जुड़ी तमाम परेशानियों समेत अन्य कारणों से आत्महत्या कर ली। खेती में लगातार हो रहे घाटे के कारण रोजाना ढाई हजार किसान खेती छोड़ रहे हैं। और तो और देश में अभी किसानों की कोई एक परिभाषा भी नहीं है। सवाल उठता हैकि आने वाले आम बजट में सरकार, गांव, खेती और किसानों को इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए क्या पहल करेगी। किसान की क्या परिभाषा हो? क्योंकि वित्तीय योजनाओं के संदर्भ में किसान की एक परिभाषा है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का कोई दूसरा मापदंड है, पुलिस की नजर में किसान की अलग परिभाषा है। उतार-चढ़ाव के बीच कृषि विकास दर रफ्तार नहीं पकड़ रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2012, 2013 में कृषि विकास दर 1.2 फीसद थी, जो 2013-14 में बढ़ कर 3.7 फीसद हुई और 2014-15 में फिर घटकर 1.1 फीसद पर आ गई। पिछले कई सालों में बुवाई के रकबे में 18 फीसद की कमी आई है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, कृषि क्षेत्र की बदहाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दो दशकों में भारी संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं और ज्यादातर आत्महत्याओं का कारण कर्ज है, जिसे चुका पाने में किसान असमर्थ हैं, जबकि 2007 से 2012 के बीच करीब 3.2 करोड़ गांव वाले खासकर किसान शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। इनमें से काफी लोग अपनी जमीन और घर-बार बेच कर शहरों में आ गए। पंचायती राज व्यवस्था के इतने साल बीत जाने के बाद भी लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। खेती के प्रति रूझान लगातार कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका कारण पंचायतों का वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं होना है। ऐसे में केंद्रीय बजट का सात फीसद सीधे गांव को दिया जाए ताकि गांव में संसाधन विकसित किए जा सकें।
गांव से पलायन करने के बाद किसानों और खेतीहर मजदूरों की स्थिति यह है कि कोई हुनर न होने के कारण उनमें से ज्यादातर को निर्माण क्षेत्र में मजदूरी या दिहाड़ी करनी पड़ती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हर रोज ढाई हजार किसान खेती छोड़ रहे हैं। भारी संख्या में गांव से लोगों का पलायन हो रहा है जिसमें से ज्यादातर किसान हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के पिछले पांच सालों के आंकड़ों के मुताबिक 2009 में 17 हजार, 2010 में 15 हजार, 2011 में 14 हजार, 2012 में 13 हजार और 2013 में 11 हजार से ज्यादा किसानों ने खेती से जुड़ी तमाम परेशानियों समेत अन्य कारणों से आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा रही है। देश में 640 में से 340 जिलों में मानसून की बारिश में 20 फीसद तक कमी दर्ज की गई है। आज भी सिंचाई के लिए ज्यादातर किसान प्रकृति पर निर्भर हैं। बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि के कारण भारी मात्रा में हर साल फसलों की बर्बादी होती है।
ढाई दशक पहले कृषि को जब बाजारवाद के आसरे छोड़ने का निर्णय किया गया, समस्या वहीं से विकट होती गई। किसानों के लिए संकट की बात यह है कि पूरी दुनिया में अनाज के भाव कम हुए हैं, ऐसे में पैदावार घटने के बावजूद भारत में फसल के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अगर उत्पादन घटेगा तो किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा और यह किसान की समस्याओं को और बढ़ा सकता है। किसानों की आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। ऐसे में भी किसान सरकार से किसी वेतनमान की मांग नहीं कर रहा है बल्कि वह अपनी फसलों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है ताकि देश के लोगों के साथ अपने पेट भी ठीक से भर सके। सच तो यह है कि देश एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है जहां कोई खेती नहीं करना चाहता लेकिन भोजन सभी को चाहिए। इस मुद्दे पर समय रहते केंद्र और राज्य सरकारों को संजीदा होना होगा और इस पर व्यावहारिक रणनीति बनानी होगी। इसके साथ ही दोहरेपन से ऊपर उठकर शहरों से लेकर कॉरपोरेट और अकादमिक जगत और खुद हमको कृषकों के लिए आगे आना होगा। सिर्फ सरकार के भरोसे किसान को बचाना सम्भव नहीं है।
(नोट – अपराजिता यह दावा नहीं करती कि उपरोक्त सामग्री या आँकड़े उसने एकत्रित किए हैं। यह लेख www.dw.com, बीबीसी व समेत अन्य समाचारपत्रों के समाचारों पर आधारित है और इसका प्रयास पाठकों तक समस्या को हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए पहुँचाना है।)