
ऐ सखी सुन, देवी पर्व अर्थात नवरात्र समाप्त हो गया है लेकिन अभी बहुत सी देवियों की अराधना बाकी है। सखियों यह मौसम ही देवियों की पूजा का है, दुर्गा, लक्ष्मी और काली की पूजा। लेकिन मुश्किल तो इस बात की है कि हमारा समाज पाखंडी है जिसकी कथनी और करनी में उतना ही अंतर है जितना अंतर आसमान और धरती के बीच है। इसीलिए वह पूजा तो करता है देवियों की लेकिन घर की स्त्रियों को उतना भी सम्मान नहीं देता जितना हाड़ मांस के किसी भी जीव को देना चाहिए। शायद इसीलिए जिस देश में नारियों की पूजा होती है वहाँ सबसे ज्यादा प्रताड़ित नारियाँ ही होती हैं। नारीपूजक देश में स्त्रियों को बराबरी का अधिकार देना तो दूर की बात है उन्हें उनका संवैधानिक प्राप्य अधिकार भी नहीं मिलता। अखबार की सुर्खियां अधिकांशतः स्त्री के प्रति होनेवाले अपराधों से भरी होती हैं। हमने तकनीकी विकास की सीढ़ियां चढ़ने में भले ही कामयाबी हासिल कर ली हो लेकिन अपने संस्कारों और मानवीयता को निचले पायदान पर छोड़ आए हैं। हमने बड़ी- बड़ी डिग्रियां भले ही हासिल कर लीं लेकिन शिक्षा के सार को किसी अंधेरे कमरे में कैद कर दिया है। हमने अपनी बेटियों को गृहलक्ष्मी बनने के सारे गुर तो सिखा दिए लेकिन बाहरी मोर्चे पर उन्हें कैसे लड़ना है या घर के शत्रु से कैसे मुकाबला करना है, यह सिखाना हम भूल गए। और यही कारण है कि लड़कियाँ सहना और धीरज धरना तो सीख जाती हैं लेकिन अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना तो दूर की बात है कभी -कभी मुँह खोलना तक भूल जाती हैं। और सहते -सहते जब दर्द हद से गुजर जाता है तब उनकी पीड़ा प्रार्थना में बदल जाती है और वे बरबस कह बैठती हैं, “अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो”। यह एक ऐसी प्रार्थना है जिस पर एक पल के लिए ठहरकर पूरे समाज को सोचना चाहिए और सोचते- विचारते हुए अपने वैचारिक परिदृश्य को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए।

जब तक तकनीकी विकास के साथ साथ हम अपना मानसिक रूप से विकसित नहीं होंगे, उदार होकर सोचते हुए लड़का- लड़की की समानता के पक्षधर नहीं बनेंगे तब तक समाज भी नहीं बदलेगा। और लड़कियों के प्रति होनेवाले अपराधों में भी कमी नहीं आएगी। इसीलिए सखी हमें एकजुट होकर समाज के मानस को बदलना है। साथ ही अपनी बेटियों को अबला बनने का संस्कार घुट्टी में नहीं पिलाना है बल्कि शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाना है। उन्हें एक लड़की की तरह नहीं पालना है बल्कि एक सजग और सचेत नागरिक का संस्कार भी देना है जिसके कंधों पर समाज को गढ़ने का दायित्व हो। साथ ही अपनी बेटियों के अलावा बेटों को भी सामाजिक और मानवीय संस्कार घुट्टी में पिलाने की जरूरत है। उन्हें एक पुरुष की तरह नहीं पालना है बल्कि एक सचेत नागरिक बनाना है। उन्हें भी यह समझाने की जरूरत है कि शारीरिक बनावट में भले ही भेद हो लेकिन वे किसी भी मायने में लड़िकयों से श्रेष्ठ नहीं है। और जब हम अपनी बेटियों के साथ बेटों को भी सिखाना, बताना और संस्कारित करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में बदलाव आएगा। जब वे लड़कियों को अपने समान मानना समझना शुरु करेंगे तो उनके मन में उन्हें सजा देने, सबक सिखाने या उनका शोषण करने की बात आएगी ही नहीं। इस संदर्भ में मंजुश्री वात्स्यायन की कविता “चलन” की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगी जो हाथरस कांड के बाद लिखी गई हैं और बेहद विचलित करती हैं-
“गुड़िया तो गुड़िया ही थी
हूबहू बार्बी डॉल
सुनहरे,रेशमी घुंघराले बाल,
गुलाबी रंगत लिए
मक्खन से मुलायम गाल,
* * * * *
मां ने उसे समझाया था
अच्छे और बुरे स्पर्श का अर्थ
* * * * * * * * *
बावजूद इसके,एक दिन
घर के पीछे, पार्क में
मिला उसका क्षत-विक्षत शरीर,
* * * * * * *
कोई परिचित ही रहा होगा,
जिसे उसके मां-बाप ने निश्चय ही
नहीं सिखाया होगा
मानवोचित संस्कार
पुरूषोचित व्यवहार
बहन बेटियों की रक्षा करना
स्त्रियों का सम्मान करना
क्योंकि / हमारे यहाँ
बेटों को सिखाने का
चलन नहीं है ….
देखो सखी, हमारे समाज में लिंगभेद की जड़ें बहुत गहरी हैं लेकिन अपने धैर्य और संकल्प से हम समस्या की जड़ तक पहुंचकर इसका समाधान ढूंढने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। मानसिकता बदलेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। आओ सखी, हम सब एकजुट होकर इस बदलाव के लिए संकल्प लें।
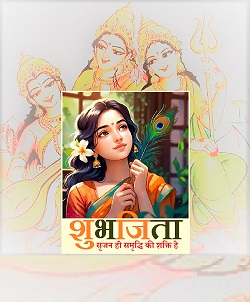





हमारे यहाँ बेटों को सिखाने का चलन नहीं है – समाज के यथार्थ को व्यक्त करती पंक्ति !
शुभजिता में प्रकाशित पोस्ट ‘ए सखी सखी सुन’ में गीता दूबे ने बदलाव की आकांक्षा से लिखे गए आक्रामक लेख में भारतीय समाज के कुटिल पाखंड पर कड़ा प्रहार किया है। देवियों की पूजा करने वाले देवी पूजक समाज में स्त्रियों को सम्मान और स्वाधीनता भी कितनी काट छाँट कर ज़रूरत और मजबूरी में दी जाती है , इसे हर उस स्त्री ने भुगता है, जो समाज के ढाँचे में विद्यमान भेदभावपूर्ण विधि-विधानों की जकड़न से मुक्त हो कर मानवीय अस्मिता और सम्मान के साथ जीना चाहती है। सच कहूँ तो हमारे समाज का ढाँचा भेदभाव पर खड़ा है। लिंगगत, जातिगत, सम्प्रदायगत, अर्थगत भेदभावों को जायज़ ठहराने के लिए हमारी तथाकथित महान संस्कृति के पास अपने तर्क और औचित्य हैं। दुख इस बात का बहुत है सखी कि इस तरह इनसे हिंसा और अधिकार हनन को सामाजिक विधि विधानों के तहत न्याय संगत मान्यता मिलती है और हमारा धर्म भीरु समाज जाने-अनजाने भेदभाव जन्य हिंसक आचरण का हिस्सा बन जाता है।
बदला बहुत कम है और बहुत बहुत बदलना है। एक पहाड़ है जिसे हिला नहीं सकते लेकिन थोड़ा काट ज़रूर सकते हैं। हाँ, सामूहिक ताक़त के डायनामाइट से उड़ा सकें और नया समाज गढ़ सकें तो राय ही अच्छा हो।सखी, गीता को समाज के लिंगगत भेदभाव की दुखती रग पर उँगली रखने के लिए साधुवाद