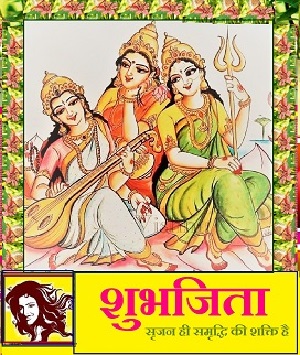शंभुनाथ
मैंने 1970 के दशक में कोलकाता के लेखकों का प्रचंड व्यवस्था-विरोध देखा है, जो अब एक मरती हुई भावना है।हिंदी और बांग्ला लेखकों के बीच तब नमस्कार-भालोबासा कहीं नहीं तो देशी शराब के एक चर्चित अड्डे खलासीटोला में दिख जाता था, जहां दोनों भाषाओं के लेखक आते थे और घुल-मिल जाते थे।
उन बांग्ला लेखकों में अहं नहीं था, नखरे नहीं थे। वे अपनी भाषा और संस्कृति से सदा प्रेम करते रहे हैं, चाहे जितने क्रांतिकारी विचारों के हों। यह प्रेम हिंदी में नहीं दिखता।
एक बार महाश्वेता देवी के लेखक बेटे नवारुण भट्टाचार्य के साथ टैक्सी में घर लौट रहा था। टैक्सी वाले ने उन्हें पहचान लिया। भीड़ में भी लेखक दिखता है, यदि उसके जन सरोकारों में ईमानदारी और निरंतरता हो। इस दिन मेरा विस्मय और बढ़ा, जब नवारुण ने बताया कि प्रसिद्ध बांग्ला कवि शक्ति चट्टोपाध्याय एक रात 11.30 बजे के करीब कोलकाता की एक सड़क पर नशे में हिलते-डुलते चल रहे थे कि गैरेज की ओर खाली लौटती एक डबल डेकर बस के ड्राइवर ने उन्हें पहचान लिया। इसने उन्हें बस में बैठाया और यह विशाल बस अकेले उन्हें लेकर उनके घर के दरवाजे तक पहुंची।
इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में लेखक की पहचान दुनिया के अन्य नगरों की तरह कोलकाता में भी धूमिल हुई है। यदि वह राजनीतिज्ञों या फिल्मी अभिनेताओं के साथ खड़ा नहीं है तो उसे कोई नहीं देखता। काफी हाउस के पहले जैसे अड्डे नहीं हैं। लेखक अपने घर से बाहर नहीं निकलते। शहर में हर तरफ रोशनी इतनी ज्यादा है कि आंखें कुछ देख न सकें। खाने-पीने की मस्त दुकानें खुल गई हैं। अब अकेलेपन को महसूस करते हुए टहलने की कोई जगह नहीं है। पहले की तरह भटकन नहीं है, और खोज नहीं है, गंतव्य इतने स्पष्ट हैं।
कोलकाता अब न जुलूसों-प्रदर्शनों से गूंजता राजनीतिक शहर है और न बहसों से उत्तप्त सांस्कृतिक शहर। जुलूसों की जगह अभिजात किस्म के रोड शो हैं। साहित्यिक बहसों की जगह लिटरेरी फेस्टिवल हैं। पिछली फरवरी में ऐसे ही एक फेस्टिवल में आए लेखकों के लिए डिनर का प्रबंध शहर के सबसे महंगे होटल द हयात में था।
वहां से केदारनाथ सिंह, अरुण माहेश्वरी और निर्मला तोदी के साथ मैं अधखाया लौटा था। ज्यादातर लेखक ऐसे थे जो मीडियाकर किस्म के थे। मीडियाकरों का कभी समाज नहीं होता। प्रश्न उठता है, आज लेखक संगठित क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या इतना भीषण सामाजिक अंतर्द्वंद्व इसलिए है कि शहर शिकारियों से भरता जा रहा है? यदि आदमी शिकारी नहीं है, तो बस किसी का शिकार है।
कोलकाता में एक समय तर्क का तूफान था, वह बुद्धिवाद का युग था। आज तर्क की जगह जुमले हैं। बुद्धिवाद अब व्यावसायिक बुद्धिवाद और तकनीकी बुद्धिवाद में सीमित हो चुका है। कोलकाता एक व्यावसायिक नगर है, जहां शिक्षा और चिकित्सा में व्यवसाय का सबसे भयंकर रूप है। यह मानवता का एक बड़ा सिरदर्द है। बुद्धिवाद के दीर्घ इतिहास से संबंधविच्छेद का नतीजा है कि एक तरफ अतीत से अंध-राष्ट्रवादी संबंध बना है तो दूसरी तरफ व्यावसायिक मुनाफाखोरी के लिए कुछ सनसनीखेज कहने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
कुछ लोग “अतीतबद्ध राष्ट्रवादी” हैं तो कुछ “अतीतविहीन ग्लोबल” हैं। ये दोनों ही नव-औपनिवेशिक तत्व हैं। क्या महानगर में बुद्धिपोषित महान भाव फिर लौटेंगे? यह सवाल इस शहर के “आत्म” को रि-डिस्कवर करने से जुड़ा है।
यहां की कुछ चीजें खास तौर पर प्रसिद्ध रही हैं — रसगुल्ला, फुटबाल और बुद्धिजीवी। रसगुल्ला अब कैडवरीज की मिठाइयों में डूब गया। फुटबाल के उत्तेजक मैच फीके पड़ गए, मोहन बगान-ईस्ट बंगाल की लड़ाई आइपीएल के मजे में खो गई। बंगाल लोकल है या एकदम ग्लोबल । बुद्धिजीवी महत्वाकांक्षी हो गए हैं। जहां नए मूल्यों का जन्म हुआ, वहां मूल्यबोध अब कोई मुद्दा नहीं है।
कोलकाता के बारे में कहा जाता है कि कोलकाता में अनेक कोलकाता हैं, उनके बीच से अपना कोलकाता ढूंढ़ लेना होता है। यह खास शहर है जहां फिर भी प्रेम और कृतज्ञता का अभी पूरी तरह अंत नहीं हुआ है। इस शहर ने जिसे पकड़ लिया, वह इसके आकर्षण से बाहर नहीं निकल सका, भले अब यहां बहुत कलह है, हिंसा है और जीवन पहले से ज्यादा असुरक्षित है। सभ्यता की नकाब में हिंसा आदमीयत को ज्यादा खाती है, पर कोलकाता में ऐसे काफी लोग हैं जो अभी इस तरह से सभ्य नहीं हैं। कई शहर मनुष्य की वापसी के इंतजार में हैं, जबकि कोलकाता में अभी मनुष्य बसते हैं।
अब एक खास तरह के शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और लेखकों से कोलकाता खाली-खाली लगता है। वे लोग व्यवस्था में कहीं शरीक होते हुए भी पूरी तरह उसमें डूबे नहीं होते थे। वे मेहनती थे, जागरूक थे और जोखिम उठाते थे। उन क्रांतिकारी प्रतिरोधों को भूलना आसान नहीं है जो कोलकाता की अविस्मरणीय घटनाएं हैं। नव-उदारवाद ने विभिन्न स्तरों पर सबकुछ निगल लिया — प्यार, गुस्सा, आत्मविश्वास, हार्दिकता। मुक्तिबोध ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि तुम्हारे पास और हमारे पास क्या है, सिर्फ ” ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लम है,अभय की गेती है, हृदय की तगारी है तसला है– नए-नए बनाने के लिए भवन—आत्मा के, मनुष्य के”। वामपंथी अति-उत्साह में पहले ईमानदारी और समझदारी का संबंधविच्छेद हुआ, ईमानदारी की तुलना में समझदारी ज्यादा जरूरी चीज मानी गई। फिर निर्भयता की जगह वफादारी ने ले ली। निर्भयता और कायरता में कायरता का पलड़ा भारी पड़ता गया। खुदगर्जी पनपी। हृदय का अभाव होता गया। राजनीति के केंद्र में जब गधे आ गए,इन्होंने सब कुछ चरना शुरू कर दिया — प्रेम, गुस्सा,आत्मविश्वास, निर्भयता, हार्दिकता– हर अच्छी चीज। जीवन में “श्रेष्ठ”, “मूल्यप्रवण” और “तर्कसंगत” को बचाने की कोशिशें जब मूर्तियों, स्मारकों के निर्माण और महापुरुषों की छवियों पर माल्यार्पण तक सीमित हो जाती हैं ये महज सांस्कृतिक बाह्याडंबर के चिह्न होते हैं।
कोलकाता में बांग्ला लेखकों के अड्डे घटे हैं। अखबारों में साहित्यिक घटनाओं के लिए जगह सिकुड़ी है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श जैसे मामले नदारद हैं। मीडिया में राजनीतिक खबरों के बाद फिल्म, क्रिकेट, अपराध और एलीट मनोरंजन ही हावी हैं। किसी जमाने में साहित्य की प्रधानता थी। अब लघु पत्रिकाएं हैं और कुछ पत्रिकाओं ने अच्छे प्रकाशन खड़े कर लिए हैं। यह हिंदी में दुर्लभ है। सभी तरफ लेखकों में बिखराव है।
सरकार से लेखकों-कलाकारों के मधुर रिश्ते रखने का चस्का लंबे समय से है। उनका राजनैतिक समायोजन पहले से बढ़ा है। ऐसे ही दृश्य हिंदी में भी हर तरफ हैं। यह अब विरोधों का युग नहीं है, अवसरों की तलाश का समय है। गाय घास खाकर दूध देती है, पर कर्इ लेखक-शिक्षक दूध-मलाई खा कर घास दे रहे हैं। नोटबंदी का ज्यादा असर न हो, नेटबंदी का व्यापक दुष्प्रभाव है। लोग घर में भी हर समय इंटरनेट पर हैं। सारी बौद्धिकता सोशल मीडिया पर खलास हो जाती है। इसने लोगों को असामाजिक बनाया है और लेखकों के सृजनात्मक पंख कतर डाले हैं। यहां भी हिंसा है। कोई शहर राजनैतिक झुंडों से भर जाए, अंध-राष्ट्रवाद का ज्वार हो और साहित्यिक वस्तु भी पुल न हो कर दीवार होती जाए तो यह उस शहर का घृणा में पागल होना है। पहले के पागल कितने अच्छे थे — टोबाटेक सिंह (मंटो),बावनदास (रेणु), जरनैल सिंह (भीष्म साहनी) जैसे पागल! अब ऐसे पागल ढूंढ़े नहीं मिलते।
पार्क स्ट्रीट से लेकर न्यू टाउन तक तुच्छ ही विराट है — विराट भवन, विराट रास्ते, विराट बाजार और विदेशी ब्रांड की वस्तुएं। बेरोजगारी और अपराध का अनंत। ऐसी घड़ियों में शहर अपनी कृतियों से नहीं कृत्रिम सजावटों से पहचाने जाने लगते हैं।
कोलकाता का लंबा इतिहास रह-रह कर पुकारता है। उसमें आधुनिक हिंदी के निर्माण का इतिहास भी है। यहां हिंदी का पहला अखबार छपा। यहां निराला हुए। यहां से “मतवाला”, “विशाल भारत”,”ज्ञानोदय” आदि पत्रिकाएं निकलीं। अब इतिहास कोई न ढोता है और न बनाता है। अपने इतिहास से बाहर निकल रहा है कोलकाता,इतिहास द्वारा बार-बार पुकारा जाता हुआ भी। अकेले शहर कोलकाता में बांग्ला लेखकों के नाम पर जितने पुल,सड़कें और स्मारक हैं, दस राज्यों के हिंदी क्षेत्र में हिंदी साहित्यकारों के नहीं होंगे।
गंगा कोलकाता के इतने करीब बहती है, पर यह शहर भूल चुका है कि गंगा कहां से बहते हुए आती है। वह कभी विभाजित नहीं की जा सकी। उसकी छाती पर नावों की जगह अब बड़े-बड़े जहाज हैं। विलासिता पूर्ण क्रूज हैं — गंगा के फोड़े की तरह। फिर भी जेटी से अब भी कूदते हैं नंग-धड़ंग बच्चे। इन्हें नागार्जुन ने 1984 में हावड़ा के बिचाली घाट से चालीस कवियों के साथ देखा था– बाबा और चालीस कवि!
एक शहर तब मरता है जब बहसें अवरुद्ध हो जाती हैं और लोकतांत्रिक परिसर सिकुड़ जाता है, भले वह आसमान छूते हुए अपनी चौहद्दी का लगातार विस्तार करता जाए। कोलकाता में बहस अब अंग्रेजों के जमाने में बने सटर्डे क्लब, टालीगंज क्लब जैसी लाखों रुपयों की सदस्यता वाली जगहों पर सेलेब्रिटी व्यक्तियों के पैनेल डिस्कशन में खिलखिलाती है। वह वेशकीमती होती है — ग्लैमर भरी। आम तौर पर बहस वहीं संभव है, जहां संवाद बचा हो। अब हर झुंड में श्रोता बन कर आज्ञा पालन में खड़े लोग हैं। तर्क करने वाले को अकेले हो जाना होगा। कोलकाता तब जिंदा रहता है सिर्फ अकेलेपन की पीड़ाओं में और युवा कलरवों में!
कोलकाता ट्राम, हावड़ा पुल और विक्टोरिया मेमोरियल के लिए प्रसिद्ध रहा है और इन सबसे अधिक रवींद्रनाथ ठाकुर के लिए। उन्होंने कहा था, “हृदय भय शून्य हो और सिर हमेशा ऊंचा उठा रहे!”
कोलकाता में निर्भय होकर आत्मसम्मान के साथ आज भी जिया जा सकता है। कहा गया है, “यदि साफ और हरा-भरा शहर देखना हो दिल्ली को देखो। यदि अमीर और एक-दूसरे से बेखबर लोगों का शहर देखना हो तो मुंबई जाओ। यदि हाई-टेक शहर चाहिए तो तुम्हारे लिए बेंगलुरु है, पर यदि ऐसे शहर में जाना चाहते हो जहां आत्मा हो तो कलकत्ता आओ।” आज भी यदि अनजानों के बीच कोई मुसीबत में पड़ जाए, एक न एक अपरिचित का हाथ सहायता के लिए बढ़ जाता है। इस मानव भावना ने ही कोलकाता को जिंदा रखा है।
अमेरिका के कंसास शहर में जब एक अमेरिकी ने दो भारतीयों पर यह कह कर गोली चलाई, “तुम बाहरी हो,अमेरिका से निकल जाओ”, चौबीस साल का एक श्वेत अमेरिकी युवक उन्हें बचाने के लिए बंदूकधारी पर टूट पड़ा था। वह भी गोली से घायल हुआ। उस अमेरिकी युवा का भारतीयों से न मजहब का रिश्ता था और न देश का। यह मानव भावना ट्रंपवाद की जयजयकार के बावजूद संसार में बची है। इसके बिना संसार चल नहीं सकता। इसे सार्वभौमिकता कह कर कोई सभ्यता खोना नहीं चाहेगी। भारत के शहरों में भी “बाहरी” को लेकर घृणा इधर बढ़ी है, पर यह मानव भाव भी है। कोलकाता में भी यह है। यह भाव ही किसी शहर की आत्मा है।
नजीर अकबराबादी के “आदमीनामा” की लाइनें हैं, “यां आदमी पे जान को वारे है आदमी/ और आदमी पे तेग को मारे है आदमी/ पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी/ चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी/ और सुन के जो दौड़ता है वह भी आदमी।” शहर में चीख सुनने पर दौड़े आने की तमीज अभी बची है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अपनों की सहायता करने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कोलकाता में सदियों की संस्कृति है, अपरिचितों के विपत्ति में पड़ने पर भी किसी न किसी के अंदर मनुष्य भाव जग जाता है। एक बुरा और बदमाश आदमी भी तब थोड़ी देर के लिए इन्सान बन जाता है
मेरा जीवन कोलकाता में बीता है। इसलिए मन ऐसा है, “जैसे उड़ि जहाज से पंछी पुनि जहाज पै आवै।” कोलकाता से मैं ज्यादा साल बाहर नहीं रह सका। दिल्ली-आगरा से एक दूसरे शिखर की ओर राह बनाने की जगह अपने घर लौट आया।
अब कोलकाता ऐसा शहर नहीं है, जहां सच के लिए जीने-मरने का पहले-सा जज्बा है। राजनैतिक संकीर्णताओं ने इस शहर में अजनबीपन का बोध बढ़ाया है, लोग मन मार कर शांतिपूर्वक रहते हैं। आपस में दूरियां बढ़ी हैं, जिसके कारण सृजनात्मकता और विकास दोनों प्रभावित हुए हैं। परिवर्तन की जगह प्रतीकवाद आ गया है। यह “पोस्ट ट्रुथ” का समय है। हर तरफ झूठ की चमचमाहट है। महत्वाकांक्षाओं के लिए मानवीय संबंधों को रौंद डालने का नया रिवाज बन गया है। पहले जहां पेड़ के पक्षी भी पहचानते थे, वहां आसमान इतना सिकुड़ गया है कि अब संकरी होती गई गलियों में चांद दिखाई नहीं देता। भीड़ में लोग इतने बदल गए हैं कि अपनेपन की तलाश की जगह आशाओं में भटकती उदास आखें होती हैं — कभी कुछ पातीं, कभी कुछ नहीं पातीं।
हर शहर ऐसे हो गए हैं जहां लोग शिवाजी और अफजल खां की तरह मिलते हैं। फिर भी हर शहर में कुछ ऐसा होता है जो मानव भाव को खत्म होने नहीं देता। इतिहास की तेजस्विता मनुष्य की अंत:शक्ति में छिपी होती है। कोलकाता तो मां की गोद की तरह है। यहां गंगा बहती है। इसका हृदय कितना विशाल है, इस पर कितने अधिक पुल हैं!
( हिन्दी मासिक ‘सबलोग’ के मार्च 2017 तथा अनहद में प्रकाशित)
(लेखक वरिष्ठ आलोचक, कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के पूर्व प्रोफेसर तथा फिलहाल भारतीय भाषा परिषद के निदेशक हैं।)