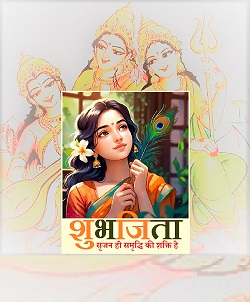दाखिले का मौसम बस चल ही रहा है..मेधा का आधार परीक्षाओं में प्राप्त अधिकतम अंक ही रह गये हैं। नतीजा यह है कि मेधावी विद्यार्थी भी अब 98 प्रतिशत पाकर भी असन्तुष्ट हैं। अधिक से अधिक अंक बटोरने के चक्कर में उनका जीवन अब स्कूल और कोचिंग के बीच सिमटता जा रहा है मगर इसका नतीजा क्या हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इस बीच जिन बच्चों को अच्छे अंक नहीं मिले हैं, उनके बारे में सोचिए…माता – पिता से लेकर रिश्तेदारों और शिक्षण संस्थानों और बोर्ड तक ने यह माहौल बना दिया है जैसे उनको जीने का अधिकार ही नहीं है। बच्चे यही समझ भी रहे हैं और इसलिए बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ने वाले बच्चों को मौत जिन्दगी से अधिक प्यारी लग रही है मगर सोचिए तो क्या ये बच्चों का दोष है? ऐसे ही बच्चे तो नशे की चपेट में आते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं और कई बार अपराध की राह पर निकल पड़ते हैं। कहने को हमें सन्तोष और परिश्रम को धन मानना सिखाया गया है मगर खुद से पूछिए क्या आपकी जिन्दगी का हिस्सा हैं या ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गये हैं? अगर आप अपना हर छोटा काम बनाने के लिए पहुँच, सिफारिश, रिश्वत और ताकत का सहारा ले रहे हैं तो क्या आपको अधिकार है कि आप बच्चों से नैतिकता और विश्वास की उम्मीद करें। अपने बोर्ड को बेहतर बनाने के चक्कर में हर एक बोर्ड, यहाँ तक कि राज्य स्तर के बोर्ड भी परीक्षाओं का अत्यधिक सरलीकृत कर रहे हैं। उनका जोर इस बात पर है कि बच्चों को अधिक से अधिक अंक मिले मगर यह उनकी चिन्ता का विषय नहीं है कि बच्चा क्या सीख रहा है और जीवन की लम्बी दौड़ में ये अंक इस गलाकाट प्रतियोगिता में कहाँ तक साथ दे रहे हैं या दे सकते हैं। हर साल टॉपर आते हैं, जाते हैं मगर कुछ समय बाद वे कही नहीं दिखायी देते। बच्चा बस्ते का बोझ लेकर घूम रहा है मगर उसे जानकारी और व्यावहारिक ज्ञान न के बराबर मिल रहा है। स्कूलों में शिक्षक कई बार बगैर सिखाए मुश्किल प्रोजेक्ट देते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोजेक्ट भी अभिभावक ही पूरा करते हैं। बच्चे ने कुछ नहीं सीखा…एक समय था जब 40 प्रतिशत अंक पाकर भी जीने की लालसा और कुछ करने की उम्मीद बनी रहती थी क्योंकि हमारा जोर सीखने और सिखाने पर रहता था। कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र – छात्राएँ कुछ दिनों तक भले ही अकड़ में रहें मगर बात जब गतिविधियों की होती थी तो उनको भी साथ आना पड़ता था। टॉपर न रहने पर भी तब लिखना सिखाया जाता था, बड़े प्रश्न लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। हिन्दी में शत – प्रतिशत अंक कभी नहीं मिले मगर फिर भी लिखना आ गया…आज शत – प्रतिशत अंक पाने वाले बच्चे भी यह दावा नहीं कर सकते है कि वे लिखना जानते हैं या उनसे त्रुटियाँ नहीं होंगी। वे अपने विषय की पूर्ण जानकारी होने का दावा नहीं कर सकते।

रटन्त विद्या से वे भले ही प्रोजेक्ट प्रदशर्नियों में रटकर सुना दें मगर क्या उनमें समझाने, समूह में सबको साथ लेकर चलने और असफलता को सफलता में बदलने का गुण हैं? क्या आपकी शिक्षा पद्धति अनजाने ही उनको मशीन में नहीं बदल रही है, क्या उनको इतना कमजोर नहीं बना रही है कि वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की बजाय नशे और अवसाद की चपेट में आ रहे? सब जानते हैं कि अंक जीवन की दौड़ में बहुत दूर तक साथ नहीं देते..अगर ऐसा होता तो पढ़े – लिखे युवा अवसाद की चपेट में नहीं आते। अन्ततः आपका आत्मबल ही जीवन में आपका साथ देता है, अंक नहीं देते तो फिर क्यों शिक्षा प्रणाली का जबरन सरलीकरण किया जा रहा है जो घातक है…इससे किसी बोर्ड का भला हो सकता है मगर न तो ये विद्यार्थी के हित में है और न ही देश के भविष्य के लिए फायदेमंद हैं। जरूरी है कि शिक्षा को जड़ों से जोड़ा जाए…हमारी परम्परागत कलाओं और हस्तशिल्प को पाठ्यक्रम में फैशन के लिए ही न रखें…बच्चों को खेत और जंगल दिखाएँ..कारखाने दिखाएँ….। आज कई शिक्षित युवाा अपनी डिग्री को लेकर इतने अधिक मोहग्रस्त होते हैं कि कोई और काम करना उनको अपनी तौहीन लगता है मगर वह ये नहीं जानते कि ऐसा करके वे अवसरों को अपनी सीमा बना रहे हैं जो बाद में उनको एकाकी और हताश ही करेगा। शिक्षा ऐसी हो जो हमारे पारम्परिक क्षेत्रों को मजबूत बनाएँ जिससे किसी किसान को आत्महत्या न करनी पड़े जो मजदूरी को सुरक्षित बनाए और सम्मान बनाए। कारीगर न हों तो कोई भी उद्योग नहीं चल सकता तो श्रम का सम्मान देना भी आवश्यक है और यह शिक्षा प्रणाली के सरलीकरण से नहीं होगा। पढ़ाई के साथ उनके पास विकल्प हो जिससे अगर उनको नौकरी न मिले तो भी उनके लिए रोजगार का अभाव समस्या न बनें। ताकि वे जीवन की वास्तविकता समझें वरना शिक्षा का सरलीकरण घातक ही साबित होगा।