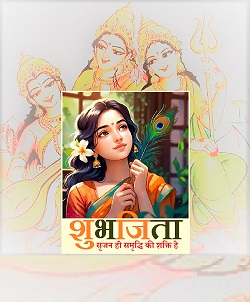भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव आज भी अपने मूल रीति-नीति को नहीं अपना पा रहा है. अब इसे हमारे देश का दुर्भाग्य कहें या दलदली राजनीति का प्रतिफल , यह जनता और राजनेता स्वयं तय करें तो बेहतर होगा! आमतौर पर चुनाव का मूल केंद्रबिंदु राष्ट्र, समाज और जनता के मूल मुद्दों को देखना, समझना उन्हें महसूस करना और सत्ता प्राप्ति के पंचवर्षीय कार्यकालों के दौरान उन तमाम समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए परन्तु यहाँ मामला एकदम इसके उलट दिखाई देता है। सवा सौ करोड़ जनता वाले इस देश में 29 राज्यों के लगभग 500-600 व्यक्ति महज अपना पद- रुतबा और अपनी तिजोरी को लक्ष्य मानकर उन्हें बनाने और बचाने के लिए जाने कितने वादें, झूठ फरेब, घड़ियाली आँसू, दो चार दस पद यात्राएं, अपशब्द, बेतुके, विषाक्त, हीनता-नीचता, अमर्यादित भाषा, उपाधियों एवं जुमलों से परिपूर्ण गलाफाड़ भाषण देने को अनिवार्य प्रक्रिया मानकर दंगे, फसाद भड़का कर अपनी रोटी सेंकने में विश्वास रखते हैं और कदाचित इसको लक्ष्य मानकर चंद दिनों की “जी तोड़ मेहनत” करके अगले पाँच सालों तक इसका फल भी जम कर खाते हैं एवं अपने घर-परिवार, रिश्ते-नातेदारों, करीबियों को खिलाते भी हैं और जनता वापस से चली जाती है वहीं जहां ये राजनेता चाहते हैं ‘भाड़’ में।
यदि हम तनिक भी सचेतनता की दृष्टि से जाति, धर्म,वर्ग और लिंग के घेरे से बाहर निकल कर देखें तो वर्तमान समय में किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में जनता की वास्तविक और जमीनी समस्याओं से जुड़े मुद्दें नजर नहीं आयेंगे। हर जगह सिर्फ एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप , बेतुकी बातें और बड़प्पन वाले जुमले ही कभी टिमटिम करते तो कभी भकभकातें हुए आँखों को चौंधियाने वाले प्रतीत होते हैं. हर संस्था यहां किसी न किसी अन्य संस्था का या तो चाटुकार या तो धुर विरोधी ही नज़र आता है।
हर दल हरेक पार्टी भ्रष्टाचार और एक से बढ़ कर एक जुमलेबाज़ी के अथाह समुद्र में गोते लगाता नजर आता है। मूलभूत समस्याएं जैसे – रोजगार , शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि गड़े मुर्दे की भांति ही नज़र आते हैं। चुनाव आते ही इन मुर्दों के ताबूत को कभी-कभी साफ़ सफाई के बहाने याद कर लिया जाता है किन्हीं तथाकथित सजग और जनप्रिय ‘नेता’ के द्वारा, तत्पश्चात परिणाम वही “ढाक के तीन पात” रहते है।
कहीं न कहीं जनता की भी उदासीनता इसका एक कारण है परन्तु इससे कही अधिक यह ‘दलदली राजनीति’ और ‘वंश के दंश’ से आहत जुगलबंदी का परिणाम है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ‘लोकतंत्र का यह महापर्व’ जिसे हम चुनाव कहते है वह महज सतारूढ़ होने की लाॅटरी हो गई है या यूँ कहें कि बाहुबलियों और समर्थ व्यक्तियों द्वारा अपनी किस्मत को आजमाने का पंचवर्षीय अनुष्ठान बन गया है जिसमें हर प्रत्याशी येन-केण-प्रकारेण सफल होना चाहता है, जिसमें जनता एवं उनके और तमाम जरूरी मुद्दें इस अनुष्ठान की हवन सामग्री बन जाती है जिसे इनके चुनाव प्रचार के सभारुपी कुंड में ‘स्वाहा-स्वाहा’ के मंत्र के साथ प्रविष्ट किया जाता है और सत्तासीन सरकारों का जो दावा होता है कि विगत पाँच सालों में उनकी उपलब्धियां ‘ऐसी रही –वैसी रही’ वो महज इस आयोजित अनुष्ठान का वो बासी प्रसाद सिद्ध होता है जिसे जाने कितने आशावादी भक्तों की हथेली प्राप्त भी नहीं कर पाती , न जाने कितने मुंह भी इस प्रसाद से अछूते रह जाते हैं!
तो इस तरह ये चुनावी महापर्व (अनुष्ठान) खुद ही एक दायरे में जाने कितनी वर्जनाओं में जकड़ा हुआ है तो फिर इसका फल भला विशुद्ध कैसे हो! ये हम जनता जनार्दन स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि “चुनाव को महज चुनाव” ही रहने दिया जाए। इसे ना तो भगवा में रंग कर देखा जाय, ना ही बिना सोचे समझे हाथ का साथ मिलना चाहिये, ना बिना आकलन के लाल मान लिया जाए , ना ही बिना पड़ताल के हरा बना दिया जाय अर्थात इसे इसकी ‘सफेदी’ मतलब मूल तिरंगे के रूप में ही रहने दिया जाय एवं “जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा” उक्ति के वास्तविक स्वरुप तक पहुँचने दिया जाय। तभी चुनाव का यह महापर्व सफल और सार्थक हो सकता है।