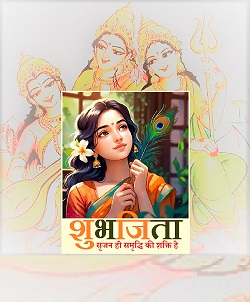यज्ञों एवं कर्मकाण्डों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली-भांति समझने के लिए ही इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। यहाँ पर ‘ब्रह्म’ का शाब्दिक अर्थ हैं- यज्ञ अर्थात् यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ‘ब्राह्मण ग्रंथ’ कहे गये। ब्राह्मण ग्रन्थों में सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक तथा अध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गयी है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे हुए हैं। इनमें उत्तरकालीन समाज तथा संस्कृति के सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक वेद (संहिता) के अपने-अपने ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थो से हमें परीक्षित के बाद और बिम्बिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ‘ऐतरेय ब्राह्मण’ में ‘राज्याभिषेक’ के नियम दिये गये हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ‘वैदिक साहित्य’ में ‘ऋग्वेद’ के बाद ‘शतपथ ब्राह्मण’ का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरू, पांचाल, कोशल, विदेश आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है।
वेद और संबंधित ब्राह्मण
वेद सम्बन्धित ब्राह्मण
1- ऋग्वेद
ऐतरेय ब्राह्मण, शांखायन या कौषीतकि ब्राह्मण
2- शुक्ल यजुर्वेद
शतपथ ब्राह्मण
3- कृष्ण यजुर्वेद
तैत्तिरीय ब्राह्मण
4- सामवेद
पंचविंश या ताण्ड्य ब्राह्मण, षडविंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण
5- अथर्ववेद
गोपथ ब्राह्मण
पृष्ठभूमि
उत्तर वैदिककाल में, जब वैदिक संहिताएँ धीरे-धीरे दुर्बोध होती चली गईं, मन्त्रार्थ-ज्ञान केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित रह गया, उस समय यह आवश्यकता गहराई से अनुभव की गई कि वेद-मन्त्रों की विशद व्याख्या की जाय्। यही स्थिति वैदिक-यज्ञों के कर्मकाण्ड की भी थी। सुदीर्घकाल तक यागों का अनुष्ठान मौखिक ज्ञान के आधार पर ही होता रहा, लेकिन शनै:शनै यज्ञ-विधान जब जटिल और संश्लिष्ट प्रतीत होने लगा तथा स्थान-स्थान पर सन्देह और शंकाओं का प्रादुर्भाव होने लगा, तब इस सन्दर्भ में स्थायी आधार की आवश्यकता अनुभव हुई। ब्रह्मवादियों (यज्ञवेत्ताओं) के मध्य यागीय विसंगतियों के निराकरण के लिए सम्पन्न चर्चा-गोष्ठियों, परिसंवादों तथा सघन विचार-विमर्श ने ब्राह्मण-ग्रन्थों के प्रणयन का मार्ग विशेष रूप से प्रशस्त किया। किसी भी युग के साहित्य के मूल में, तत्कालीन सांस्कृतिक विचारधारा, राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता, आस्थाओं, आदर्शों एवं मूल्यों की अभिव्यक्ति का दुर्निवार्य आग्रह स्वभावत: सत्रिहित रहता है। ब्राह्मण-साहित्य के अन्तर्दर्शन की पृष्ठभूमि में भी, निश्चित ही यह आकांक्षा निहित रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वेद-मन्त्रों की सुगम व्याख्या करने, यज्ञीय विधि-विधान के सूक्ष्मातिसूक्ष्म पक्षों को निरूपित करने तथा समकालीन वैचारिक आन्दोलन को दिशा देने की भावना मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रन्थों के साक्षात्कार की पृष्ठभूमि में निहित रही है।
ब्राह्मण शब्द का अर्थ
मन्त्र-भाग से अतिरिक्त शेष वेद-भाग ब्राह्मण है, जैसा कि जैमिनि का कथन है-‘शेषे ब्राह्मणशब्द’।[1] माधवाचार्य तथा सायणाचार्य ने भी इसी लक्षण से सहमति व्यक्त की है।[2] कोश ग्रन्थों के अनुसार वेद-भाग का ज्ञापक ‘ब्राह्मण’ शब्द नपुंसक लिङ्ग में व्यवहार्य है।[3] इसका अपवाद केवल महाभारत का एक स्थल है, जहाँ पुल्लिंग में भी यह प्रयुक्त है।[4] ग्रन्थ के अर्थ में ‘ब्राह्मण’ शब्द का प्राचीन प्रयोग तैत्तिरीय संहिता में है।[5] पाणिनीय अष्टाध्यायी[6], निरुक्त[7] तथा स्वयं ब्राह्मण ग्रन्थों में तो एतद्विषयक पुष्कल प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं।[8] व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह ‘ब्रह्म’ शब्द से ‘अण्’ प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है। इस सन्दर्भ में सत्यव्रत सामश्रमी का अभिमत है कि ‘ब्राह्मण’ शब्द से ही प्रोक्त अर्थ में ‘अण्’ प्रत्यय लगकर ‘ब्राह्मण’ शब्द बना है।[9] ‘ब्रह्म’ शब्द के दो अर्थ हैं- मन्त्र तथा यज्ञ।[10] इस प्रकार ब्राह्मण वे ग्रन्थ विशेष हैं, जिनमें याज्ञिक दृष्टि से मन्त्रों की विनियोगात्मिका व्याख्या की गई है।[11] जिन मनीषियों ने ब्राह्मणों का मन्त्रवत् प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया है, वे भी इन्हें वेद-व्याख्यान रूप मानते हैं।[12]
श्रुतिरूपता
आचार्य आपसम्ब ने मन्त्रभाग के साथ ही ब्राह्मणभाग को भी वेद ही माना है-मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् (यज्ञपरिभाषा)। इसी का अनुसरण करते हुए शबरस्वामी पितृभूति, शंकराचार्य, भट्ट कुमारिल, भवस्वामी, देवस्वामी, विश्वरूप, मेधातिथि, कर्क, धूर्तस्वामी, देवत्रात, वाचस्पति मिश्र, राजशेखर, रामानुज, उवट, मस्करी और सायणाचार्य सहित बहुसंख्यक महान् आचार्यों और भाष्यकारों ने मन्त्र-संहिताओं के साथ ही ब्राह्मणों की भी श्रुतिरूपता पर बल दिया है।[13] पाणिनी और पतञ्जलि की भी यही अवधारणा है। इस आस्था का एक प्रमुख हेतु यह भी है कि आरण्यक और अधिकांश उपनिषद-ग्रन्थ ब्राह्मण-ग्रन्थों के ही अन्तिम भाग हैं और भारतीय दर्शनों का विशाल प्रासाद उपनिषदों की ही आधारभित्ति पर निर्मित है। ब्रह्मसूत्र, गीता और अन्य दार्शनिक सूत्रग्रन्थ पग-पग पर इनके प्रामाण्य पर अवलम्बित हैं। ऐसी स्थिति में भाष्यकर शंकराचार्य द्वारा ताण्ड्य ब्राह्मण के उद्धरण को ‘ताण्डिनां श्रुति:’ रूप में उपस्थापित करना स्वाभाविक ही था। आज भी वेदज्ञों का एक विशाल वर्ग इस मान्यता पर श्रद्धावान् दिखलाई देता है।[14]
स्वरूप और उनके प्रवचनकर्ता
ब्राह्मण-ग्रन्थों का वर्तमान स्वरूप प्रवचनात्मक और व्याख्यात्मक है। विधियों और उनके हेतु प्रभृति का निरूपण प्रवचनात्मक अंशों में है तथा विनियुक्त मन्त्रों के औचित्य का प्रदर्शन व्याख्यात्मक ढ़ग से है। दीर्घकाल तक मौखिक परम्परा से प्रचलित यज्ञीय कर्मकाण्ड का संकलन तो इनमें है ही, ब्रह्मवादियों के मध्य विद्यमान वाद-विवाद के अंशों की झलक भी यत्र-तत्र मिल जाती है। आधुनिक युग में, स्वामी दयानन्द सरस्वती और उनके आर्य समाज में दीक्षित विद्वानों ने, ब्राह्मण-ग्रन्थों को वेद न मानकर वेदव्याख्यान ग्रन्थ भर माना है। इन विचारकों की दृष्टि में, पशु-हिंसा और कहीं-कहीं यागगत अश्लील कृत्यों का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों को अपौरुषेय वेद की श्रेणी में सम्मिलित करने में बाधक है। इस विवाद में उलझे बिना भी, यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मन्त्र-संहिताओं की तुलना में ये वेद नहीं, तो ‘वेदकल्प’ तो हैं ही। ब्राह्मण-ग्रन्थों को श्रुतिस्वरूप स्वीकार करने वाले मनीषियों ने संहितावत् इन्हें भी अपौरुषेय ही माना है। उनकी मान्यता है कि इनका भी साक्षात्कार किया गया। जिन व्यक्तियों के नाम इनसे सम्बद्ध हैं, वे इनके रचयिता न होकर प्रवचनकर्ता ऋषि अथवा आचार्य हैं, जिन्होंने इन्हें संप्रेषित किया। भिन्न-भिन्न ब्राह्मण-ग्रन्थों के प्रवक्ता भी पृथक्-पृथक् हैं, जिनका परिचय उन ब्राह्मण ग्रन्थों के विशिष्ट विवरण के साथ प्रदेय है। यों संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि प्रवचनकर्ताओं में से कुछ ॠषि श्रेणी के हैं और अन्य आचार्य-परम्परा के। शतपथ के प्रवचनकर्ता याज्ञवल्क्य ॠषि हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास आचार्य माने जाते हैं।
प्रतिपाद्य विषय
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ब्राह्मणग्रन्थों का मुख्य विषय यज्ञ का सर्वांगपूर्ण निरूपण है। इस याग-मीमांसा के दो प्रमुख भाग हैं- विधि तथा अर्थवाद। ‘विधि’ से अभिप्राय है यज्ञानुष्ठान कब, कहाँ और किन अधिकारियों के द्वारा होना चाहिए। याग-विधियाँ अप्रवृत्त कर्मादि में प्रवृत्त कराने वाली तथा अज्ञातार्थ का ज्ञापन कराने वाली होती हैं। इन्हीं के माध्यम से ब्राह्मणग्रन्थ कर्मानुष्ठानों में प्रेरित करते हैं, जैसा कि आपस्तम्ब का यज्ञपरिभाषा[15] में कथन है-‘कर्मचोदना ब्राह्मणानि’। विधि का स्तुति और निन्दारूप में पोषण तथा निर्वाह करने वाले ब्राह्मणगत अन्य विषय अर्थवाद कहलाते हैं अर्थवादपरक वाक्यों में यज्ञनिषिद्ध वस्तुओं की निन्दा तथा यज्ञोपयोगी वस्तुओं की प्रशंसा रहती है। इस प्रकार के वाक्यों की विधि-वाक्यों के साथ ‘एकवाक्यता’ का उपपादन मीमांसकों ने किया है-विधिना तु एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु:[16] उनके अनुसार विधि और अर्थवाद वचनों के मध्य परस्पर शेषशेषिभाव अथवा अङ्गाङिगभाव है। अत: शबरस्वामी के मतानुसार वस्तुत: विधियाँ ही अर्थवादादि के रूप में ब्राह्मण ग्रन्थों में दस प्रकार से व्यवह्रत हुई हैं-
हेतुर्निर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधि:।
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना॥
उपमानं दशैवैते विधयो ब्राह्मणस्य तु।
एतद्वै सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम्[17]
इनका सोदाहरण स्पष्टीकरण इस प्रकार है-
हेतु
कर्मकाण्ड सम्बन्धी किसी विशिष्ट विधि की पृष्ठभूमि में निहित कारणवत्ता का निर्देश, यथा ‘तेन ह्यन्नं क्रियते'[18], अर्थात् सूप से होम करना चाहिए, क्योंकि उससे अन्न को तैयार किया जाता है।
निर्वचन
व्युत्पत्ति के माध्यम से याग में प्रयोज्य पदार्थ की सार्थकता का निरूपण, यथा-तद्दध्नो दधित्वम्[19] यही दही का दहीपन है।
निन्दा
किसी अप्रशस्त वस्तु की निन्दा कर याग में उसकी अनुपादेयता का प्रतिपादन करना; यथा-‘अमेध्या वै माषा:'[20] उड़द यज्ञ की दृष्टि से अनुपादेय है।
प्रशंसा
वायु के निमित्त क्यों यागानुष्ठान किया जाय, इसका प्रतिपादन इस रूप में किया गया है कि वायु शीघ्रगामी देवता है-वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता।[21]
संशय
इसका तात्पर्य है सन्देह, जैसे यजमान के भीतर यह सन्देह उत्पन्न हो जाए कि मैं होम करूँ कि नहीं? तदव्यचिकित्सज्जुहुवानी इमा हौषादूम्।[22]
विधि
औदुम्बरी (गूलर की वह शाखा, जिसके नीचे बैठकर उदगातृमण्डल सामगान करता है) कितनी बड़ी होनी चाहिए, इस विषय में यह विधान मिलता है कि वह यजमान के परिमाण (नाप) की होनी चाहिए-यजमानेन सम्मिता औदुम्बरी भवति।[23]
परकृति
इसका अभिप्राय है दूसरे का कार्य, यथा-माषानेव मह्यं पचति[24] वह मेरे लिए उड़द ही पकाता है।
पुराकल्प
तात्पर्य है पुराना आख्यान, जैसे-पुरा ब्राह्मणा अभैषु:[25] प्राचीन काल में ब्राह्मण डर गये।
व्यवधारणकल्पना
अभिप्राय है विशेष प्रकार का निश्चय करना। इसका उदाहरण है कि जितने घोड़ों का प्रतिग्रह करे, उतने ही वरुणदेवताक चतुष्कपालों से याग करे-यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात्तावतो वरुणान् चतुष्कपालार्न्निवपेत्।[26]
उपमान
शबरस्वामी ने यद्यपि इसका उदाहरण नहीं दिया है, तथापि छान्दोग्य उपनिषद[27] के इस अंश को प्रस्तुत किया जा सकता है-
स यथा शकुनि: सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयते, एवमेव खलु सोम्य! तन्मनो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतन्मलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते, प्राणबन्धनं हि सोम्य! मन इति।
-हे सोम्य! जैसे धागे से बँधा हुआ पक्षी हर दिशा की ओर जाकर और अन्यत्र आश्रय न पाकर बन्धन का अवलम्ब लेता है; इसी प्रकार से है सोम्य! यह मन विभिन्न दिशाओं में भटकने के बाद वहाँ, आश्रय न पाकर इस प्राण का अवलम्बन ग्रहण करता है। हे सोम्य! मन का बन्धन प्राण है।
विधि और अर्थवाद-वाक्यों की एकवाक्यता को स्पष्ट करने के लिए ताण्ड्य महाब्राह्मण से एक उदाहरण प्रस्तुत है- षष्ठ अध्याय के सप्तम खण्ड में अग्निष्टोमानुष्ठान की प्रक्रिया में बहिष्पवमान स्तोत्र के निमित्त अध्वर्यु की प्रमुखता में उद्गाता प्रभृति पाँच ॠत्विजों के सदोमण्डप से चात्वाल-स्थान तक प्रसर्पण का विधान है-बहिष्पवमानं प्रसर्पन्ति। इस प्रसर्पण के सन्दर्भ में दो नियम विहित हैं- क्वाण (मृदुपदन्यासपूर्वक) प्रसर्पण तथा वाङनियमन्। साथ ही पाँचों ॠत्विजों-अध्वर्यु, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा ब्रह्मा के एक दूसरे के पीछे इसी क्रम से पंक्तिबद्ध होकर चलने का विधान है, क्योंकि यह पंक्ति है।[28] वहीं इन नियमों के पालन से यज्ञ की शान्ति बनी रहने, और अन्य लाभों तथा हेतुओं का उल्लेख है। नियमों का पालन न करने से अनेकविध अनर्थों की सम्भावना भी उल्लिखित है। इस प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्थों में यागानुष्ठान की विभिन्न विधियों के निरूपण में प्रशंसा और निन्दा ही नहीं, उनके औचित्य-बोधक हेतु भी दिये गये हैं। उदाहरणार्थ अग्निष्टोम याग के ही प्रसंग में ताण्ड्य-ब्राह्मण में उद्गाता के द्वारा सदोमण्डप में औदुम्बरी[29] के उच्छ्रयण का विधान करते समय कहा गया है कि प्रजापति ने देवों के निमित्त अर्क् का जो विभाजन किया, उसी से उदुम्बर की उत्पत्ति हुई। अत: उदुम्बर वृक्ष प्रजापति से सम्बद्ध है और उद्गाता का भी उससे सम्बन्ध है, इसलिए जब वह औदुम्बरी का उच्छ्रयण रूप प्रथम कृत्य करता है, तब वह उसी प्रजापति नाम्नी अधिष्ठात्री दैवी शक्ति के द्वारा अपने को आर्त्विज्य-हेतु वरण कर लेता है। इसी प्रसंग में द्रोणकलशप्रोहण, जिस कृत्य के अन्तर्गत द्रोणकलश में सोम रस चुराकर रथ के नीचे रखा जाता है, का समर्थन एक आख्यायिका के द्वारा किया गया है। तदनुसार प्रजापति ने अनेक होने के लिए सृष्टि-कामना की। सृष्टिविषयक विचार करते ही उनके मस्तक से आदित्य की उत्पत्ति हुई। आदित्य ने स्वयं उत्पन्न होने के लिए प्रजापति के शिर को छिन्न कर दिया। वह छिन्न-भिन्न मूर्द्धा ही द्रोणकलश हो गया, जिसमें देवों ने शुभ्रवर्ण के चमकते हुए सोमरस को ग्रहण किया।[30] इस आख्यायिका के माध्यम से द्रोणकलश और तत्रस्थ सोमरस में सर्जनाशक्ति से ओतप्रोत श्रेष्ठ मानसिक सामर्थ्य के अस्तित्व का उपपादन किया गया है।
इस प्रकार विधि-निर्देश के समानान्तर ही ब्राह्मण-ग्रन्थ उनकी उपयुक्तता भी विभिन्न प्रकार से बतला देते हैं। इस सन्दर्भ में यागों, उनकी अनुष्ठान-विधियों, द्रव्यों, सम्बद्ध देवों और विनियुक्त मन्त्रों का छन्द आदि के द्वारा औचित्य-निरूपण करते समय ब्राह्मण-ग्रन्थों के रचयिता मानवीय भावनाओं और मनोविज्ञान का सदैव ध्यान रखते हुए यजमान के सम्मुख उस कृत्य विशेष के अनुष्ठान से होने वाली लाभ-हानि का यथावत् विवरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। अग्निष्टोम याग का अनुष्ठान व्यक्ति क्यों करें? उससे क्या लाभ हो सकता है? इसे जाने बिना व्यक्ति मानवीय स्वभाव के अनुसार यज्ञ में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता। इस बिन्दु पर ब्राह्मणग्रन्थ उसे आश्वस्त कर देते हैं कि यह वस्तुत: समस्त फलों का साधन होने के कारण मुख्य है, इसके विपरीत अन्य याग एक-एक फल देने वाले हैं, इसलिए अग्निष्टोम के अनुष्ठान से समस्त फल प्राप्त होते हैं।[31] इस सामान्य निर्देश के अनन्तर विस्तार से यह बतलाया गया है कि इसके अनुष्ठान से पशु-समृद्धि, ब्रह्मवर्चस्-प्राप्ति आदि पृथक्-पृथक् फलों की प्राप्ति भी हो सकती है।
जहाँ तक विभिन्न यज्ञ-कृत्यों में विनियुक्त मन्त्रों के औचित्यप्रदर्शन की बात है, ब्राह्मणग्रन्थ उस बिन्दु के अनावरण का पूर्ण प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण उस मन्त्रविशेष का किसी कृत्यविशेष में विनियोग किया गया है। ब्राह्मण-ग्रन्थों की पारिभाषिक शब्दावली में यह रूप-समृद्धि कहलाती है। रूप-समृद्धि, जिसका स्थूल अभिप्राय क्रियमाण कर्म के साथ विनियुक्त मन्त्र का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, से स्वयं यज्ञ समृद्ध होता है।[32] इस प्रकार रूप-स्मृद्धि का वास्तविक तात्पर्य तत्तत् विशिष्ट कृत्य के सन्दर्भ में विनियुक्त मन्त्र की सार्थकता का प्रदर्शन है। जहाँ सीधे विनियुक्त स्तोत्रिया के अर्थ से औचित्य की प्रतीति नहीं हो पाती, वहाँ ब्राह्मणग्रन्थ मन्त्रगत देवों से कृत्य को सम्बद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए किसी दीर्घरोगी की रोग-निवृत्ति के लिए[33] में ‘आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्। मध्वा रजांसि सुक्रतू'[34] मन्त्र का विनियोग है। आपातत: इस ऋक् के अर्थ से रोग-निवृत्ति का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है, किन्तु यहाँ भी प्रकारान्तर से सम्बन्ध निरूपित है। ताण्ड्य ब्राह्मणकार का कथन है कि दीर्घरोगी के प्राण और अपान अपक्रान्त हो जाते हैं, जबकि प्राण और अपान की समान स्थिति पर ही आरोग्य निर्भर है। प्राण और अपान की तथाकथित समस्थिति मित्र और वरुण की अनुकूलता पर अवलम्बित है, क्योंकि इन दोनों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्राणापान वस्तुत: अहोरात्ररूप है और दिन के देव मित्र है तथा रात्रि के वरुण। इन दोनों के आनुकूल्य अर्जुन से शरीर में प्राण और अपान की यथावत् स्थिति बनी रहती है। अत: दीर्घरोगी की रोग-निवृत्ति के सन्दर्भ में उपर्युक्त ऋक् का गान सर्वथा उपयुक्त है। इनके साथ ही ब्राह्मणग्रन्थों में निरुक्तियाँ और आख्यायिकाएं भी पुष्कल परिमाण में प्राप्त होती हैं।