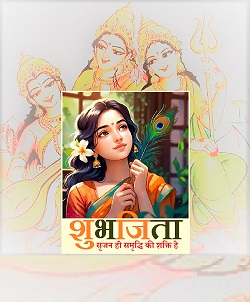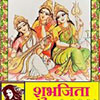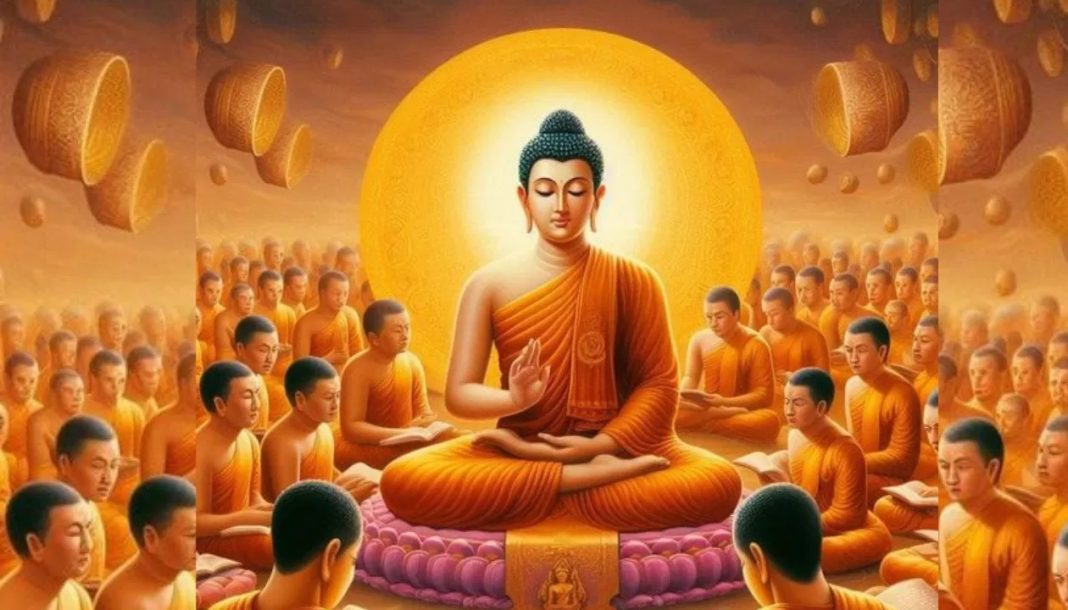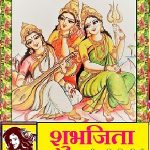प्रागैतिहासिक काल से ही भारत विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का आश्रय रहा है। विभिन्न प्रवृतियों तथा जीवन विधाओं के संघर्ष और समन्वय के द्वारा भारतीय इतिहास की प्रगति और संस्कृति विकास हुआ है। आर्य तथा आर्येतर जातियों की सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय भारतीय सभ्यता के निर्माण की आधार शिला रही है जिसका प्रभाव एक ओर वैदिककालीन समाज रचना पर पड़ा और दूसरी ओर बौद्ध धर्म पर पड़ा जो बौद्धिक और आध्यात्मिक आंदोलन का चरम परिणाम है।
563 ईसा पूर्व के आसपास सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है और थेरवादी बौद्ध मत के अनुसार बुद्ध का परिनिर्वाण 544 ईसा पूर्व हुआ। बुद्ध के उपदेशों ने इस संसार को एक नया अध्याय दिया जो ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ की भावना से परिपूर्ण है। यह युग भारतीय विचार जगत में उथल पुथल का युग था। सामाजिक एवं धार्मिक नव चेतना के लिए बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने संसार को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया जो भव व्याधि से पीड़ित मानव के लिए वरदान हो गया। धार्मिक जगत में संघीय जीवन पद्धति का प्रसार हुआ जिसका अवांतरकालीन संप्रदायों में बडा़ प्रभाव पडा़। इस युग में कई नये मतों का प्रदुर्भाव हुआ जिन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों, कुरीतियों तथा अंधविश्वासों के प्रतिकार का मार्ग प्रशस्त किया। जातिवाद का सर्वप्रथम विरोध करने वाले बुद्ध और महावीर ही थे। वेद और ब्राह्मणों को चुनौती दी। बुद्ध तथा महावीर के धर्मोपदेश जनता की भाषा में दिए गए अतः वे सभी बोधगम्य हो सके। ब्राह्मण ग्रंथ दुरूह होने के कारण जनता के लिए दुर्बोध हो गए थे। अतः नवीन विचारों का जन मानस पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा। भगवान् बुद्ध के धर्मोपदेशों का राजा तथा जनता दोनों ने स्वागत किया। बुद्ध के समकालीन अनेक प्रमुख ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, इस मत के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ बनाया। भगवान् बुद्ध ने सर्व बोधगम्य और सुधारक के रूप में समाज में अपने दर्शन को लोगों में प्रसारित किया। इसी कारण बौद्ध धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ और वह अपने युग की चेतना को बहुत अधिक प्रभावित कर सका। बौद्ध मत के व्यापक प्रचार के फलस्वरूप बुद्ध निर्वाण के तुरंत बाद बुद्ध वचनों का संकलन राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति की बैठक में, फिर बुद्ध निर्वाण के एक शताब्दी बाद वैशाली में हुई बैठक में हुई ऐसा माना जाता है। सम्राट अशोक के समय पालि पिटक का संकलन कर सद्धर्म अथवा थेरवाद के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया गया जिसका प्रमाण दीपवंश और महावंश ग्रंथों में मिलता है। यह संगीति बैठक बुद्ध निर्वाण के 236 वें वर्ष में पाटलिपुत्र में मोग्गलिपुत्त तिस्स के सभापतित्व में हुई जिसमें एक सहस्र बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। कुमार महेंद्र पालि पिटक की एक प्रति लंका ले गए थे। पांचवीं शताब्दी ईसा सन् में लंकाधिपति बट्टगामनी ने उसका पुनः संकलन करवाया जो बहुमूल्य निधि है।
उपनिषद युग के बाद बुद्ध का समय है। गौतम बुद्ध का महत्व संसार व्यापी है, उनके उपदेशों ने पश्चिमी एशिया में धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक क्रांति का सूत्रपात किया था। बुद्ध की ज्ञान एवं कर्म की विचारधारा ने प्रसिद्ध दार्शनिकों एवं शासकों को प्रभावित किया। गौतम बुद्ध के दिव्य आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों से प्रभावित होकर एक ओर अश्वघोष, बुद्ध घोष, कुमार लब्ध, दिंङ्नाग, असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, शांति देव जैसे तार्किक और दार्शनिक पुरुष पैदा हुए तो दूसरी ओर अशोक, कनिष्क और हर्ष वर्धन संसार के कल्याण के लिए कर्म योगी पुरुष बने। बुद्ध के निर्वाण के 200 वर्षों के अंदर ही बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, वज्रयान, सहज यान चार संप्रदायों का और अट्ठारह निकायों स्थविरवाद,वज्जिपुत्तक, महीशासक, धर्मोत्तरीय, भद्रपाणिक, छन्नागरिक, सम्मितीय, धर्म गुप्तिक, सर्वास्तिवादी, काश्यपीय, सांक्रातिक, सूत्रवादी, (सौत्रांतिक), महसांघिक, व्यावहारिक, गोकुलिक, प्रज्ञप्तिवादी, बाहुश्रुतिक, चैत्यवादी का विकास हुआ। विभिन्न संप्रदायों और मतों के बावजूद भी बौद्ध धर्म आज पूरे विश्व में लोकप्रिय धर्म है। बौद्ध दर्शन का उदय बौद्ध धर्म से माना जाता है। विद्वानों और बौद्ध आचार्यों ने बौद्ध धर्म के दो रूप बताए हैं पहला शुद्ध धार्मिक रूप जिसमें आचार संबंधी नैतिक एवं सामाजिक आदर्शों का सरलतम प्रतिपादन किया गया है। भगवान् बुद्ध के उपदेश एवं शिक्षाएं इसी धार्मिक रूप में मिलती हैं। बौद्ध धर्म का दूसरा दार्शनिक रूप है जिसमें बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक रूपरेखा को आध्यात्मिक व्याख्या के रूप में स्पष्ट किया गया है।
बुद्ध के मूल सिद्धांत या विचार – –
बुद्ध के मूल वचनों या उपदेशों के सिद्धांतों को ही समझने की कोशिश की गई है जो बोधि उपदेश हैं।
बुद्ध के उपदेशों को जानने के लिए बुद्ध के मूल सिद्धांतो को जानना आवश्यक है जिनमें तीन अस्वीकारात्मक हैं और एक स्वीकारात्मक। ये चार सिद्धांत इस प्रकार हैं – –
1-ईश्वर को नहीं मानना अन्यथा मनुष्य स्वयं अपना मालिक है
2- आत्मा को नित्य मानना अन्यथा नित्य एक रस मानने पर उसकी परिशुद्धि और मुक्ति के लिए गुंजाइश नहीं रहेगी।
3-किसी अन्य को स्वतः प्रमाण नहीं मानना अन्यथा बुद्धि और अनुभव की प्रामाणिकता जाती रहेगी।
4- जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक सीमित मानना अन्यथा जीवन और उसकी विचित्रताएं कार्य – कारण नियम से उत्पन्न न हो कर सिर्फ आकस्मिक घटनाएँ रह जाएंगी
ईश्वर को न मानना – – -बच्चे की उत्पत्ति के साथ उसके जीवन का आरंभ होता है।बच्चा शरीर और मन का समुदाय मात्र है। शरीर भी कोई एक इकाई मात्र नहीं बल्कि एक काल में भी असंख्य अणुओं का समुदाय है। अणु भी क्षण क्षण बदल रहा है और उनकी जगह दूसरे उनके समान ही अणु उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार शरीर भी परिवर्तित होता जाता है। शरीर की तरह मन भी परिवर्तित होता जाता है। मन का परिवर्तन सूक्ष्म रूप से होता है क्योंकि मन सूक्ष्म होता है और पूर्वापर रूपों का भेद भी सूक्ष्म होता है इसलिए उस भेद को समझना भी दुष्कर है। आत्मा और मन एक ही है और क्षण क्षण दोनों में परिवर्तन होता है। इस कार्य कारण का संबंध जन्म से मरण तक अटूट दिखाई पड़ता है। आकस्मिक रूप से कुछ घटित नहीं होता बल्कि कार्य कारण के सिद्धांत से भी इन्कार करना होता है जिसके बिना कोई बात सिद्ध नहीं की जा सकती। यदि कहें कि माता-पिता से उत्पन्न पुत्र का शरीर, मन उनके अनुरूप ही होगा तो यह पूरी तरह से ठीक नहीं है। प्रतिभाशाली माता-पिता के मंदबुद्धि और मंदबुद्धि माता-पिता के प्रतिभाशाली संतान कैसे होती। जिस प्रकार खान से निकला लोहा भी अलग अलग संस्कार लिए होता है उसी प्रकार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि फौलाद की तरह पूर्व जीवन के अभ्यास का परिणाम कहा जा सकता है। इस शरीर का जीवन प्रवाह एक सुदीर्घ जीवन प्रवाह का छोटा सा बीज का अंश है जिसका पूर्व कालिक प्रवाह चिरकाल से चला आ रहा है बाद के काल तक भी चिरकाल ही रहेगा। जीवन का यह प्रवाह इस शरीर से पूर्व से आ रहा है और पीछे भी रहेगा तो भी अनादि और अनंत नहीं है। इसका आरंभ तृष्णा या स्वार्थपरता से है। तृष्णा के क्षय के साथ ही इसका क्षय हो जाता है।
जीवन प्रवाह में प्रवाहित मनुष्य अपने जीवन को अच्छा बुरा बना सकता है। यह सिद्धांत व्यक्ति के लिए भविष्य को आशा मय बनाने के लिए सुंदर उपाय है।
बुद्ध की शिक्षा और दर्शन इन चारों सिद्धांतों पर अवलंबित है। प्रथम तीन सिद्धांत बौद्ध धर्म को दुनिया के अन्य धर्मों से पृथक करते हैं। ये तीनों सिद्धांत भौतिकवाद और बुद्ध धर्म में समान हैं किंतु चौथी अर्थात् जीवन प्रवाह के इसी शरीर तक परिसीमित न मानना, इसे भौतिकवाद से अलग करता है और साथ ही मनुष्य को अच्छा बनने के लिए विकसित करता है। मनुष्य परतंत्रता से मुक्त हो जीवन के प्रति आशावादी होता है और शील सदाचार के लिए नींव बनाता है। चारों सिद्धांतों का सम्मिलन ही बुद्ध धर्म और धर्म उपदेश है।