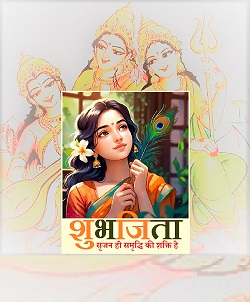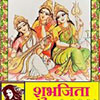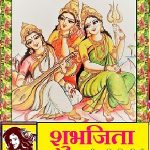समय के साथ हमारे परंपरागत त्योहार अपना स्वरूप बदलते जाते हैं, और बहुधा उनका परंपरागत स्वरूप याद ही नहीं रहता। आज जहां दीपावली का अर्थ रंग-बिरंगी बिजली की लड़ियों से घरों-प्रतिष्ठानों को सजाना, महंगी से महंगी आसमानी कान-फोड़ू ध्वनियुक्त आतिषबाजी से अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करना और अनेक जगह सामाजिक बुराई-जुवे को खेल बताकर खेलने और दीपावली से पूर्व धनतेरस पर आभूषणों और गृहस्थी की महंगी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं को खरीदने के अवसर के रूप में जाना जाता है, ऐसा अतीत में नहीं था। खासकर कुमाऊं अंचल में दीपावली का पर्व मौसमी बदलाव के दौर में बरसात के बाद घरों को साफ-सफाई कर गंदगी से मुक्त करने, घरों को परंपरागत रंगोली जैसी लोक कला ‘ऐपण’ से सजाने तथा तेल अथवा घी के दीपकों से प्रकाशित करने का अवसर था। मूलतः ‘च्यूड़ा बग्वाल” के रूप से मनाए जाने वाले इस त्योहार पर कुमाऊं में बड़ी-बूढ़ी महिलाएं नई पीढ़ी को सिर में नए धान से बने ‘च्यूड़े’ रखकर आकाश की तरह ऊंचे और धरती की तरह चौड़े होने जैसी शुभाशीषें देती थीं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रकृति एवं पर्यावरण से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला पूरा उत्तराखंड प्रदेश और इसका कुमाऊं अंचल अतीत में धन-धान्य की दृष्टि से कमतर ही रहा है। यहां आजादी के बाद तक अधिसंख्य आबादी दीपावली पर खील-बताशों, मोमबत्तियों तक से अनजान थी।
पटाखे भी यहां बहुत देर से आए। बूढ़े-बुजुर्गों के अनुसार गांवों में दीपावली के दीए जलाने के लिए कपास की रुई भी नहीं होती थी। अलबत्ता, लोग नए खद्दर का कपड़ा लाते थे, और उसकी कतरनों को बंटकर दीपक की बत्तियां बनाते थे। दीपावली से पहले घरों को आज की तरह आधुनिक रंगों, एक्रेलिक पेंट या डिस्टेंपर से नहीं, कहीं दूर-दराज के स्थानों पर मिलने वाली सफेद मिट्टी-कमेट से गांवों में ही मिलने वाली बाबीला नाम की घास से बनी झाड़ू से पोता जाता था। इसे घरों को ‘उछीटना’ कहते थे। घरों के पाल (फर्श) गोबर युक्त लाल मिट्टी से हर रोज घिसने का रिवाज था। दीपावली पर यह कार्य अधिक वृहद स्तर पर होता था। गेरू की जगह इसी लाल मिट्टी से दीवारों को भी नीचे से करीब आधा फीट की ऊंचाई तक रंगकर बाद में उसके सूखने पर भिगोए चावलों को पीसकर बने सफेद रंग (बिस्वार) से अंगुलियों की पोरों या नीबू, नारंगी आदि की पत्तियों से ‘बसुधारे’ निकाले जाते थे। फर्श तथा खासकर द्वारों पर तथा चौकियों पर अलग-अलग विशिष्ट प्रकार के लेखनों से लक्ष्मी चौकी व अन्य आकृतियां ऐपण के रूप में उकेरी जाती थीं, जो कि अब प्रिंटेड स्वरूप में विश्व भर में पहचानी जाने लगी हैं। द्वार के बाहर आंगन तक बिस्वार में हाथों की मुट्ठी बांधकर छाप लगाते हुए माता लक्ष्मी के घर की ओर आते हुए पदचिन्ह इस विश्वास के साथ उकेरे जाते थे, कि माता इन्हीं पदचिन्हों पर कदम रखती हुई घर के भीतर आएंगी। दीपावली के ही महीने कार्तिक मास में द्वितिया बग्वाल मनाने की परंपरा भी थी। जिसके तहत इसी दौरान पककर तैयार होने वाले नए धान को भिगो व भूनकर तत्काल ही घर की ऊखल में कूटकर ‘च्यूड़े’ बनाए जाते थे, और इन च्यूड़ों को बड़ी-बुजुर्ग महिलाएं अपनी नई पीढ़ी के पांव छूकर शुरू करते हुए घुटनों व कंधों से होते हुए सिर में रखते थे। साथ में आकाश की तरह ऊंचे और धरती की तरह चौड़े होने तथा इस दिन को हर वर्ष सुखपूर्वक जीने की शुभाशीषें देते हुए कहती थीं, ‘लाख हरयाव, लाख बग्वाल, अगाश जस उच्च, धरती जस चौड़, जी रया, जागि रया, यो दिन यो मास भेटनै रया।’ कहते हैं कि आकाश की तरह ऊंचे और धरती की तरह चौड़े होने की यह आशीषें सबसे पहले भगवान राम को भी दी गयी थीं। इसी दौरान गोवर्धन पड़वा पर घरेलू पशुओं को भी नहला-धुलाकर उन पर गोलाकार गिलास जैसी वस्तुओं से सफेद बिस्वार के गोल ठप्पे लगाए जाते थे। उनके सींगों को घर के सदस्यों की तरह सम्मान देते हुए तेल से मला जाता था।
यहां महालक्ष्मी के साथ इसलिए विष्णु की जगह विराजते हैं गणेश
लोक चित्रकार एवं परंपरा संस्था के प्रमुख बृजमोहन जोशी के अनुसार पहाड़ पर दिवाली छोटी दिवाली से बूढ़ी दिवाली तक तीन स्तर पर मनाई जाती है। यहां कोजागरी पूर्णिमा कही जाने वाली शरद पूर्णिमा को छोटी दिवाली माता लक्ष्मी के बाल स्वरूप के साथ मनाई जाती है। कोजागरी पूर्णिमा से बूढ़ी दिवाली यानी हरिबोधनी एकादसी तक घरों के बाहर पितरों यानी दिवंगत पूर्वजों के लिये आकाशदीप जलाया जाता है। इस दौरान चूंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चातुर्मास के लिये क्षीरसागर में निद्रा में होते हैं, इसलिए महालक्ष्मी के पूजन पर माता लक्ष्मी के साथ विष्णु की जगह प्रथम पूज्य गणेश की पूजा होती है, तथा कुमाऊं की प्रसिद्ध डिगारा शैली में गन्ने से बनाई जाने वाली लक्ष्मी को घूंघट में बनाकर कुमाऊं की परंपरागत ऐपण विधा में बनने वाली लक्ष्मी चौकी पर कांशे की थाली में रखा जाता है। साथ ही घर के छज्जे से गन्ने लटकाए जाते हैं, ताकि देवगण इन्हें सीढ़ी बनाकर घर प्रवेश करें। महालक्ष्मी पूजन के लिये प्रयुक्त कुल्हड़, ऊखल व तुलसी के बरतनों में भी अलग तरह के ऐपण बनाए जाते हैं। वहीं बूढ़ी दिवाली को चूंकि विष्णु भगवान जाग जाते हैं, इसलिये इस दिन लक्ष्मी के साथ विष्णु के चरण भी ऐपण के माध्यम से बनाए जाते हैं।