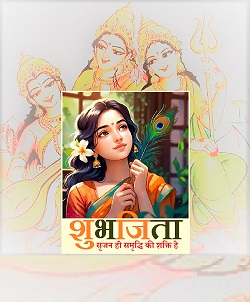सभी सखियों को नमस्कार। सखियों, आज थोड़ी सी बात स्त्री के अधिकारों और उसके प्रति होने वाले शोषण पर करने का बहुत मन हो रहा है। कारण कोई विशेष तो नहीं। दरअसल स्त्री के अधिकारों को लेकर जितना हल्ला मचता है, उतना काम नहीं होता। जी हाँ हल्ला, इस शब्द का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रही हूँ क्योंकि हल्ला मचाने से यह भ्रम जरूर तैयार होता है कि काम हो रहा है लेकिन उस हल्ले में जरूरी मुद्दे सायास दब या दबा दिया जाते हैं। आजकल इस हल्ले के हम इस कदर आदी होते जा रहे हैं कि असली सवालों से हमारा ध्यान हट सा गया है। कहने को स्त्री विमर्श तो है ही, साहित्य का एक विमर्श, जिसके तहत विद्यार्थियों को एक पेपर पढ़ाया ही जा रहा है तो स्त्रियों को उसी में खुश हो जाना चाहिए कि साहित्य के इतिहास में एक अध्याय तो उनके नाम हुआ। भले ही जमीनी तौर पर आम स्त्री ने इस विमर्श का नाम ही ना सुना हो। उसके लिए पति देवता और ससुराल स्वर्ग समान है और उसी के सपनों में वह दिन- रात खोई रहती है या फिर ऐसा करने को बाध्य होती है। अब ससुराल अगर सच का स्वर्ग अथवा स्वर्ग जैसा भी हुआ तो गनीमत है न हुआ तो चुनौती उसके सामने रख दी जाती है कि “बड़े घर की बेटी” तो वही होती है जो खंडहर को भी अपने त्याग और समर्पण से स्वर्ग में तब्दील कर दे और निष्ठुर से निष्ठुर व्यक्ति के मन में प्रेम का दीप जला दें। और इस चुनौती को स्वीकारने के सिवाय और कोई रास्ता उसके पास होता ही नहीं। लेकिन उस तथाकथित स्वर्ग में कभी- कभार उसे ऐसी नारकीय यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता है कि उसके बयान के लिए शब्दों को दर्द की स्याही में डुबाने की जरूरत पड़ती है।
यह बात तो हुई ससुराल रूपी स्वर्ग की। अब थोड़ी सी बात उस घर की भी कर लें जहाँ की मिट्टी में खेल -कूदकर वह बड़ी होती है। वहाँ क्या उसके लिए फूलों की चादर बिछी होती है या उन फूलों में कांटे भी छिपे होते हैं ? चलिए फूलों और कांटों को तितलियों और भंवरों के लिए छोड़ देते हैं और बात करते हैं लड़कियों की जिन्हें बचपन से ही यह मंत्र घुट्टी में पिलाया जाता है कि यह घर तो उनके लिए पराया है और उन्हें किसी और बगिया को अपने परिश्रम से महकाना है। और इसी पराए या किसी और स्थान में बसने के साथ ही जुड़ा होता है एक पारंपरिक और तथाकथित पवित्रता मंडित शब्द “विवाह” जो लड़कियों के लिए लगभग अनिवार्य स्थिति होती है। अर्थात लड़की के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, विवाह। और विवाह के उपरान्त जिस घर में वह जाएगी वह होगा उसका स्वर्ग या ??? इस बहस को अगर छोड़ भी दें तो भी यह प्रश्न तो अधर में टंगा ही रहेगा कि क्या लड़की को विवाह करना ही होगा ? हाँ सो तो करना होगा अन्यथा इधर- उधर डोलती फिरेगी और खानदान का नाम डुबाएगी। और यही सब कह- कह कर, लड़कियों को विवाह की वेदी पर होम किया जाता है। लेकिन अगर लड़की विवाह न करना चाहे तो क्या समाज इसे सहजता से स्वीकार करेगा ? शायद क्या बिल्कुल नहीं। दरअसल परायेपन और पराया धन बनाने का षडयंत्र इसलिए रचा गया था ताकि लड़की को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सके। चूंकि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अलिखित संविधान के तहत लड़कों की होती है इसीलिए संपत्ति का उत्तराधिकारी भी वही होता है। हालांकि भारत में समान नागरिक संहिता की मांग 1930 में ही उठाई गई थी। उसके बाद 19848 में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हिन्दू कोड बिल का जो प्रारूप तैयार किया था, उसमें स्त्रियों के लिए विरासत के अधिकार का मुद्दा भी शामिल था लेकिन कट्टरपंथियों के भय से सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लंबी लड़ाई के बाद उत्तराधिकार कानून 2005 में हुए संशोधन के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्रियों को भी पुत्रों के समान हक मिला। 5 सितंबर 2005 को संसद ने अविभाजित हिंदू परिवार के उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया जो 9 सितंबर 2005 से देश भर में लागू हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि कानून बनने से भारत जैसे देश में कुछ भी नहीं बदलता। बदलाव तो तब आएगा जब हमारी सोच बदलेगी। अक्सर शादीशुदा लड़कियों से कह दिया जाता है कि उनकी शादी में जो खर्च किया गया वही उनका प्राप्य है गोया लड़कों की शादी तो बिना किसी खर्च के हो जाती है। और संबंधों को टूटने से बचाए रखने के लिए प्राय: विवाहित लड़कियाँ सारी संपत्ति भाई के लिए त्याग कर खुश होने का भ्रम पाल लेती हैं। इस प्रसंग को सुधा अरोड़ा ने अपनी कविता “राखी बांधकर लौटती हुई बहन” में बड़ी मार्मिकता से पिरोया है। उनकी पंक्तियाँ त्याग और संतोष के पीछे छिपे असंतोष को बड़ी कुशलता से उभारती हैं। देखिए-
“कितना अच्छा है राखी का त्यौहार !
बिछड़े भाई -बहनों को मिला देता है
कोठी के एक हिस्से पर हक जताकर
क्या वह सुख मिलता
जो मिला है भाई की कलाई पर राखी बांधकर !
मायके का दरवाजा खुला रहने
का मतलब क्या होता है
यह बात सिर्फ वह बहन जानती है
जो उम्र के इस पड़ाव पर भी इतनी भोली है
कि चुका कर इसकी बहुत बड़ी कीमत
अपने को बड़ा मानती है।”
अब रही बात अविवाहित लड़की को तो उसे हमेशा तानों से छीला जाता है कि वह परिवार वालों की छाती पर मूंग दलने के लिए बैठी है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर बहुत सी खुदमुख्तार लड़कियाँ संपत्ति का मोह त्याग अपना अलग रास्ता चुन लेती हैं। मजबूत पंखों के सहारे उड़ जाती हैं, आकाश की ऊंचाइयों तक और अगर न उड़ पाईं तो भाइयों और भाभियों की चाकरी बजाती हैं। लेकिन यह तो कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इससे संपत्ति में अधिकार का सवाल हल नहीं होता। इसके बावजूद हमारे यहाँ इन सवालों को इसी तरह हल करने की मानसिकता दिखाई देती है। भरण- पोषण के वायदे के नाम पर उम्र भर की गुलामी करने को, अविवाहित या विधवा औरतों को बाध्य होना पड़ता है। इसके बावजूद अगर कोई लड़की अधिकारों के नाम पर पैतृक घर और संपत्ति में हिस्सा मांगती है तो पहले तो उसे तानों से छेदा जाता है कि वह भाई- भाभी और उनके बच्चों के हिस्से और सुख- समृद्धि पर कुंडली मारकर बैठी है और इतने पर भी अगर वह अपनी मांग से पीछे नहीं हटती तो कदम- कदम पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी की जाती हैं। परिस्थितियों को इतना दुसह्य बना दिया जाता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। कहा जा सकता है कि लड़की कानूनी सहायता ले सकती है लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उतरकर देखें तो वह भी बहुत आसान नहीं होता । पहले तो अपने ही पिता -भाइयों के खिलाफ खड़ी होने वाली लड़की की बेतरह लानत- मलामत की जाती है और अगर इसके बावजूद वह अपने इरादों पर दृढ़ रही तो बैलगाड़ी की रफ्तार से चलने वाली भारतीय न्याय व्यवस्था उसकी हिम्मत तोड़ देती है। और उसी बीच पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक दबाव अपना काम करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में डटे रहने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। जो डटी रहती हैं, वे इतिहास लिखती हैं और औरों के लिए मिसाल बनती हैं। लेकिन ऐसी लड़कियाँ अंगुलियों पर गिनी जाने लायक ही हैं क्योंकि लड़कियों को तो बचपन से ही अधिकारों से वंचित रखा जाता है, ऐसे में वे अपने हक की बात करें भी तो कैसे करें। अक्सर हम कहते हैं कि लड़कियों को विवाहोपरांत शोषण का शिकार होना पड़ता है लेकिन शोषण का चक्र तो उनके जन्म के साथ आरंभ हो जाता है। लिंगभेद की राजनीति की यंत्रणाओं को झेलने की शुरुआत उनके अपने घर या मायके में ही हो जाती है ताकि वह दीर्घकालिक शोषण को बर्दाश्त करने के लिए, हर हाल में खुश रहने या एडजस्ट करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो सकें। हत्या का सिलसिला भी ऐसे ही शुरू होता है- भ्रूण हत्या, सम्मान हत्या से लेकर दहेज हत्या तक के सुनियोजित षड्यंत्र का सिलसिला परंपरा के महिमा मंडन के नाम पर सुचारू रूप से चलता है। हमें इन षड्यंत्रों को पहचान कर उससे बचने और उसका तोड़ खोजने की जरूरत है अन्यथा सरकार “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” के प्रचार के विज्ञापनों पर धन लुटाकर महिला उत्थान का छद्म रचती रहेगी और लड़कियाँ परंपरागत आदर्शों की रक्षा के नाम पर अपनी अस्मिता की हत्या की गवाह बनती रहेंगी। वर्तमान समय में उम्मीद की किरण इस रूप में नजर आती है कि इस स्थिति को लड़कियाँ – स्त्रियाँ अपने जीवट से बदलने की मुहिम में लग चुकी हैं। आज की स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, वह लड़ रही है, सवाल पूछ रही है, देर तक टिके रहने के भरोसे और जीत की उम्मीद के साथ वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शुरुआत कर चुकी है। कात्यायनी इस जागरूक स्त्री की छवि को अपनी कविता में बेबाकी से उकेरती हैं-
“यह स्त्री
सब कुछ जानती है
पिंजरे के बारे में
जाल के बारे में
यंत्रणागृहों के बारे में।
उससे पूछो
पिंजरे के बारे में पूछो
वह बताती है
नीले अनन्त विस्तार में
उड़ने के
रोमांच के बारे में।
जाल के बारे में पूछने पर
गहरे समुद्र में
खो जाने के
सपने के बारे में
बातें करने लगती है।
यंत्रणागृहों की बात छिड़ते ही
गाने लगती है
प्यार के बारे में एक गीत।
रहस्यमय हैं इस स्त्री की उलटबासियाँ
इन्हें समझो,
इस स्त्री से डरो।”
इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि कानूनी अधिनियमों के संशोधन किताबों के पन्नों से निकलकर व्यवहारिक जिंदगी का हिस्सा बने और कानून के रखवाले इस दिशा में क्रियाशील हों तो यह लड़ाई थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी।