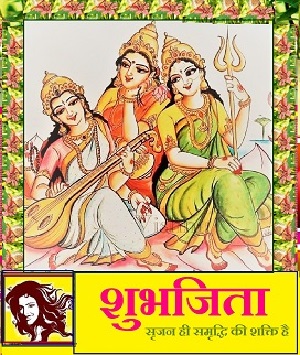-
सुषमा त्रिपाठी
एक युवा और कर्मठ साहित्य व संस्कृतिप्रेमी से बात हो रही थी। वो प्रोफेशनल हैं और एक कॉरपोरेट कम्पनी में काम करते हैं, तनख्वाह भी अच्छी है मगर उनको एक ही परेशानी है। दरअसल, यह परेशानी तो हर सृजनात्मक व्यक्ति की है जो कुछ अलग और दूसरों के लिए करना चाहता है। यहाँ हम यह बता दें कि कुछ करने का मतलब सिर्फ कम्बल, चश्मा औऱ पाठ्यपुस्तकें या छात्रवृत्ति बाँटना नहीं होता। हालाँकि इसका भी अपना महत्व है औऱ यह जरूरी भी है मगर यह काफी नहीं है क्योंकि दान किसी को सक्षम नहीं बनाता। खैर, हम तो साहित्य और संस्कृति की बात कर रहे हैं जिसे हम बाजार के हाथ में छोड़ने को तैयार नहीं हैं मगर इस सच्चाई को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते कि किसी काम को सुचारू रखना हो तो आप बाजार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी कार्यक्रम और योजना को चलाना हो तो आर्थिक सम्बल भी जरूरी होता है और इसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक जागरुकता भी जरूरी है। बस, हमारी बात का जो मुद्दा है, वह यही है क्योकिं हिन्दी को चाहने वालों और सराहने वालों की समस्या यहीं से शुरू होती है क्योंकि वे हिन्दी पर खर्च नहीं करते। उनके पास रेस्तरां, कॉन्वेंट स्कूल, मल्टीप्लेक्स समेत हर चीज पर खर्च करने की कूबत है मगर हिन्दी की किताबें, नाटक या किसी कार्यक्रम पर खर्च करना बोझ लगता है। वह तारीफ जी भरकर करेंगे, अच्छी – अच्छी बातें करेंगे मगर उसका उत्साह बढ़ाने के लिए टिकट या खरीदने की बात उनके दिमाग में नहीं आएगी। ये समस्या बांग्ला और अँग्रेजी के साथ नहीं है क्योंकि वहाँ लोग टिकट खरीदते हैं। पुस्तक मेले में बांग्ला व अन्य भाषाओं के स्टॉल पर उमड़ने वाली भीड़ उस रुचि को दर्शाती है और बुकसेलर्स एंड पब्लिशर्स गिल्ड का कारोबार साहित्य के साथ आयोजकों को भी ऊर्जा देता है कि वे लगातार तीन दशक से इतना भव्य आयोजन करते आ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दी को बाजार को अछूत क्यों मानना चाहिए और बाजार के माध्यम से अगर हिन्दी का प्रचार करें तो क्या बुराई है? तालाब को साफ करना हो तो तालाब में घुसकर ही उसे साफ किया जा सकता है और अगर आप बाजार को तालाब समझते हैं तो आप उसमें घुसना होगा। जब आप बाजार में घुसेंगे तो उससे रोजगार जुड़ेगा और रोजगार जुड़ेगा तो जनता भी जुड़ेगी, ये तय है। अगर आप किसी कार्यशाला या प्रशिक्षण पर शुल्क लगाते हैं तो उसके जरिए होने वाली आय भले ही कम हो मगर उत्साह जरूर बढ़ाएगी। जब लोग खर्च करेंगे तो उस कार्यक्रम में गहराई से जुड़ेंगे और अगर कोई कमी हुई तो आपको बताएंगे क्योंकि उनकी कमाई का एक अंश इस कार्यक्रम से जुड़ा है। जो आय होती है, उससे आप किसी प्रतिभा को सामने लाने में मदद कर सकते हैं और यकीन मानिए हिन्दी से बाहर भी लोग हें जो रुचि रखते हैं। अगर साहित्य और इतिहास से जुड़े विषयों को ऑडियो – विजुअल माध्यम शिक्षण संस्थानों और बाजार में कुछ शुल्क लेकर पहुँचाया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुकाबला करना हो तो वही हथियार आजमाना पड़ता है जो आपका शत्रु इस्तेमाल कर रहा है। हम मानते हैं कि अँग्रेजी हमारी शत्रु नहीं है मगर यह तो मानना होगा कि उसके पास बाजार की ताकत है और यही उसे मजबूत बना रही है। अगर सुल्तान के साथ हरिवंश राय बच्चन की सीडी रहती है तो क्या हर्ज है, कोई एक तो खरीदेगा। अगर प्रेमचंद की कहानियाँ सीडी या ऐप्स पर उपलब्ध हैं तो कोई क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा। हिन्दी से प्रेम है तो पहले खरीद कर पढ़ने की आदत डालिए और किसी भी आयोजक, लेखक या प्रकाशक से, सिर्फ इसलिए कि आप समाज में स्थान रखते हैं, ये उम्मीद करना छोड़िए कि आप तक हर चीज निःशुल्क पहुँचे क्योंकि हर आयोजन पर मेहनत होती है और हर प्रकाशन में खर्च होता है। जब तक वह लागत नहीं निकलती या लाभ नहीं होता, ऐसे आयोजन लाभ में नहीं बदल सकते और लाभ नहीं होगा तो किसी भी युवा में इतनी ऊर्जा नहीं बचेगी कि दोबारा इस सृजन में उसी उत्साह से जुड़े क्योंकि उसको साहित्य के साथ घर भी चलाना है। अगर आय होगी तो घर भी प्रोत्साहित करेगा वरना यह वक्त की बर्बादी भर ही रहेगी और एक समय के बाद पत्रिका, प्रकाशन और आयोजन बंद हो जाएंगे जैसे कि आज हो रहे हैं। हम हिन्दी शिक्षण अथवा आयोजनों अथवा साहित्य को लेकर ऐप्स तैयार क्यों नहीं कर सकते? प्रतियोगिता बढ़ेगी तब लोग अपनी रचनाओं पर और मेहनत करेंगे जिससे सृजन और बेहतर होगा और जब प्रसार होगा तो साहित्य और संस्कृति, दोनों का विस्तार होगा और वह वहाँ पहुँचेगी, जहाँ आप चाहते हैं इसलिए खरीदने और खर्च करने की संस्कृति भी बेहद जरूरी है। डिजिटल इंडिया को हिन्दी में लागू करने की जरूरत है और जनता तक पहुँचना है तो हिन्दी को बाजार को अछूत मानना छोड़ना होगा। बाजार को अपनाकर भी हिन्दी अपनी पहचान मजबूत कर सकती है।