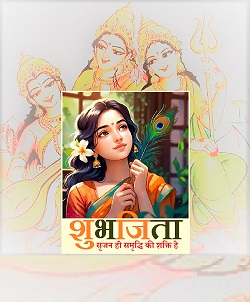समकालीन स्त्री लेखन का परिदृश्य बहुत व्यापक हो चला है। प्राय: महिला लेखन पर यह पहचान चस्पां कर दी जाती है कि वह सिर्फ स्त्री सवालों के इर्द-गिर्द ही घूमता है लेकिन आज के स्त्री कथाकारों की एक बड़ी उपलब्धि है कि वह स्त्री सवालों के साथ -साथ समाज की छोटी – बड़ी सभी समस्याओं पर अपनी विहंगम दृष्टि डालते हुए उनके समाधान की दिशाएं तलाशने की भरपूर कोशिश कर रही है। वह घर -परिवार की परिधि को लांघ कर देश दुनिया की न केवल खबर रखती हैं बल्कि उन खबरों, घटनाओं और परिदृश्यों का अपने लेखन में बखूबी इस्तेमाल भी कर रही हैं। बड़ी संख्या में सक्रिय इन रचनाकारों की रचनाओं पर विचार विश्लेषण और उनका पाठ दर पाठ करते हुए हम पाते हैं कि शिल्प हो या भाषा, विषय-वस्तु हो या मुद्दे हर पहलू पर इनकी गहरी पकड़ है । इसके साथ ही एक उल्लेखनीय बिंदु यह भी है कि आज की लेखिकाएं लेखन को स्त्री और पुरुष लेखन के अलग अलग खानों में बांटने का विरोध करते हुए चाहती हैं कि रचना का स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए।
स्त्री रचनाकारों पर बात करते समय सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहती हूं वरिष्ठ कथाकार चित्रा मुद्गल का जो विविध विषयों पर निरंतर लिखते हुए अपनी सृजनात्मकता और सक्रियता का परिचय देती रही हैं। संवेदनशील कथाकार चित्रा जी के सद्यप्रकाशित उपन्यास “पोस्ट बाक्स नं 203 नाला सोपारा” में एक बिल्कुल नये मुद्दे को केन्द्र में रखा गया है। शिल्प हालांकि बिल्कुल नया नहीं है पर रोचक अवश्य है। पूरा का पूरा उपन्यास एक तृतीयलिंगी पात्र विनोद उर्फ बिन्नी और अंततः बिमली की नजर से दुनिया को देखने समझने की कोशिश है। बिन्नी जो अपनी विशेष शारीरिक पहचान और उस पहचान से जुड़ी भारतीय मान्यताओं के कारण अपने परिवार से जुदा कर दिया जाता है अपनी पीड़ा, दर्द और अपनी नयी दुनिया के संघर्षों को पत्रों के माध्यम से अपनी मां तक ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाता है , इन पत्रों के सहारे ही उपन्यास आगे बढ़ता है। भारत में अगर कोई बच्चा तृतीय लिंगी की पहचान के साथ जन्म लेता है तो उसे किन्नर समुदाय ( आम बोलचाल में हिजड़े) अपने साथ ले जाता है और उनके लिए निर्धारित पेशे को ही उनका प्राप्य या नियति मान लिया जाता है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र बिन्नी बड़े मार्मिक ढंग से यह उल्लेखनीय प्रश्न उठाता है कि आखिरकार क्यों वह सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता ? आखिर क्यों उसे परिवार के सुरक्षा घेरे से बाहर निकाल कर एक गलाजत भरी दुनिया में ढकेल दिया जाता है जहां की रवायतें आम दुनिया से एकदम अलग हैं। इस दुनिया में अनायास ढकेला गया बिन्नी लगातार जटिल परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी मां को लिखे पत्रों में सवालों की झड़ी लगा देता है और ये सवाल अभी तक हमारे समाज में अनुत्तरित ही हैं। आखिर क्यों यह योनिपूजक समाज ऐसे संतानों को घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखता है ? चित्रा जी की पूरी कोशिश रही है कि हम आम लोग जिस उपेक्षापूर्ण दृष्टि से इस विशेष समुदाय के लोगों को देखते हैं उसमें बदलाव आए। समाज इन्हें भी बाकी आम लोगों की तरह समाज में स्वीकार करे और इन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले जैसा और कई देशों में सहज रूप से मिलता भी है।
आलोच्य उपन्यास हिजड़ों के प्रति आमलोगों की मानसिकता को सामने तो लाता ही है जिससे प्रायः हम सभी परिचित होते हैं पर इसकी एक बड़ी उपलब्धि यह है कि यह किन्नरों की मानसिकता और मनःस्थिति की भी गहन पड़ताल करता है। इस तरह के लोगों का बचपन किस तरह के असुरक्षा बोध से घिरा हुआ होता है और अपनी विशिष्ट पहचान के चलते ये किस तरह की मानसिक जद्दोजहद से गुजरते हैं इसका बहुत बारीक विवेचन लेखिका ने किया है। बिन्नी का पहला सवाल ही यह होता है कि वह अपने अन्य दोस्तों जैसा क्यों नहीं है- “स्कूल की चारदीवारी से सटकर पैंट के बटन खोलकर खड़े हो जाने वाले ?” (पृ 10) यह सवाल बेहद मासूम ही नहीं जायज भी है और बिन्नी को बेहद चाहनेवाली ‘बा’ जो उसे दुनिया की नजरों से दूर बचाकर अपने आंचल की सुरक्षा में छिपा लेना चाहती हैं, अपने मासूम बच्चे को यह संबल देती हैं कि वह अपनी विशिष्टता को खुले मन से स्वीकार कर दुनिया का मुकाबला कर पाए। बिन्नी अपनी मां की बातों को याद करते हुए पत्र में लिखता भी है -“तूने यह भी समझाया था और छोकरों से तू अलग है। यह मान लेने में ही तेरी भलाई है, न किसी से बराबरी कर, न अपनी इस कमी की उनसे कोई चर्चा। समाज को ऐसे लोगों की आदत नहीं है और वे आदत डालना भी नहीं चाहते पर मुझे विश्वास है, हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहनेवाली। वक्त बदलेगा। वक्त के साथ नजरिया बदलेगा।”(पृ 10) वक्त तो पता नहीं कब बदलेगा पर बिन्नी की दुनिया जरूर बदल जाती है और उसका मासूम मन इस बदलाव के लिए अपने परिवार को भी कटघरे में खड़ा करता है -“तूने, मेरी बा, तूने और पप्पा ने मिलकर मुझे कसाइयों के हाथों मासूम बकरी सा सौंप दिया। मेरी सुरक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की ? मनसुख भाई जैसे पुलिस अधीक्षक पप्पा के गहरे दोस्त रहते हुए भी ? वो अपने आप मुझे बचाने के लिए तो आ ही नहीं सकते थे। मेरे आंगिक दोष की बात पप्पा ने उनसे बांटी जो नहीं होगी।” ( पृ.11) मासूम बिन्नी के लिए यह समझना मुश्किल था कि जो बात नजदीकी रिश्तेदारों तक से छिपाकर रखी गयी थी वह भला दोस्तों से कैसे बांटी जा सकती थी।
सवाल यह भी है कि शरीर में किसी अन्य अंग की कमी तो स्वीकार्य है और सरकार उसके लिए विशेष आरक्षण भी देती है पर मात्र इस एक कमी के कारण व्यक्ति तिरस्कृत और अस्वीकार्य क्यों हो जाता है जबकि वह अपने सभी सामाजिक कर्तव्यों को भली भांति निभा सकता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज की जड़ मानसिकता जिम्मेदार है तभी तो बिन्नी के चले जाने के बाद भी उसकी छाया उसके मोटा भाई पर मंडराती रहती है। वह निरंतर इस चिंता से घिरा रहता है कि उसका होनेवाला बच्चा कहीं छोटे भाई बिन्नी जैसा न हो और इस मानसिक अवसाद के कारण वह अपना पैतृक घर छोड़कर पत्नी समेत कहीं और रहने के लिए चला जाता है। साथ ही परिवार वालों की निष्ठुरता भी पाठकों को व्यथित करती है जो बिन्नी की आकस्मिक दुर्घटना में मौत की खबर गढ़कर उसकी अनुपस्थिति को ढंकते हैं।
इस उपन्यास की बड़ी खूबी है इसके केन्द्रीय पात्र का मजबूत चरित्र जो अपने जीवट से अपनी जिंदगी को बदलने की ठान लेता है। आम किन्नरों की तरह बुंदे लटका कर , लिपस्टिक -पावडर पोतकर तालियां पीटकर पैसे कमाने के बदले शारीरिक श्रम के बूते आगे बढ़ने की ठान लेता है। वह सिर्फ खुद अपनी जिंदगी के अंधेरे को ही नहीं दूर करने की नहीं सोचता है बल्कि अपने आस -पास के लोगों के ताने झेलकर भी उनकी जिंदगी को शिक्षा की रोशनी से जगमगाना चाहता है। इस राह में जहां कई बाधाएं आती हैं वहीं कई मददगार भी मिलते हैं जिनमें से अन्यतम है पूनम जोशी जो उसपर जान छिड़कती है। वही उसे विधायक तिवारी जी से भी मिलवाती है जहां से बिन्नी की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है लेकिन जहां उसके परिवार ने उसकी शारीरिक कमी के कारण उसे अलग किया था वहीं दूसरी ओर उसके प्रखर व्यक्तित्व उसकी बौद्धिकता के कारण तिवारी जी के कारिंदे उसे उसकी जिंदगी से जुदा कर देते हैं क्योंकि वे समझ गये थे कि विनोद कभी भी उनके इशारों पर नहीं नाचेगा। आलोच्य उपन्यास तिवारी जी जैसे विधायकों की अच्छी छवि के पीछे छिपे घृणित और खौफनाक चेहरे और चरित्र को उजागर करता है जिसका एकमात्र लक्ष्य किसी भी व्यक्ति, मुद्दे या स्थिति का इस्तेमाल अपने हित में करना होता है। पूनम जोशी का बलात्कार, अपराधियों का बच निकलना और अन्ततः विनोद की हत्या राजनीति ही नहीं मानवीयता को भी शर्मसार करनेवाली घटनाएं हैं। एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ खड़ा होता है कि क्या विनोद का अस्तित्व इतना चुनौतीपूर्ण हो गया था कि उपन्यास में उसकी हत्या जरूरी थी। इसके साथ ही एक और सवाल भी उठता है कि ऐसी हत्याएं कब तक होती रहेंगी, क्या कभी किसी विनोद को उसका जायज हक मिलेगा ? हिंदी में किन्नरों के जीवन पर आधारित संभवतः यह पहला उपन्यास है जो किन्नरों के हक के इस सवाल को बड़ी शिद्दत से उठाता है। बांग्ला में कमल चक्रवर्ती ने तकरीबन तीस वर्ष पहले इस विषय पर ‘ब्रह्मभार्गव पुराण’ नामक उपन्यास लिखा था, संभवतः अन्य भाषाओं में भी इस विषय पर लिखा गया हो लेकिन हिंदी में इस विषय पर एक नयी बहस को आरंभ करने का श्रेय निश्चित तौर पर चित्रा जी को जाता है। आलोच्य उपन्यास का एक और उल्लेखनीय और महत्त्वपूर्ण बिंदु है विनोद की दिवंगत बा का माफीनामा जिसमें वह विनोद से वापस लौट आने की गुजारिश करती हैं और घोषणा करती हैं कि उसके पिता ने अपनी अन्य संतानों की तरह विनोद को भी संपत्ति में समान अधिकार दिया है जो एक परिवर्तन की उम्मीद जगाता है। हो सकता है विनोद जैसे दूसरे लोगों के लिए जिंदगी ही आसान न हो बल्कि समाज भी थोड़ा और उदार हो जाए। और जरूरत इस बात की है कि कानून भी इसमें मदद करे। वैसे लक्ष्मी त्रिपाठी की आत्मकथा “मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी’ से गुजरते हुए लगातार यह महसूस होता है कि यह मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि ऐसे बच्चों को जन्म देनेवाले मां बाप किसी ग्लानि बोध का शिकार हुए बिना उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह विकसित होने का अवसर दें। इस उपन्यास को जितना अधिक पढ़ा और समझा जाएगा संभवतः स्थितियों के बदलने की उम्मीद उतनी ही पुख्ता होगी।
बहुत बार ऐसा भी होता है जब मनुष्य की समस्याएं शारीरिक , सामाजिक या आर्थिक नहीं रह जातीं वह मानसिक उलझनों या झंझावातों का शिकार होकर जीवन के प्रति रूचि खो बैठता है या फिर उसका जीवन स्व के प्रति विरक्त होकर व्यापक समाज को समर्पित हो जाता है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिंदगी को बेहद सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। न तो सुखों पर इतराते हैं और न दुखों से घबराते, हर हाल में जिंदगी को एक कर्तव्य समझकर बस जीते चले जाते हैं। ये सारी खूबियां वरिष्ठ कथाकार कुसुम अंसल के नये उपन्यास “परछाइयों का समयसार” के किरदारों में मिलती हैं। मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखा गया यह उपन्यास मि मेहरा, नताशा आदि पात्रों के जीवन के इर्द -गिर्द बुना गया है जो उनके मानसिक अंतर्द्वंद्व को सामने लाता है। इंसान सब से छुटकारा पा सकता है पर अपने अतीत से नहीं, उसका अतीत परछाईं की तरह उसका पीछा करता है। वह जितना ही उससे उबरना चाहता है उतना ही अतीत की अवसादपूर्ण परछाइयां उसे चारों ओर से घेरे रखती हैं। इस उपन्यास के पात्रों के जीवन में भी इसी अवसाद की गहरी छाया दिखाई देती है। सुख एक बिजली की तरह कौंध कर , थोड़ी देर के लिए दृष्टि को चकाचौंध कर फिर से विषाद के घने अंधेरे में लुप्त हो जाता है। इस उपन्यास की भूमिका में लेखिका उपन्यास के स्वरूप को व्याख्यायित करते हुए कहती हैं -“जब मैंने यह उपन्यास लिखना आरंभ किया था, तो सोचा था इसे एब्सट्रैक्ट या आकारहीनता जैसा कोई स्वरूप दूंगी। निर्विचार में चलते-चलते जाने कैसे एक गहरी मनोवैज्ञानिक मानसिकता ने मुझे विवश कर दिया और मेरे हाथ थाम लिए। शायद वह मेरे आत्मचेतन में दबी पुरानी कोई चिंगारी थी, जिसे मुझे पूर्णता तक ले जाना था।”(पृ 7)
लेखिका के अनुभवों की कथायात्रा नताशा नामक एक साधारण पृष्ठभूमि की सामान्य सी लड़की के इर्द- गिर्द घूमती है जिसका चरित्र भले ही बहुत तेज तर्रार नहीं है लेकिन उसका संयत, धैर्यशील और शालीन स्वभाव पाठकों के दिल में क्रमश पैठ बनाता जाता है। इस भौतिक संसार में रहते हुए भी संन्यासी की तरह अपना जीवन बिताने वाले मनोविज्ञान के अध्येता प्रो. वेदप्रकाश मेहरा की छात्रा नताशा के शांत जीवन में अचानक एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है जब प्रो मेहरा का सुंदर, उच्चशिक्षित और एकमात्र पुत्र शैलेन्द्र उसे अपनी जीवनसंगिनी बनने का प्रस्ताव देता है जिसमें प्रो मेहरा की सम्मति भी शामिल थी। कारण था, नताशा का शालीन व्यक्तितव और प्रो मेहरा का अतीत। अपनी अति महत्वाकांक्षी, तेज तर्रार पत्नी ( जो अचानक एक दिन अपने सपनों का पीछा करते हुए पति पुत्र को पीछे छोड़ गयी थी ) से आक्रांत प्रो मेहरा के सामने नताशा एक शांतिपुंज की तरह आती है और पिता से नताशा की प्रशंसा सुनकर शैलेन्द्र अपने पिता की मानसिक सुख-शांति के लिए उसे जीवनसंगिनी बनाना चाहता है। यह रिश्ता नताशा के जीवन में अल्पकालीन खुशियां लाता है क्योंकि एक दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो पक्षाघात का शिकार होकर शैलेन्द्र की जिंदगी अस्पताल के बिस्तर तक सिमट जाती है और नताशा की एक बेंच तक जिसपर बैठी अपने पति की तीमारदारी करती हुई वह अंतहीन प्रतीक्षा बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह इस जगत की पात्र ही न हो। उसे न अपने भविष्य की चिंता सताती है ना रोजी रोटी की। वह किसी वायवीय जगत की शापग्रस्त तपस्विनी सी लगती है जो अनथक साधना करती हुई मानो शापमुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हो। यह तो डा. संदीप उसे उसके भविष्य के प्रति आगाह करते हुए ‘डाइटीशियन’ का कोर्स करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वह उस ओर बढ़ जाती है। आज के दौर में इस तरह का अनासक्त चरित्र चौंकाता है। उपन्यास में कई स्त्री चरित्र हैं और हर चरित्र अपने ढंग का अनूठा है। नताशा की मां, बहन, विद्यावती बहनजी आदि सामान्य पारंपरिक स्त्रियां है। कामिनी अति महत्वाकांक्षी तो नताशा अति धीर गंभीर। विद्यावती के माध्यम से स्त्री की करूणाजनक सामाजिक स्थिति को भी रेखांकित किया गया है। नताशा की सखी मंदिरा एक आधुनिक स्त्री है जो विवाह संस्था को नकारते हुए अपने दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। इसी तरह की एक तथाकथित आधुनिक स्त्री भी है जो सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षय के भय से अपनी बलात्कार पीड़िता बेटी को भावनात्मक संबल तक देने से कतराती हैं। कुछ नर्सें भी हैं जो निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाते हुए समलैंगिक रिश्तों में जीवन का आनंद खोजती हैं। वह नताशा को भी इस ओर खींचने की कोशिश करती हैं पर नताशा उनसे कतराकार निकल जाती है । नताशा को संभवतः लेखिका एक आदर्श स्त्री चरित्र के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक आकर्षण उसकी राह नहीं रोकते पर वह उनके जाल में उलझे बिना अपनी तपस्या में लीन रहती है। पर एक सुशिक्षित लड़की का विज्ञान की बजाय आध्यात्म पर अतिरिक्त विश्वास चौंकाने वाला है। संभवतः परिस्थितियां उसे उस ओर ढकेलती जाती हैं।
विज्ञान और आस्था के बीच की तनातनी कोई नयी नहीं है । विज्ञान किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं करता पर यह भी आश्चर्यजनक है कि जहां विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र समाप्त होता है वहीं से कुछ लोग भक्तिभाव या चमत्कार की शुरुआत मानते हैं। शायद इसी कारण जब डाक्टर सारी दवाइयों का प्रयोग करके हार जाते हैं तो ईश्वर और प्रार्थना की बात करते हैं और कई प्रसिद्ध और बड़े नर्सिंग होम्स में भगवान की मूर्ति या मंदिर विज्ञान और भगवान के इसी अजीबोगरीब तालमेल की ओर संकेत करते हैं । यह घालमेल इस उपन्यास में भी है जब लेखिका एक असाध्य रोग का इलाज मंत्रपाठ से होते दिखाती है। एक महिला की गर्भस्थ संतान जो मानसिक रोग से ग्रस्त है और डा. उसे अबार्ट करने की सलाह तक वह उसे दे चुके हैं वह डाइटीशियन नताशा द्वारा दिए गये मंत्र का पाठ करने से बिल्कुल स्वस्थ पैदा होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि मंत्रपाठ करनेवाली महिला हिंदू हैं ही नहीं।
उपन्यास का अंत भी आकस्मिक संयोग और रहस्यात्मकता के साथ होता है। अस्पताल के जिस बिस्तर पर शैलेन्द्र ने अंतिम सांस ली थी उसी पर एक अजनबी महिला फैशन डिजाइनर ‘रोमी मेहरा’ ह्रदयाघात के बाद सहारा पाती हैं। क्या उनका नताशा से कोई रिश्ता था ? क्या वह शैलेन्द्र की मां थी जिसे अपने दिवंगत बेटे की आत्मा की पुकार अपनी विधवा पत्नी तक खींच लाई थी या इन दोनों स्त्रियों की मिलाकर लेखिका अतीत और वर्तमान का संगम कराकर परिवार को जोड़ना चाहती थी। खैर इस गुत्थी को पाठकों के लिए छोड़कर उपन्यास समाप्त हो जाता है। मनोविज्ञान के अध्येताओं और आध्यात्मिक रूचि के लोगों को यह उपन्यास प्रभावित करेगा इसकी उम्मीद तो की ही जा सकती है।
दलित और स्त्री विमर्श दोनों ही आंदोलन हिंदी साहित्य में नये नहीं हैं लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इन आंदोलनों के फलस्वरूप देश और समाज में जो बदलाव अपेक्षित थे वह वास्तव में आए हैं ? दलितों को कानूनी तौर पर अधिकार भले ही मिल गये हैं पर उनके प्रति वृहत्तर समाज की मानसिकता में कोई व्यापक बदलाव नहीं आया है। आरक्षण के आधार पर भले ही दलितों के एक वर्ग ने थोड़ी- बहुत उन्नति कर ली हो पर यह एक कठोर सच्चाई है कि दलितों के साथ अभी भी भेदभाव होता है और यही स्थिति कमोबेश स्त्रियों के साथ भी है। आरक्षण के फलस्वरूप उन्हें आगे बढ़ने का अवसर तो प्राप्त हुआ पर इसका लाभ चंद महिलाओं को ही मिला वह भी कई मर्तबा सिर्फ दिखावे के लिए ही। उन्हें पद तो मिले पर शासन की बागडोर उनके पतियों के साथ में ही रही और सरपंच और मुखिया के साथ -साथ एक और अतिरिक्त पद की सृष्टि हुई, सरपंच पति, मुखिया पति आदि। आश्चर्य की बात यह है कि इस स्थिति से महिलाओं को कोई खास तकलीफ होती नहीं दिखाई देती । अधिकांश तो पति के साये में सुरक्षित महसूस करती हैं और कुछ को अगर आपत्ति होती भी होगी तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। इन सारे सवालों को सुशीला टाकभौरे अपने उपन्यास ‘तुम्हे बदलना ही होगा’ में बड़े सशक्त ढंग से उठाती हैं। आलोच्य उपन्यास में सामाजिक बदलाव की जरूरत को रेखांकित करते हुए लेखिका उस बदलाव की बयार का स्वागत करती दिखाई देती हैं। साथ ही वह बड़े जोरदार तरीके से समाज और राजनीति के उस पाखंड का पर्दाफाश भी करती हैं जिसके तहत खास वर्ग के लोगों को लगातार उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। नौकरियों में आरक्षण के बावजूद कई बार उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता। आवाज़ उठाने और आंदोलन करने पर हार कर बेमन से उन्हें उनका प्राप्य दिया जाता है। देश और समाज के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज सवर्णों की घिनौनी साजिशों पर कठोर प्रहार करते हुए सुशीला जी बताती हैं कि किस प्रकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दलितों के आंदोलनों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश होती है – ” शोषितों के बढ़ते आंदोलनों को शांतिपूर्ण ढंग से रोकने के लिए , हम स्वयं उनके आंदोलनों का नेतृत्व करें। उन्हें अपने ढंग से समझाने-बहलाने के लिए उनके हित संबंधी कार्यों को अपने हाथों संपन्न करें। इससे समाज की पुरानी व्यवस्था भी बनी रहेगी और हमारी समाजसेवा से हमारा सम्मान भी बढ़ेगा।” (पृ 30) गोया कि बदलाव किसी को स्वीकार नहीं है क्योंकि बदलाव से एक वर्ग विशेष का वर्षों पुराना वर्चस्व समाप्त जो होता है। यही हाल स्त्री विमर्श का है, इसे जितना नुकसान इसके झूठे पैरोकारों ने पहुंचाया है उतना किसी दूसरे ने नहीं और लेखिका बड़ी कुशलता से इन छद्म आंदोलनकारियों का पर्दाफाश करती हैं जो सार्वजनिक मंचों पर तो दलितों और स्त्रियों की तरक्की की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक ओर दलितों के प्रति ऊपरी सहानुभूति दिखाते हुए अंदर ही अंदर उनसे घृणा करते हैं , यहां तक कि उन्हें अपने घर की चौखट तक लांघने नहीं देते तो दूसरी तरफ दुनिया भर की औरतों के उद्धार की बातें करने के बावजूद अपने घर की औरतों को घूंघट की ओट में छिपाकर घर की चौखट के अंदर कैद रखते हैं। लेखिका ऐसे लोगों पर तीखा व्यंग करती हैं -“जाग्रत महिलाओं के समता- स्वतंत्रता के आंदोलनों को देखते हुए पुरुष वर्ग विशेष रूप से चैतन्य हो गया है। वे अब विशेष रूप से महिलाओं के शुभचिंतक बनकर महिलाओं के हित में कार्यक्रमों को बढ़ -चढ़कर करने और दिखाने का प्रयत्न करने लगे हैं। स्वर्ण संपन्न पुरूषों के ऐसे सहयोगपूर्ण स्वभाव, व्यवहार और कार्यों को देखते हुए, मध्यवर्ग की स्वर्ण महिलाएं आश्वस्त होने लगी हैं । वे कहती हैं, अब हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई सफलता के साथ पूरी हो गयी है। अब पुरुष हमारे अधिकारों के रक्षक बन गये हैं।” वे अपने शुभचिंतक पुरुष वर्ग के प्रति अति कृतज्ञता के साथ, अति विनम्र बनती जा रही हैं। अपने घर के पुरूषों की सेवा और आज्ञा पालन में वे पहले से अधिक सजग और कृत-संकल्प हो गयी हैं।” ( पृ 30)
महिमा भारती, धीरज कुमार , चमनलाल बजाज जैसे चरित्रों के माध्यम से आगे बढ़ते उपन्यास का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन की मांग करना है लेकिन सवाल यह भी है कि बदलाव की प्रक्रिया आरंभ कैसे होगी और इसके लिए क्या आवश्यक है। इसका एक जवाब हो सकता है शिक्षा लेकिन बहुधा तथाकथित शिक्षित मनुष्य अधिक कट्टर होते हैं इसीलिए लेखिका इस बदलाव के लिए शिक्षा और सतत आंदोलन के साथ -साथ प्रेम का रास्ता सुझाती हैं। ढाई आखर के प्रेम में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेम न केवल समाज की मानसिकता में परिवर्तन ला सकता है बल्कि दहेज आदि कई सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति भी दिला सकता है। और प्रेम पर आधारित अंतर्जातीय विवाहों द्वारा सुशीला जी जातीय भेद भाव और ऊंच नीच की पथरीली दीवार को पाटकर समाज को मानव प्रेम की खुशबू से महकाना चाहती हैं। हालांकि महिमा को चमनलाल से ब्याह के बाद भी गेस्ट हाउस में गृहस्थी जमानी पड़ती है और तेज तर्रार महिमा बाहर की दुनिया से कटकर घर की चारदीवारी में सिमटने को बाध्य होती है लेकिन अंततः उसी की कोशिशों से न केवल मास्टर धीरज कुमार और उषा का विवाह संभव हो पाता है बल्कि चमनलाल बजाज का परिवार अपनी सुशिक्षित बहू को पूरे मन से अपना लेता है। इसी सुखद बदलाव की बयार के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है, जो बेहद प्रेरक ही नहीं प्रभावशाली भी है। ‘वह सुबह कभी तो आयेगी’ की तर्ज पर बदलाव की उम्मीद इस उपन्यास का केंद्रीय भाव है और हम उम्मीद करते हैं कि यह बदलाव जरूर आएगा तभी समाज और देश का सर्वांगीण विकास भी संभव है। कितना प्रेरक दृश्य है -“पटाखे फूटने की आवाज़ें आने लगी। महिमा, धीरज कुमार और उनके दलित आंदोलन के साथी अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, उनके प्रयत्नों से समाज के पुराने दृश्य बदल रहे हैं, समाज में उनके दायरे बदल रहे हैं। सदियों से चली आती रही वर्ण- जाति भेद की रीति परंपरा और नीतियां बदल रही हैं। सबके मन में ये भाव मुखरित हो रहे हैं, ‘तुम्हें बदलना ही होगा..” (पृ 240)
स्त्री विमर्श के स्वरूप की एक नयी व्याख्या के साथ हमारे सामने आती हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ। प्रायः स्त्री विमर्श की बात करते हुए उसे पश्चिम से आयातित दर्शन मान लिया जाता है और यह सिद्ध किया जाता है कि भारत में स्त्री सशक्तिकरण का कोई स्वरूप था ही नहीं। गार्गी, मैत्रेयी के इस देश में जहां पंडिता भारती शंकराचार्य तक को बहस में चुनौती देने और हराने की क्षमता रखती है उस देश की स्त्रियों को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए आखिरकार पश्चिम की ओर देखने की जरूरत क्यों पड़ी ? इसका एक उत्तर यह हो सकता है कि हमने अपने प्राचीन साहित्य को न ठीक से पढ़ा और न ही उसकी सम्यक व्याख्या करने की कोशिश ही की। मनीषा अपने उपन्यास ‘पंचकन्या’ में पांच पौराणिक नारी चरित्रों ( द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी और अहिल्या )के माध्यम से भारतीय स्त्री विमर्श की खूबसूरत व्याख्या करती हैं।
इन पांच प्रातस्मरणीया पौराणिक स्त्री चरित्रों को ‘पंचकन्या’ कहा गया है और ये भारतीय स्त्रियों के लिए आदर्श चरित्र या प्रेरणास्रोत हैं। ये स्त्रियां अपनी दृढ़ता, स्वतंत्र व्यक्तित्व और निर्णायक क्षमता के कारण भारतीय स्त्री विमर्श की शुरुआत करती हैं जिसे कालांतर में दबा दिया गया। असूर्यम्पश्या ,सकुची- सहमी भारतीय सती नारी की पारंपरिक स्त्री छवि के उलट वे भव्य और स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं जो तथाकथित सामाजिक नियमों को चुनौती देती हुई अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीती हैं। मनीषा का यह सवाल जायज है कि जब हमारे देश में स्त्री स्वतंत्रता की इतनी समृद्ध परंपरा है तो हमें इसे पश्चिम से आयातित करने की क्या जरूरत है। अपने इसी मत को प्रस्तुत करते हुए वह उपन्यास की भूमिका में लिखती हैं -” निजी तौर पर फेमिनिज्म शब्द की जगह एलिस वाकर का दिया शब्द ‘वुमेनिज्म’ मैं अपने मन के ज्यादा करीब पाती हूं। यह शब्द स्त्रियोचित मुलायमियत लिए ज्यादा उर्वर और फेमिनिज्म का एक बेहतर स्वरूप है जो कि न केवल हर वर्ग की अधिक स्त्रियों को खुद से जोड़ता है, बिना विचारधारागत अलगाव के, पुरुष के साथ भी अपने को जोड़ पाता है। यह स्त्री होने के अहसास को लेकर ज्यादा सकारात्मक प्रतीत होता है…… एलिस वाकर कहती हैं -वुमेनिज्म इज़ टू फेमिनिज्म जजों पर्पल इज़ टू लैवेंडर (ज्यादा चमकदार, आकर्षक, जीवंत और वास्तविक) मुझे इस वाक्य के समानांतर अपनी दमदारी में ‘पंचकन्या’ दर्शन लगता है, जिन्होंने हर युग में अपनी आजादी और अपना कन्या होना बचाए रखा।”(पृ 9)” इसके साथ ही वह प्रदीप भट्टाचार्य के उस बांग्ला लेख का भी जिक्र करती हैं जिसका हिंदी अनुवाद करते हुए वह न केवल इस दर्शन से प्रभावित हुईं बल्कि उन्हें यह उपन्यास लिखने की प्रेरणा भी मिली। इस उपन्यास के अंत में वह लेख भी “पंचकन्या : स्त्री सारगर्भिता” शीर्षक से संकलित हैं।
आलोच्य उपन्यास कई स्त्री चरित्रों के माध्यम से स्त्री स्वतंत्रता के सवालों से टकराता हुआ परंपरा, आधुनिकता और क़बीलाई संस्कृति का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। उपन्यास में जहां दादी और मंजू काकी जैसे पारंपरिक स्त्री चरित्र हैं जो परंपरा प्रेम में खुद को होम करती दिखाई देती हैं तो दूसरी ओर प्रज्ञा , माया और एग्नेस जैसी स्त्रियां भी हैं जो अपने जीवन के नियम कानून खुद गढ़ती हैं। प्रज्ञा जो समाज की दृष्टि में एक अवैध रिश्ते की उपज है और अपने जायज हक के लिए निरंतर बेचैन भी रहती है, अपने दम पर पत्रकारिता की दुनिया का एक नामचीन चेहरा बन जाती है और इस पूरी संघर्ष यात्रा में वह तथाकथित आधुनिक पुरुषों की मानसिकता को भली प्रकार समझ जाती है -“ये वही पुरूष थे जो औरत की आजादी की बात करते थे, कई बार आयातित होकर आए इस परकटे फेमिनिज्म के बिगड़े- विकृत स्वरूप पर वह सोच में पड़ जाती थी कि जिसमें आजादी तो थी पर एकतरफा ‘जेंडर बायस्ड’ ( लैंगिक भेदभाव के साथ ) शुचिता की जिम्मेदारी भी साथ थी।स्वप्नवीहिनता, दैहिक दमन और आगे बढ़ने और बेहतर होने की आकांक्षा के बिना हम किस और कैसे फेमिनिज्म की बात कर रहे थे ? फिर यह भारतीय फेमेनिस्ट होना नहीं, किसी विक्टोरियन कान्वेंट की नं बनने का फरमान हुआ कि शुचिता तुम्हारे हिस्से, सद्चरित्रा और वैवाहिक पवित्रता भी और सादा जीवन उच्च विचार भी तुम्हारे हिस्से ! एक तरफ फेमिनिस्ट बनकर दूसरी तरफ मीराबाई बनकर प्रेम कविताएं लिखते रहो और सारे बेहतरीन पद, प्रतिष्ठा पुरुष को दे दो क्योंकि तुमने कुछ मांगा या खुद की श्रेष्ठता को साबित भी कर दिया तो भी ‘महत्वाकांक्षा’ की तुम्हारे ही गले में लटका दी जाएगी ! क्योंकि तुम स्त्री हो !” (पृ 16) प्रज्ञा इन पुरूषों के नाटक से बचते हुए अपना स्वतंत्र अस्तित्व अपनी शर्तों पर गढ़ने में कामयाब भी होती है । उसकी मजबूत शख्सियत के नीचे एक भावुक लड़की भी छिपी बैठी है जिसे अपने जड़ों से जुड़ने की हुड़क लगातार बेचैन बनाए रखती है लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अपनी भावुकता को आसानी से वश में कर लेती है।
एक और स्त्री व्यक्तित्व है एग्नेस जो अपनी नानी की प्रेरणा से नृत्य सीखने भारत आती है। बेहद रोमानी एग्नेस जिसे यह रोमांटिक स्वभाव अपनी मां और नानी से मिला है बार- बार में प्रेम में पड़ती है और फिर- फिर उससे उबरकर आगे बढ़ जाती है। उसे किसी किस्म का ग्लानि बोध या यौन शुचिता का हव्वा आक्रांत नहीं करता। पर हां वह प्रेमी पुरुष के छद्म को नजानते ही उसे झटककर आगे बढ़ जाती है।
इसी तरह माया है जो अपने सपने बंचवाने आश्विन के पास आती है और सदा के लिए वहीं की होकर रह जाती है। बिना ब्याह के अश्विन के साथ बंधने या रहने को लेकर थोड़ी बहुत हिचक जरूर है पर अश्विन के परिवार के स्त्रियों का मानसिक खुलापन और उदार व्यवहार उसे निरंतर मानसिक संबल प्रदान करता है।
इन प्रमुख स्त्री चरित्रों के साथ ही मनीषा राजस्थान की घुमंतू जनजाति कालबेलिया समाज का वर्णन करती हुई वहां की स्त्रियों के जीवन की विसंगतियों को भी उजागर करती हैं। ऊपर से देखने पर तो ये स्त्रियां बेहद उन्मुक्त और स्वतंत्र जान पड़ती हैं पर वास्तव में ऐसा नहीं है , इनका जीवन भी कई प्रकार की नियम श्रृंखलाओं में बंधा होता है। ये कितने भी लोगों से फ्लर्ट या दोस्ती कर ले पर शादी अपने ही कबीले में करनी होती है और एक बार शादी हो जाने के बाद ये मेले में नाच नहीं सकतीं। ऊपर से स्वच्छंद दिखाई देते समाज की लड़कियां भी अपने जीवन साथी का चयन खुद नहीं कर सकती परिवार के फैसले को उन्हें सिर झुकाकर खुशी -खुशी मानना पड़ता है। उस पर से तुर्रा यह कि शादी के सालभर के अंदर संतानोत्पत्ति करनी होती है अन्यथा उन्हें बुरी औरत माना जाता है। सोपीना जैसी कुछ स्त्रियां जो अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए इन नियमों का उल्लघंन करती हैं वह अगर सफल होती हैं तो ‘बादाम’ बन जाती हैं जो कि प्राय बहुत कम स्थितियों में संभव हो पाता है, अन्यथा बिना शादी के किसी पुरुष के साथ बंधकर, ताने झेलते हुए नाच गाकर जीवन बिताती हैं। लेकिन इन स्त्रियों के स्वभाव की उन्मुक्तता और बेबाक व्यवहार में पंचन्याओं की झलक जरूर दिखाई देती है। कबीले विशेषष का वर्णन करते हुए मनीषा वहां की भूख , गरीबी और रोज़मर्रा के जीवन संघर्षों को भी रेखांकित करती चलती हैं।
प्रज्ञा निरंतर अपने इर्द-गिर्द की स्त्रियों में पंचन्याओं की खोज करती है और उस पहचान को पाकर आश्वस्त होती है। उनका मानना है कि “पंचकन्याएं हर कहीं हैं, हम में भी हैं, इसी समाज में…”(179) उसे कालिंदी या काली में भी उनकी झलक मिलती है जो पति और प्रेमी के बीच झूलती हुई अंततः पति के हत्यारे प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने का निर्णय लेती है । इस तरह इन पौराणिक सशक्त स्त्री चरित्रों की पुनर्खोज करती हुई मनीषा भारतीय स्त्री विमर्श को परिभाषित और व्याख्यायित करती हैं। हालांकि कई स्थलों पर उदाहरणों के कारण कथाप्रवाह में बाधा पड़ती है और उपन्यास बोझिल होता जान पड़ता है लेकिन अपनी नयी शैली , विचारधारा और स्थापनाओं के कारण निसंदेह यह उपन्यास पाठकों को प्रभावित करेगा और इससे स्त्री विमर्श के भारतीय स्वरूप को समझने में सहायता मिलेगी।
——-+ ——+++-+——++++++ —–+++++
- बाक्स नं 203 नाला सोपारा (उपन्यास) , चित्रा मुद्गल , सामयिक पेपरबैक्स, नयी दिल्ली, 2010, मूल्य 200 रूपए
- परछाइयों का समयसार ( उपन्यास), कुसुम अंसल, सामयिक प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2007, रूपए 395
- तुम्हें बदलना ही होगा…( उपन्यास), सुशीला टाकभौरे, सामयिक प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2017, रूपए 495
- पंचकन्या ( उपन्यास), मनीषा कुलश्रेष्ठ, सामयिक प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2016, रूपए 395
गीता दूबे, पूजा अपार्टमेंट, फ्लैट नं ए 3, द्वितीय तल, 58 ए/ 1 प्रिंस गुलाम हुसैन शाह रोड, यादवपुर, कोलकाता :700032, मोबाइल : 9883224359, ईमेल : [email protected]