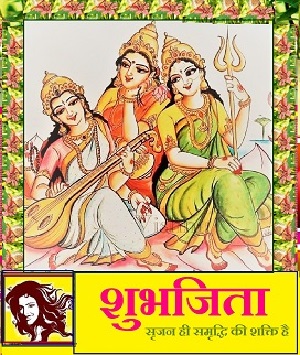यह एक सामान्य सिद्धांत है कि किसी भाषा पर प्रभुत्व होना या उससे अच्छी तरह परिचित हो जाना तभी लोग मानते हैं जब सीखने वाला उसी भाषा में सीख सके अर्थात चित्तवृत्ति उसके मनन करने के विषयों की उसी भाषा के रंग से ग्रहण करे। इसके मानने में किसको इनकार होगा कि हर एक भाषा के ढंग निराले ही हैं। दो भाषा व्याकरण की रीति पर कुछ मिलती भी हो परंतु वे चीजें जिनकी मुहाविरे कहते हैं कभी नहीं मिल सकते और यही मुहाविरे ही हर भाषा की जान है। हिंदी और अंगरेजी ही को लीजिए इन दो भाषाओं में थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं व्याकरण के नियमों का तो भेद हई है। किंतु बड़ा भारी अंतर मुहाविरों की निराली चाल का है। जहाँ कहीं इन मुहाविरों की कोई गलती सुनने में आती हैं तो वह कान से चट खटक जाती है। यह लोग कदापि न समझै कि मुहाविरे अंगरेजी ही में हैं और जब उन पर आक्षेप होता हैं तो ‘राधा बाजार अंगरेजी’ या ‘बाबुओं की अंगरेजी’ इत्यादि शब्द तजआ निंदा की राह से कहे जाते हैं। जब तक किसी भाषा में जान है अर्थात रोजमर्रे के काम में उसे लोग वर्तते हैं और पुष्ट रीति पर उसके स्थिति बनी रहती है तब तक नये-नये मुहाविरे नित्य गले में बनते ही जायेंगे।
सृष्टि के चेतन पदार्थों का जो नियम है कि वे कभी एक सा नहीं रहते वरन दिन प्रतिदिन परिवर्तन की सान पर चढ़ते ही जाते हैं। यह नियम भाषा के संबंध में पूरी रीति पर लगता है। क्योंकि कुछ ऐसा मालूम होता है कि रुधिर और अस्थि मनुष्य के शरीर से उतना निकट संबंध नहीं रखते जितना उनकी भाषा रखती है। और इसी कारण बड़े से बड़े पंडित के आगे कोई अशुद्ध संस्कृत शब्द बोलिए तो वह इतना न खटकेगा जितना एक सामान्य से सामान्य बेमुहाविरे हिंदी शब्द कान को चोट पहुँचावेगा। क्योंकि संस्कृत अब बोल चाल की भाषा न रह गई। विचार कर देखिए तो जो हिंदी हम आजकल बोलते हैं वह पहले क्या थी और अब क्या है। अब फारसी उर्दू शब्द उसमें मिलते जाते हैं क्योंकि जब आपके बड़े-बड़े प्रामाणिक हिंदी कवियों ने फारसी अरबी के शब्द ग्रहण किए तो हमारे और आपके निकाले वे सब जो हमारी भाषा के नस-नस में अंतःप्रविष्ठ में हो रहे हैं क्योंकर निकाल सकते हैं। बल्कि, विरुद्धता दिखलाना वैसा ही है जैसा किसी वेगगामिनी नदी के प्रवाह को अकेले एक हाथ से रोककर उलट देने का प्रयत्न करना है। जिस तरह ये शब्द सर्वसाधारण अपनी भाषा में प्रचलित कर लेते हैं या जिस तरह के शब्द अपने नित्य के बोल चाल से लोग निकालकर फेंक देते हैं और उस पर आप को कुछ भी अधिकार नहीं है। आप मनुष्यों की भाषा तभी बदल सकते हैं जब जुलू या हबशी की जात का कोई आदमी इन देशों में पैदा कर सकैं या इससे भी बढ़कर कोई दूसरा प्राकृतिक अनर्थ जो सर्वथा प्रकृति विरुद्ध हो कर सकैं। क्योंकि यह कैसे संभव है कि प्रबल कालचक्र अपनी निशानी सब चीजों पर न छोड़ जाय। मुसलमानों के अत्याचार का फल जैसा हम अपनी रीति-रसम सामाजिक व्यवहार अपनी और अपने यहाँ की स्त्रियाँ की दशा सब में पाते हैं तब यह क्यों कर हो सकता है कि मुगलों की भाषा का असर हमारी भाषा में न हो।
सोचिये कि जिस हिंदी को हम बोलते हैं वह कितने हजार वर्ष से घिसते-घिसते करोड़ों टक्करें खाकर और न जानिये कौन-कौन सी मुसीबतें झेलकर न मालूम किसका-किसका जमाना देख भाल आज हमारे बोल-चाल के काम में आ रही है। यदि प्रकृति को भी हिंदी ही मान लीजिये तो देखिये कि आजकल की हिंदी से और चाँद और पृथ्वीराज के समय की हिंदी से और चाँद के समय की हिंदी से और कालिदास के समय की हिंदी से काल में कितना अंतर है क्योंकि कालिदास भवभूति प्रभृति कवियों के समय में भी संस्कृत जैसी उनके नाटकों में पाई जाती है केवल विद्धानों ही की मंडली में बोली जाती थी और वे लोग भी कवित्व शक्ति के प्रकाशक गाझिन शास्त्रार्थ के बाद घर जाते रहे होंगे तो नौकरों या लड़के बालों या स्त्रियों से (या सृष्टिसृष्टुराध्या) के जोड़ की बड़े धूम-धाम की संस्कृत न बोलते रहे होंगे। जैसा वेद की संस्कृत का व्याकरण भास बाल्मीकि तथा कालिदास आदि कवियों की संस्कृत के व्याकरण से कुछ पृथक है वैसा ही नाटक की प्राकृतों का व्याकरण चंद आदि की प्राकृतों से विभिन्न है अर्थात जो एक समय के विद्धानों की साधु भाषा थी वही किसी पूर्व समय के बेपढ़े-लिखे लोगों की भाषा रही और उस अदल-बदल में एक बात सदा ध्यान देने लायक है कि भाषा का परिवर्तन शब्दों पर इतना निर्भर नहीं जितना उसके व्याकरण संबंधी विषयों पर या मुहाविरों के अदल-बदल होने पर अर्थात नये शब्दों की भरती होने से कुछ डर की बात नहीं है बल्कि पढ़े-लिखे लोग या सर्वसाधारण उन शब्दों को अपना कर मान लें तो भाषा भी पुष्ट हो जायगी।
फारसी में देखिये तो यही हाल है अंगरेजी में देखिये तो यही हाल है। पृथ्वी की और भाषाओं में यही नियम पाया जाता है कि दूसरी भाषा के शब्द बेधड़क अपना कर लेते हैं। जैसा कोई किसी लड़के को गोद ले वैसा ही वह शब्द उसी भाषा का होकर रह जाता है। एक दूसरी विचित्र बात यह भी है एक भाषा का शब्द जब दूसरी भाषा में जाता है तो बहुधा अपने शुद्ध रूप में कभी नहीं रहता और जब ऐसा अशुद्ध शब्द भी दूसरी किसी भाषा में अच्छी तरह मिल जाता है तो उसके शुद्ध करने का प्रयत्न भी व्यर्थ ही है क्योंकि बोलने वालों के मन या जबान पर जो एक बार चढ़ गया वह कभी नहीं निकल सकता।
भाषाओं के इतिहास में आप हिंदी की दशा देखा यह मत समझ लीजिये कि भाषा की सूरत बदलने के लिए विदेशी भाषा के साथ टक्कर खाना जरूरी बात है। ऐसा ख्याल करना भूल है कि अगर विदेशियों की भाषा के साथ यह भाषा टक्कर न खाये होती तो शुद्ध रीति पर बनी रहती। क्योंकि वेद की संस्कृत को नाटक और काव्यों की संस्कृति में किसने उतार दिया। या संस्कृत को प्राकृतों के रूप में किसी विदेशी भाषा के साथ टक्कर खाने ने बदल दिया। और फिर भाषा की बाहरी आकृति पर विदेशियों का कुछ असर पहुँच सकता है पर उसके भीतरी नियमों को तिलभर भी खसकाना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। हमने ऊपर कहा कि भाषा भी संसार को इतर चैतन्य सृष्टि का नियम मानती है। इस तरह जैसा पीटने से गदहा घोड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह बाहर वालों का संपर्क भी कुछ बहुत हानिकारक नहीं हो सकता और फिर भाषा के संबंध में (हानि) शब्द का पूरा-पूरा तात्पर्य तय करना बड़ा कठिन है क्योंकि परिवर्तन के बीज तो भाषा में आप ही आप भरे हैं। क्यों संस्कृत से प्राकृत हुई और प्राकृतों से वर्तमान हिंदी। हम लोगों का केवल इतना ही कर्तव्य है कि देखते जायँ कि क्या-क्या अदल-बदल हुआ है। अभेद्य दुर्ग सदृश पाणिनि के व्याकरण के आगे हिंदी का व्याकरण छोटी सी फूस की झोपड़ी है। ये तो प्रकट है कि अब हमें उतने बड़े व्याकरण की आवश्यकता न रह गई। एक वह समय था कि अनेक जंजालों से भरे हुए पाणिनि कात्यायन पंतजलि के सूत्र वार्तिक भाष्य में एक मात्रा का भी हेर फेर हो जाने पर एक बड़ी भारी इमारत को ढहाकर फिर से खड़ी करना था और इसी का परिणाम यह हुआ कि हमारे यहाँ का व्याकरण ऐसा झंझट से भरा हुआ शास्त्र हो गया जैसा पृथ्वी के किसी कोने में न हुआ होगा। सच पूछिये तो दो गाड़ी के बोझ की पुस्तकें शेखर मंजूषा कैयट बड़े-बड़े जगड़ जाल जो रच गये उनमें और है क्या। सिवा इसके कि कीचड़ में पाँव फिर धोओ एक बड़े यत्न और प्रयास से। एक बने बनाये सुंदर और मनोहर महल को तोड़-फोड़ छिन्न-भिन्न कर पीछे पछताय फिर उसी को बनाया है। इन्हीं विफल चेष्टाओं में व्याकरण इतना बड़ा शास्त्र हो गया जिसमें नवीन और प्राचीनों का झगड़ा पढ़ते-पढ़ते उमर की उमर बीत जाती है कोरे के कोरे मूर्ख रह जाते हैं। ऐसी सरल भाषा हिंदी में इस सब खटपट का अब कुछ काम ही न रह गया पर क्यों ऐसा हुआ यह तो आदमी तभी तैकर रखेगा। जब और भी सैकड़ों हजारों (क्यों) का उत्तर दे सकेगा जैसा क्यों मनुष्य संसार में पैदा होता है? क्यों फिर यहाँ से चला जाता है? इत्यादि, इत्यादि। अब यह प्रश्न उसके संबंध में और उठता है कि यदि भाषा की धारा ऐसे अपरिवर्तनीय इतने जोर-शोर के साथ बह रही कि उसमें चूँ भी नहीं कर सकते तो किसी समय के अच्छे-अच्छे लेखकों का क्या दबाव या अंतर उस पर होता है। इस प्रश्न का उत्तर सहज में मिल सकता है। पुरानी हिंदी को ही लीजिये पुराने ठेठ हिंदी शब्दों को कोई अच्छी तरह सोच-विचार कर लिखने वाला फिर से निज कर समाज में प्रचलित कर सकता है। अपनी निज की भाषा के कामकाजी शब्दों को मर जाने का मृतक प्राय हो जाने से बचाना अच्छे लेखकों का काम है। बाहरी भाषाओं के शब्दों को अपना-सा कर डालना जिसमें भाषा दिन-प्रतिदिन अमीर होती जाय यह भी एक बड़ा काम है और सबसे बड़ा काम है अपने भाषा के विषयों को दूना-चौगुना करते जाना अर्थात जो-जो विषय भाषा में पहले कम थे उनको जिलो देना और जो विषय कभी थे ही नहीं उनको बाहर से लाय भरती करना। इस सबका असर यह होगा कि भाषा की नमन शक्ति बहुत बढ़ जायगी अर्थात जिस तरह के विषय पहले उससे बाहर समझे जाते थे वे जल्द उसकी पहुँच के भीतर आ जायेंगे। हमारे देखते ही देखते अंगरेजी मेमों ने हिंदुस्तानी गहनों का पहिनना आरंभ कर दिया जैसा सोने की चूड़ियाँ जड़ाऊ करें आदि। इसी तरह यदि हम अपनी मातृभाषा को अंगरेजी भाषा के आभूषण से आभूषित करें तो क्या क्षति है। ऐसे प्रश्नों की मीमांसा में अभी अनेक पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष रह गये हैं उनका विचार हम दूसरे अंक में करैंगे। आगे के अंक में ग्रामीण शब्दों के गुण प्रकट किए जायेंगे।